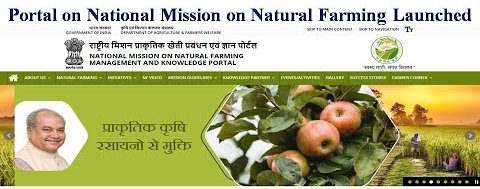फ्रेंच बीन एक महत्वपूर्ण फली है और युवा फली और सूखे बीज दोनों के रूप में उत्कृष्ट सब्जी के लिए पूरे देश में व्यापक रूप से उगाई जाती है। यह मध्यम मौसम की स्थिति में सबसे अच्छा बढ़ता है। इसके अलावा, यह गर्मियों में बढ़ सकता है जहां दिन का तापमान 35°C से अधिक नहीं होता है। यह मेघालय के किसानों के लिए विशेष रूप से पश्चिम खासी पहाड़ियों, पूर्वी खासी पहाड़ियों और री-भोई जिले के कुछ हिस्सों में एक लाभदायक फसल के रूप में उभर सकता है। साल भर फसल उगाने की संभावना को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
@ जलवायु
यह मुख्य रूप से भारत के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है और 21°C के तापमान के आसपास उच्च उत्पादकता दिखाता है और इसकी अधिक उपज के लिए लगभग 16°C से 24°C का इष्टतम तापमान बेहतर होता है। फ्रेंच बीन को बहुत कम या उच्च तापमान पर उगाने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इससे कलियों और फूलों के गिरने के साथ खराब उत्पादकता हो सकती है। अच्छी फसल के लिए इसे 50 - 150 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और पाले की शुरुआत से पहले इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। बहुत अधिक वर्षा जल जमाव का कारण बन सकती है जिससे फूल गिर जाते हैं और पौधे को विभिन्न रोग हो जाते हैं।
@ मिट्टी
यह मिट्टी के मामले में लचीला है और हल्की रेत से लेकर भारी मिट्टी की मिट्टी तक की मिट्टी की एक विस्तृत श्रृंखला में उगाया जा सकता है। हालांकि इसे कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी में इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। बेहतर विकास के लिए इसे 5.2 से 5.8 के इष्टतम पीएच की आवश्यकता होती है और यह उच्च लवणता के प्रति भी संवेदनशील होता है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है कि मिट्टी पर्याप्त रूप से नम हो। अंकुरण के लिए लगभग 15°C मिट्टी के तापमान की आवश्यकता होती है और 18°C पर अंकुरण में लगभग 12 दिन लगते हैं और 25°C अंकुरण में लगभग 7 दिन लगते हैं।
@ खेत की तैयारी
पहाड़ियों में, मिट्टी को ठीक से खोदा जाता है और गोबर की खाद (FYM) को मिलाया जाता है, जिसके बाद उचित आकार के क्यारियां बनाई जाती हैं। मैदानी इलाकों में मिट्टी को दो बार जोतने की जरूरत होती है, जिसके बाद मेड़ और नालियां बनाई जाती हैं। अच्छी तरह से जुताई करने के लिए खेत की 2 या 3 बार ठीक से जुताई करना बहुत जरूरी है। अंतिम जुताई के दौरान बुवाई के लिए मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए प्लांकिंग की जाती है।
@ प्रचार
फ्रेंच बीन्स के बीज जो परिपक्व और सूखे होते हैं, प्रसार के लिए उपयोग किए जाते हैं।
@ बीज दर
झाड़ी प्रकार: 60-65 किग्रा / हेक्टेयर।
पोल प्रकार: 25-30 किग्रा/हेक्टेयर।
@बीज उपचार
बुवाई से 24 घंटे पहले 2 ग्राम बाविस्टिन या थियारम या कार्बेन्डाजिम या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीजों का उपचार करें।
@ बुवाई
* बुवाई समय
इसकी खेती भारत में सर्दियों में सितंबर से नवंबर, वसंत गर्मियों में फरवरी से अप्रैल और पहाड़ियों में जून-जुलाई में की जाती है।
* रिक्ति
झाड़ी प्रकार के लिए 40 x 15 सेमी और पोल प्रकार के लिए 90 x 15 सेमी की दूरी रखी जा सकती है।
* बुवाई विधि
बीजों की बुवाई हाथ से डिब्लिंग करके की जाती है।
अधिक और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के लिए पोल प्रकार की किस्मों की स्टेकिंग आवश्यक है। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली के साथ फसल को लाभकारी रूप से अंतर-फसल किया जा सकता है।
@ उर्वरक
फ्रेंच बीन की झाड़ी प्रकार खेती के लिए 16 किग्रा/एकड़ नाइट्रोजन, 36 किग्रा/एकड़ फॉस्फोरस और 36 किग्रा/एकड़ पोटेशियम की आवश्यकता होती है। बीज बोने के लिए खांचे और मेड़ बनाते समय और अंकुरण के एक सप्ताह के बाद भी आधारी खुराक के रूप में पूर्ण P और K के साथ N का आधा भाग लगाना अत्यधिक प्रभावी होता है। फ्रेंच बीन की उच्च उत्पादकता के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए गुणवत्ता और फली निर्माण में सुधार के लिए 0.1% B, Cu, Mo, Zn, Mn और Mg की सिफारिश की जाती है। बेहतर पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 8 - 10 टन एफवाईएम का प्रयोग करें।
@ सिंचाई
फ्रेंच बीन एक उथली जड़ वाली फसल है, इस प्रकार यह जल तनाव और जल जमाव दोनों के प्रति संवेदनशील फसल बन जाती है। यह आवश्यक है कि फसल तक केवल आवश्यक मात्रा में ही पानी पहुंचे। बरसात के मौसम के बाद यदि कुछ मात्रा में नमी रह जाती है तो यह पौधे की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। जब फूल खिलने से पहले की अवस्था में और फली भरने की अवस्था में पौधे को पानी की कमी की स्थिति के अधीन किया जाता है, तो यह पौधे की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर फ्रेंच बीन की खेती काली कपास की मिट्टी पर की जाती है, तो जल जमाव की संभावना होती है और इसलिए मेड़ों पर फ्रेंच बीन उगाने की सलाह दी जाती है। पौधे की सिंचाई नियमित सिंचाई के बजाय कुंड सिंचाई पद्धति से की जा सकती है। सिंचाई पूरी तरह से खेती के प्रकार, मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि वनस्पति अवधि के दौरान पानी की कमी होती है, तो यह पौधों की वृद्धि को धीमा कर देता है और असमान वृद्धि की ओर ले जाता है। फ्रेंच बीन की फसल को किस्म के आधार पर आंशिक या पूर्ण सिंचाई के साथ पूरक किया जा सकता है।
@ खरपतवार प्रबंधन
बीज बोने के 2 या 3 सप्ताह बाद खरपतवार उगने लगते हैं। प्रारंभ में, बुवाई से पहले खेत की जुताई की जा सकती है और सभी खरपतवारों को हटाने के लिए जुताई की जा सकती है। बीज के अंकुरण के बाद, खेत को मैन्युअल रूप से निराई-गुड़ाई और 15 दिनों के अंतराल पर दो बार निराई-गुड़ाई की आवश्यकता होती है। 0.8 से 1.0 किग्रा/एकड़ अलाक्लोर के प्रयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। लगभग 45 दिनों तक खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण के लिए कई खरपतवारनाशी जैसे 1.2 लीटर/एकड़ का स्टॉम्प या 300 मिली/एकड़ पर लक्ष्य का छिड़काव किया जा सकता है। चौड़े पत्तों वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एक अन्य रासायनिक बासग्रान का भी उपयोग किया जा सकता है।
@ फसल सुरक्षा
*कीट
1. कॉर्न इयरवॉर्म
लार्वा पत्तियों, कलियों, फूलों और फलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। लार्वा फूलों को नुकसान पहुंचाते हैं और फल में छेद करते हैं। बड़े प्रवेश छेद बहुत स्पष्ट हैं जो आंतरिक सड़ांध का कारण बन सकते हैं।
इसे कीटनाशकों के छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है और सफेद चादर पर पौधे को हिलाकर भी कीड़ों को हटाया जा सकता है।
2. एफिड्स
मुख्य रूप से लोबिया और मटर एफिड्स फ्रेंच बीन को प्रभावित करते हैं। यदि एफिड का प्रकोप अधिक होता है, तो इससे पत्तियां पीली हो जाती हैं और पत्तियों पर नेक्रोटिक धब्बे दिखाई देते हैं और अंकुर रुके हुए दिखाई देते हैं। यह लताओं की वृद्धि में मंदता का कारण भी बनता है जो उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
इसे चांदी के रंग के प्लास्टिक जैसे प्रतिबिंबित मल्च के साथ पौधें को कवर करके और मजबूत पानी जेट से पौधे को स्प्रे करके भी प्रबंधित किया जा सकता है। नियंत्रण के सर्वोत्तम तरीकों में से एक कीटनाशक साबुन या तेल जैसे नीम या कैनोला तेल का उपयोग है। इसे मिथाइल डेमेटोन 25 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी प्रत्येक को 1 मिली/लीटर पर छिड़काव करके भी नियंत्रित किया जा सकता है। रोगर या मेटासिस्टोक्स के 1 मिली/लीटर पानी का छिड़काव करके भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। थियोडन जैसे कीटनाशकों का 1ml/L या सेविन 2ml/L पर छिड़काव भी अत्यधिक प्रभावी है।
3. फली छेदक
यह क्षतिग्रस्त फली के बीजों को खाता है और लार्वा भी फली में छेद बनाता है। फसल प्रारंभिक नवोदित अवस्था से प्रभावित होती है और अंडों को फूलों पर रखा जाता है जिससे लार्वा फूलों में प्रवेश कर जाते हैं। कैटरपिलर पत्तियों को रोल करते हैं और उन्हें शीर्ष शूट के साथ वेब करते हैं।
Carbaryl 50 WP को 2g/L की दर से अंतराल पर तीन बार छिड़काव करके इसे कुशलता से नियंत्रित किया जा सकता है। पौधे कोकार्बेरिल 10डी@1 किग्रा/एकड़ की दर से से भी झाड़ा जा सकता है। एंडोसल्फान या थियोडान या मैलाथियान के 2 मि.ली./लीटर पानी का छिड़काव करके भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि संख्या अधिक हो तो 5% की दर से नीम के बीज की गिरी का अर्क भी लगाया जा सकता है।
4. बीन वीविल
वयस्क घुन संग्रहित बीजों पर अंडे देते हैं और लार्वा बीज में छेद करते हैं और परिपक्व होने तक उन पर भोजन करते हैं। इससे छिद्रों का निर्माण होता है जो अंततः बीजों की अंकुरण क्षमता को कम कर देता है।
फॉस्फीन गैस के साथ बीजों को फ्यूमिगेट करके इस पर अंकुश लगाया जा सकता है जो कि सेल्फोस और फॉस्फ्यूम टैबलेट के रूप में उपलब्ध है, जिसे 1 या 2 टैबलेट प्रति टन बीज की दर से लगाया जा सकता है।
5. सफेद मक्खी
अंडे पत्तियों के नीचे की तरफ रखे जाते हैं जो 8 दिनों में बच्चे पैदा करते हैं और इसे चूसकर रस पर भोजन करते हैं।
सुबह-सुबह पौधे की वैक्यूमिंग करना ताकि वयस्क अंडे देने में असमर्थ हों, छोटे क्षेत्रों के लिए एक नियंत्रण उपाय है। अरंडी के तेल के साथ पीले स्टिक ट्रैप लगाकर भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है जो कीड़ों को आकर्षित करता है और वे जाल पर चिपक जाते हैं। इसे प्रारंभिक फसल अवस्था में 0.25% मेटासिस्टोक्स या रोगोर का छिड़काव करके भी नियंत्रित किया जा सकता है।
*रोग
1. अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट
पत्तियों पर छोटे अनियमित भूरे रंग के घाव बन जाते हैं जो धीरे-धीरे बड़े वृत्तों के साथ भूरे भूरे रंग में बदल जाते हैं। घाव सामूहिक रूप से बड़े परिगलित पैच बनाते हैं। नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी वाली मिट्टी में उगाए जाने वाले पौधे इस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह पत्तियों के समय से पहले मुरझाने का कारण बन सकता है जिससे लाल भूरे रंग के घाव हो सकते हैं जो फली पर विकसित होने वाली लंबी धारियों में विलीन हो जाते हैं।
2. एन्थ्रेक्नोज
बीजपत्रों पर छोटे, गहरे भूरे से काले रंग के घाव और तने पर घाव हो जाते हैं जो धँसे हुए प्रतीत होते हैं। फली पर भी घाव हो जाते हैं जो भूरे से बैंगनी रंग के होते हैं और धँसे हुए प्रतीत होते हैं। जब संक्रमित बीजों का अंकुरण होता है, तो बीजपत्रों के घाव विकसित हो जाते हैं और बीजाणु कीड़ों, मनुष्यों या किस्मों द्वारा फैल सकते हैं।
रोगाणु मुक्त बीजों का उपयोग करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसे फसल चक्र से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। मैनकोजेब जैसे 2 ग्राम/लीटर या कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम/लीटर या क्लोरोथालोनिल 2 ग्राम/लीटर पर छिड़काव करके रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
3. हेलो ब्लाइट
एक बीजजनित रोगज़नक़ के कारण होता है। यह निचली पत्ती की सतह पर छोटे, कोणीय और पानी से लथपथ धब्बे बनाता है और पीले ऊतक का एक प्रभामंडल बनाता है जो प्रत्येक पानी से लथपथ स्थान के चारों ओर विकसित होता है। फलियों पर, पानी से भीगे हुए धब्बे कई उम्र के साथ थोड़े धँसे और लाल भूरे रंग के हो जाते हैं।
इस रोग को फैलने से रोकने के लिए गहरी जुताई और रोगाणु मुक्त बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों को स्ट्रेप्टोमाइसिन से उपचारित किया जा सकता है और संक्रमित पौधों पर हर 7 से 10 दिनों में कॉपर युक्त रसायनों का छिड़काव करके इसे रोका जा सकता है।
4. बैक्टीरियल ब्लाइट
इससे पत्तियों पर पानी से भीगे हुए धब्बे बन जाते हैं जो बड़े होकर परिगलित हो जाते हैं। घाव आपस में जुड़ जाते हैं और पौधे को जला हुआ रूप देते हैं। फलियों पर गोलाकार, धँसा और लाल भूरे रंग के घाव फलियों पर बनते हैं। यह रोग दूषित बीज, गीले मौसम की स्थिति आदि के कारण हो सकता है। यह जीव आमतौर पर बीजजनित होता है और जैसे ही अंकुरण होता है, बैक्टीरिया बीजपत्र की सतह को दूषित करते हैं और अंत में संवहनी प्रणाली में फैलते हुए पत्तियों तक फैल जाते हैं।
इसे फसल चक्रण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
@ कटाई
झाड़ी प्रकार की किस्मों में बुआई के 50-55 दिन बाद (डीएएस) और पोल प्रकार की किस्मों में 55-60 दिन बाद कोमल फलियाँ कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के लिए फलियों की कटाई 3-4 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए जब वे पूर्ण आकार में आ जाएं।
@ उपज
हरी फली की उपज लगभग 10-15 टन/हेक्टेयर और बीज की उपज लगभग 1.5 टन/हेक्टेयर होती है।French Bean Farming - फण्सी की खेती......!
2022-11-12 15:39:49
Admin