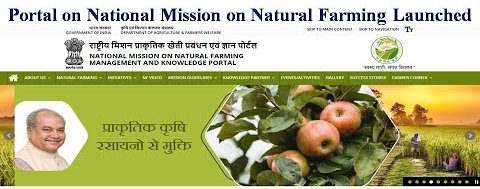पानी के हर बूंद का सही उपयोग करके खेती के माध्यम से आय में वृद्धि। श्री सिचिचेरला चेन्ना रेड्डी (48), लक्कसमुद्रम गांव, तालुपुला मंडल, अनंतपुर जिले, आंध्र प्रदेश, भारत के हैं। वह 15 एकड़ पुश्तैनी जमीन के मालिक हैं और बचपन से ही उन्हें कृषि का शौक रहा है, जब उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लगातार सूखे और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का अवलोकन करना शुरू किया था। वह हमेशा सूखे के दौरान फसलों को बचाने के लिए पानी के आवेदन के अभिनव तरीकों की कोशिश करना चाहता था। श्री रेड्डी कहते हैं, "जैसे पानी की छोटी बूंदें और रेत के छोटे दाने ताकतवर महासागर बनाते हैं, बूंद-बूंद करके, पानी मिट्टी में जड़ों तक नीचे जाता है और अंतर का एक सागर बनाता है"। श्री रेड्डी कहते हैं कि पानी की सीमित उपलब्धता होने पर फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई सिंचाई का एक कारगर तरीका है। इससे पहले, वह सिंचाई की बाढ़ पद्धति का उपयोग कर रहा था। उस समय के दौरान, बोरवेल एक सीज़न में सूख जाता था, और वह अगले सीज़न में सिंचाई नहीं कर पाएगा। उन्होंने महसूस किया कि स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई पद्धति ने सूखे की स्थिति में फसलों को बचाया। वह 1998 की शुरुआत में फसलों की सिंचाई के लिए एक बोरवेल ड्रिल करने वाले अपने गांव के पहले व्यक्ति थे, और फिर उन्होंने 2004 में स्प्रिंकलर के तीन सेट और 2011 में ड्रिप के दो सेट अपनाकर पानी की बचत शुरू की। उन्होंने फसलों के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल किया। जैसे मूंगफली, बंगाल चना और काला चना। जब से उन्होंने ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया है, तब से वह पानी की कमी के बिना पूरे एक साल का प्रबंधन करने में सक्षम हैं। वह न केवल मूंगफली, बंगाल चना और काले चने जैसी कृषि फसलों की खेती करता है, बल्कि वह सब्जियों जैसे डोलिचोस बीन और फल फसलों जैसे तरबूज भी उगाता है। वह ड्रिप सिंचाई की मदद से क्रॉसेंड्रा की खेती करके एक एकड़ भूमि में फूलों की खेती भी करता है। इस सब के कारण, वह अपने परिवार के लिए एक नियमित आय उत्पन्न करने में सक्षम हो गया है। 2014 के बाद से, उन्होंने ड्रिप सिस्टम (प्रजनन) के माध्यम से उर्वरकों को लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने पौधों के प्रभावी विकास के लिए बोरान और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को लागू किया, और बाद में, उन्होंने एसिड का उपयोग करके ड्रिप पाइप को साफ करना शुरू कर दिया। मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने के लिए उन्होंने हर साल फसल चक्रण का पालन किया, और उन्होंने ससंदेनिया के चारों ओर और क्रॉसेंड्रा के बीच में भी पौधरोपण किया, जो आश्रय पट्टी की तरह काम करता है। इसके साथ, उन्हें रुपये 120-200 / प्रति किलो बीज से अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी। मुख्य कारक जिन्होंने उनकी सफलता में योगदान दिया है, उनकी रुचि और उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रति जुनून है। फसल की देखभाल करने की प्रक्रिया में उचित प्रबंधन प्रथाओं के कारण, उन्होंने मूंगफली में नट्स की पॉपिंग को कभी नहीं देखा। वह प्रभावी भूमि उपयोग के लिए आम और काले बेर के बागों में मूंगफली उगाते हैं। दुबले मौसम के दौरान श्रम की अनुपलब्धता के कारण, उन्होंने अंतर-खेती कार्यों के लिए एक ट्रैक्टर का उपयोग करना शुरू कर दिया, और वे एक सीडक-ड्रिल उर्वरक का भी उपयोग करते हैं। भविष्य के लिए उनकी योजना ड्रिप सिंचाई के तहत अपनी पूरी जमीन को कवर करने और फूलों की खेती को बढ़ाने की है। शहरों में फूलों की मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने नई ड्रिप सिंचाई तकनीकों को अपनाने की भी जल्दी की है। उनका मानना है कि जब हम बुद्धिमान निर्णय लेते हैं तो कृषि पारंगत होती है। वह कहते हैं कि युवा पीढ़ी को कृषि को सतत विकास के लिए प्रयास करना चाहिए।
Farmer Success Stories
कृषि के क्षेत्र में सफलता पारिस्थितिक तंत्र की सफलता की ओर ले जाती है।
कृषि के क्षेत्र में सफलता पारिस्थितिक तंत्र की सफलता की ओर ले जाती है। श्री नरिंदर सिंह (54), सर्वश्री राम चंदर, उचाना गाँव, करनाल जिला, हरियाणा, भारत के हैं। उन्होंने लेबर लॉ और ह्यूमन बिहेवियर में मास्टर ऑफ सोशल वर्क (MSW) के रूप में स्नातक किया। शिक्षित होने के बावजूद, वह सेवा क्षेत्र में अपना करियर नहीं बनाना चाहते थे। बचपन से ही उन्हें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का शौक रहा है। अपने स्कूल के दिनों के दौरान, वह अपनी जेब के पैसे का उपयोग करके एक छोटी मधुमक्खी के छत्ते को बनाए रखता था, जो खेती के प्रति उसकी रुचि और जुनून का संकेत था। श्री सिंह ने संजीवनी ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर के साथ अपने करियर की शुरुआत की। कुछ वर्षों तक काम करने के बाद, उन्होंने महसूस किया कि वह अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, और उन्होंने कृषि और संबद्ध गतिविधियों को लेने का फैसला किया। उन्होंने लोगों को विभिन्न कृषि विज्ञानों को समझने और उनके ज्ञान में सुधार करने के लिए मिलना शुरू किया; महाराष्ट्र के पुणे में बागवानी फसलों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, वह एक बागवानी अधिकारी, श्री धर्मपाल से मिले, जब उनका जुनून और दिलचस्पी चौड़ी हो गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तुरंत बाद, श्री सिंह ने अनार के पौधे खरीदे और उन्हें अपने खेत में लगाया। वह न केवल खुद के लिए लाभ कमाने में दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि उन्होंने पूरे हरियाणा में अनार का प्रसार भी किया है। वह अपने खेत को नियमित चावल-गेहूं की खेती प्रणाली से अलग करना चाहते थे। इसी इरादे से उन्होंने 1990 से बागवानी नर्सरी शुरू की। नर्सरी में उन्होंने सेब, जामुन, नाशपाती, आड़ू, सपोटा, अमरूद, आम, लीची जैसी बागवानी फसलों को लिया। वह हरियाणा में सेब पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, और उन्होंने इसका नाम "राणा गोल्ड ऐप्पल" रखा और सेब के पौधे बेचने शुरू किए। उन्हें "हरियाणा के एप्पल मैन" के रूप में भी जाना जाता है। नर्सरी के साथ, उन्होंने अन्य संबद्ध उद्यमों, जैसे मधुमक्खी पालन, फसल उत्पादन, वर्मी-खाद और इतने पर ले लिया। वह प्रतिदिन 180 लीटर दूध देने वाली 15 गायों को पालता है। वह 350 मधुमक्खी के बक्से को भी रखता है जो 27 30 किलो शहद प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि उद्यमों के और पूरक संबंध किसानों के लिए उच्च आय उत्पन्न करते हैं। मधुमक्खी पालन और प्रजनन में अपने समृद्ध ज्ञान और विशेषज्ञता के कारण, उन्होंने साथी किसानों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। 1992-93 में, उन्होंने नर्मदा परियोजना के हिस्से के रूप में गुजरात सरकार को मधुमक्खी के बक्से की आपूर्ति की। बागों में मधुमक्खी के बक्से रखने की उनकी सलाह से उपज में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए, ICAR-NDRI (नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट), करनाल ने उन्हें हरियाणा राज्य पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बी-कीपर से सम्मानित किया। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो (AIR), रोहतक द्वारा 'प्रगतिशील किसान' से भी सम्मानित किया गया है। वह मधुमक्खी पालन और सेब उत्पादन प्रथाओं के बारे में कई टेलीविजन शो का हिस्सा रहे हैं, और उन्होंने कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए कृषक समुदाय को प्रेरित किया है। उनकी भविष्य की योजना बागों के तहत अपने क्षेत्र को बढ़ाने की है। श्री सिंह के अनुसार, "एक विविध कृषि प्रणाली एक सुंदर बगीचे में विभिन्न रंगों के फूलों के पौधों की तरह है"।
किसान ने प्रतिकूलता को अवसर में बदल दिया।
किसान ने प्रतिकूलता को अवसर में बदल दिया। श्री हरि बाबू एक ऐसे किसान हैं जो कृषि का आनंद लेते हैं और जिन्होंने एक किसान बनने का विकल्प चुना है, जबकि उनके पास अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाएं हैं, जैसे कि पत्रकारिता, सिनेमा आदि। खेती उनके दिल के बहुत करीब है। श्री हरि बाबू हैदराबाद के पास 10 एकड़ जमीन के मालिक हैं। भूमि थिमापुर गांव, रंगारेड्डी जिले से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है और मुख्य सड़क पर है, लेकिन यह कुछ नुकसान का सामना करती है कि मिट्टी खराब है और पानी की उपलब्धता अपर्याप्त है। कृषि के अपने जुनून के कारण, उन्होंने इन 10 एकड़ को धरती पर स्वर्ग में बदल दिया। वह 90 विभिन्न प्रजातियों के 9,000 पेड़ लगाए गए। इनमें लाल चंदन, चंदन, शीशम और बागवानी के पौधे जैसे सीताफल, गुलाब सेब, स्टार फल, आम, अमरूद जैसे दुर्लभ और मूल्यवान वन पौधे शामिल हैं। इसमें अश्वगंधा, सरपा सारिका आदि औषधीय पौधे हैं। कोई रासायनिक खेती नहीं। श्री हरि बाबू द्वारा अपनाया गया सफलता मॉडल एकीकृत खेती प्रणाली है। उनके पास छह गायें हैं, जिनके गोबर और मूत्र को जीवनमृतम में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग पौधों के लिए उर्वरक के रूप में किया जाता है। वह कभी रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग नहीं करता है; वह कृषि के केवल प्राकृतिक तरीकों का पालन करता है। उनके बगीचे में 300 से अधिक मुर्गियाँ स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं, और श्री हरि बाबू के अनुसार, ये मुर्गियाँ कीटों को नियंत्रित करने में बहुत अच्छी हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश, दीमक सहित खाते हैं। उसकी खेती के लिए सफलता की कुंजी। उन्होंने व्यक्तिगत भागीदारी और नज़दीकी पर्यवेक्षण, उच्च घनत्व वाले रोपण, नियमित बागवानी और सभी बागवानी संयंत्रों के प्रशिक्षण सहित कई कारकों के कारण अपने खेत में सफलता प्राप्त की है, गायों और पिछवाड़े कुक्कुटों को एकीकृत करके इनपुट लागत को कम किया है, अपरंपरागत पौधों और किस्मों को बेहतर बनाने के लिए। उदाहरण के लिए, ड्रैगन फ्रूट, गुलाब सेब और स्टार फल, जो हैदराबाद में आम नहीं हैं। वह चंदन और लाल चंदन जैसे पौधों के माध्यम से दीर्घकालिक लाभ की योजना बनाता है और साथ ही अल्पकालिक लाभ हालांकि अमरूद, औषधीय आदि। श्री हरि बाबू सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास कृषि के अलावा आय के स्रोत भी हों, जैसे कि ग्राफ्ट, कटिंग आदि बेचना। वह गुणवत्ता सुनिश्चित करने और लागत कम करने के लिए अपने स्वयं के उपयोग के लिए संयंत्र सामग्री को गुणा करता है। वह पूरे वर्ष निरंतर आय की योजना बनाता है और फलों और अन्य उपज का प्रत्यक्ष विपणन करता है। जबकि उनके पड़ोसी कृषि से लाभ नहीं कमाते हैं, श्री हरि बाबू को मिट्टी और जल संसाधनों की सीमाओं के आधार पर उचित फसल योजना, सभी क्षेत्र के कार्यों में व्यक्तिगत भागीदारी और पारंपरिक बुद्धिमत्ता के साथ आधुनिक प्रथाओं का पालन करने के कारण मुनाफा मिलता है। वह एक सफल किसान का एक उदाहरण है और यह साबित किया है कि कृषि में चमत्कार किया जा सकता है अगर निवेश सही दिशा में किया जाए और किसान नवीनतम ज्ञान से लैस हों। श्री हरि बाबू की प्रत्येक एकड़ की शुद्ध आय लगभग रु. 1,00,000 प्रति वर्ष है।
मधुमक्खी पालन के साथ सफलता का मीठा स्वाद।
मधुमक्खी पालन के साथ सफलता का मीठा स्वाद। श्री भूपालक्ष (४ ९), भारत के कर्नाटक के हासन जिले में अलूर तालुका के केंचनहल्ली पुरा गाँव से हैं। वह 7 एकड़ भूमि का मालिक है और खेती की मिश्रित कृषि प्रणाली का अनुसरण करता है (एग्री + हॉर्टी + पेस्ट्री)। मानसून के मौसम में, वह धान, मक्का और बागवानी फसलों जैसे कि मिर्च, अदरक, नारियल, आम, सपोटा, अमरूद और केला उगाते थे और घरेलू उपयोग के लिए सब्जियों की खेती करने के लिए कृषि क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बनाते थे। अपने बचपन में, उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए एक जुनून विकसित करना शुरू कर दिया था। उनकी दिलचस्पी तब बढ़ी जब उनके परिवार के सदस्यों ने हसन जिले के विभिन्न हिस्सों से शहद इकट्ठा करने में भाग लिया। मैट्रिक पूरा करने के बाद, मधुमक्खी पालन का उनका जुनून कृषि के साथ-साथ उनके पेशे में बदल गया। पेशेवर रूप से मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए, 2006 में, उन्होंने अलूर में एक गैर सरकारी संगठन पुण्यभूमि से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, उसे बनाए रखने के लिए मधुमक्खी का डिब्बा दिया गया। कार्यक्रम के एक संसाधन व्यक्ति श्री शांतिवीर के साथ उनके परिचित ने मधुमक्खी पालन में उनकी रुचि को बढ़ाया। इसके बाद, वर्ष 2008 में, उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), हसन से परामर्श किया, ताकि वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के साथ-साथ मूल्यवान प्रबंधन प्रथाओं पर अतिरिक्त जानकारी जुटाई जा सके। समय के साथ, उन्होंने वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इस तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ, उन्होंने पेशे में उद्यम किया और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ अतिरिक्त आय कमाया। 2014-15 के बाद, श्री भूपालक्ष ने केवीके, हासन में आयोजित एक मधुमक्खी पालन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना शुरू कर दिया, दोनों एक प्रतिभागी के साथ-साथ एक संसाधन व्यक्ति भी थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने मधुमक्खी कालोनियों के गुणन का कौशल हासिल किया। उन्होंने सफलतापूर्वक तकनीक को अपनाया, और अब वह सीजन के दौरान एकल मधुमक्खी कॉलोनी को 5-6 मधुमक्खी कॉलोनियों में गुणा करने में सक्षम हैं और उन्हें मधुमक्खी पालकों को आपूर्ति करते हैं। वह चन्नारायणपटना, अर्सिकेरे, गुब्बी, तुमकुर, चिक्कमगलुरु, मदिकेरी और मैंगलोर में 100 मधुमक्खी पालनकर्ताओं की सहायता भी करता है। मधुमक्खी पालन पर तकनीकी ज्ञान हासिल करने के लिए लगभग 2,000 किसान और छात्र उसके खेत में जाते हैं। इस सहायक उद्यम से, उसे सालाना 50 किलो शहद मिलता है और इसे रु.600 / किग्रा और 50 मधुमक्खी के बक्से मधुमक्खी कालोनियों के साथ रु.4000 / बॉक्स की दर से बेचा जाता है। इसलिए यह उद्यम उसे रु.1,40,000 / - से अधिक की वार्षिक आय प्राप्त करता है। अपने कृषि उद्यमों के सफल एकीकरण के लिए, उनके उद्यम के सदस्यों को 2014-15 के दौरान तालुक स्तर पर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (UAS), बेंगलुरु में "सर्वश्रेष्ठ कृषि महिला" पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2015-16 में, उन्हें बागवानी विभाग, कर्नाटक द्वारा कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ति के रूप में भी सम्मानित किया गया, और उन्होंने उन्हें मधुवन योजना के तहत 25 मधुमक्खी के बक्से भी प्रदान किए। श्री भूपालक्ष ने अपने साथी किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया है। वे केवल कृषि में ही सफल किसान नहीं हैं, वे इस क्षेत्र में एक संसाधन व्यक्ति भी हैं, जिनकी सेवाओं का उपयोग विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि KVK-Hiriyur, KVK-Hassan, All India Radio (AIR) -Hassan, Samaya-Television, मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एनजीओ-पुण्यभूमि आदि। भविष्य की उनकी योजनाओं में मधुमक्खी के अधिक से अधिक बॉक्स के साथ अपने मधुमक्खी पालन व्यवसाय का विस्तार करना शामिल है। वह युवाओं को प्रशिक्षित करने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं।
श्री मुत्तप्पा पुजारी एकीकृत खेती के माध्यम से समृद्ध हुए।
श्री मुत्तप्पा पुजारी एकीकृत खेती के माध्यम से समृद्ध हुए। भारत के कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले के हसनपुर गाँव के श्री मुत्तप्पा पुजारी (45) ने 5 वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उनके पास 8 एकड़ जमीन है, और उनके पास दो बैलों और दो बकरियों का भी मालिक है। वह खरीफ के मौसम में लाल चना, कपास, अदरक, फूल और पत्तेदार सब्जियां उगाते हैं। खरीफ की फसलों की कटाई के तुरंत बाद, वह रबी के लिए गेहूं, मिर्च, छोले और ज्वार लेते हैं। श्री पुजारी बचपन से ही खेती कर रहे हैं, और वे समकालीन स्थिति में एकीकृत खेती प्रणाली के साथ जारी रखना चाहते हैं, जहां एक फसल में नुकसान को दूसरे उद्यम के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उनके पास साथी किसानों और इनपुट डीलरों के साथ अच्छा संपर्क है, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। रेडियो के बारे में सुनते हुए उनके पास व्यापक मीडिया प्रसार है, वे टेलीविजन देखते हैं और नियमित रूप से कन्नड़ समाचार पत्र पढ़ते हैं। श्री पुजारी का मानना है कि मिश्रित कृषि प्रणाली की खूबी यह है कि उन्हें ज्यादातर राशन अपने खेत से ही मिलता है। उनके अनुसार, उद्यमों के बीच पूरक संबंध किसानों के लिए अधिक आय उत्पन्न करता है। वह 8 एकड़ जमीन पर 10 अलग-अलग फसलें लेने वाले गांव के एकमात्र किसान हैं। उसके पास एक घर है, लेकिन वह अपने खेत पर 8 साल तक रहा है ताकि अधिक पैदावार के लिए भूमि में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हो सके। उनका मत है कि खेती तभी सफल हो सकती है जब कोई सही समय पर सही निर्णय ले और कड़ी मेहनत करे। वह 0.5 एकड़ जमीन पर टमाटर उगाता है, और प्रभावी प्रबंधन के साथ, उसे 10 टन की उपज मिलती है। श्री पुजारी कहते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र में श्रम की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके कारण वह बेहतर पैदावार के लिए लेबर बल को स्थानापन्न करने के लिए नई मशीनरी खरीदना चाहता है और कृषि महिलाओं का सामना करने वाले नशे को कम करने में मदद करता है। वह अपने ही गाँव में पत्तेदार सब्जियाँ बेचकर प्रतिदिन 200 से 300 / - रु कमाता है। बिचौलियों के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए, वह एक ग्लूट के कारण बाजार मूल्य गिरने पर सब्जियां और मिर्च बेचने के लिए गांव-गांव जाता है। वह कहते हैं कि खेती से उन्हें आत्मविश्वास मिलता है और अपने परिवार को चलाने और आरामदायक जीवन स्तर बनाए रखने के लिए काफी आमदनी होती है। श्री पुजारी को अपनी 8 एकड़ जमीन से 4 से 5 लाख रु का शुद्ध लाभ मिलता है। उन्हें विश्वास है कि यदि गर्मी के मौसम में उनकी बिजली और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो वे अपनी आय में काफी वृद्धि कर पाएंगे। कृषि के अलावा, उन्होंने रु. 3,500 / - के दो बकरे खरीदेऔर दो महीने के भीतर, उन्होंने उन्हें रु. 2,500 / - रुपये के लाभ मार्जिन के साथ रु. 7,000 / - में बेच दिया। वह खेती और मछली पकड़ने के बीच एक समानता के माध्यम से समानताएं खींचता है: उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपको खेत स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक और हर चीज को देखने की जरूरत है। उनके अनुसार, निर्णय लेते समय हाथ होने का श्रेय किसानों को आत्मविश्वास देता है। उनका मानना है कि खेती पारिश्रमिक है और यह रोजमर्रा की सामाजिक-आर्थिक घटनाओं से संबंधित है। हर साल, त्योहार के दौरान उनके गांव के पास पशु उत्सव आयोजित किया जाता है । मकर संक्रांति इस अवसर का उपयोग करने के लिए, उन्होंने दो बैलों को खरीदा और उन्हें चार महीने के भीतर रु. 21,000 / - लाभ के साथ 58,000 / - रुपये में बेच दिया। इसके अलावा, उन्हें जैविक खाद के रूप में गोबर के दो ट्रैक्टर मिले। भविष्य में, श्री पुजारी ने अपनी शुद्ध आय बढ़ाने के लिए साझेदारी में वाणिज्यिक बकरी, मुर्गी पालन और मछली पालन शुरू करने की योजना बनाई है। वह खेती को साक्षरता के बजाय ब्याज और उत्साह से संबंधित करता है और मानता है कि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर मुनाफा कमाने के लिए गणना किए गए जोखिम उठाने की जरूरत है।
पंजाब के किसान ने टिकाऊ कृषि के लिए आगे का रास्ता बनाया।
पंजाब के किसान ने टिकाऊ कृषि के लिए आगे का रास्ता बनाया। श्री एस.सुखदेव सिंह (60),भारत, पंजाब के कपूरथला जिले के भुल्लर बेट गाँव से हैं। उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की और बचपन से ही कृषि का अभ्यास कर रहे हैं। उन्हें जो जमीन विरासत में मिली थी, वह बंजर थी, जिसमें सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी और बहुत कम पैदावार होती थी। भूमि पुनर्ग्रहण कार्यक्रम के तहत, उन्होंने जिप्सम आवेदन के साथ मिट्टी की उर्वरता में जबरदस्त सुधार देखा। इससे पहले, उन्होंने पारंपरिक धान-गेहूं फसल प्रणाली का पालन किया। मिट्टी की उर्वरता में सुधार के साथ, उन्होंने अन्य फसलों, जैसे गन्ना, आलू, सरसों, ब्रेसिम और मक्का आदि पर स्विच किया। धीरे-धीरे, सरासर मेहनत के माध्यम से, कृषि से उनकी आय बढ़ने लगी। अब, वह 74 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं, विविध फसलें उगाते हैं। वह एक लत्ता-से-समृद्ध कहानी का एक आदर्श उदाहरण बन गया है। उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के विस्तार केंद्रों और फार्म सलाहकार सेवा केंद्र (एफएएससी), कपूरथला के तहत प्रशिक्षित किया गया था। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अपने समृद्ध ज्ञान के साथ, वह फसलों की उन्नत किस्मों की खेती करने के लिए प्रेरित हुए। पीएयू, लुधियाना की उन्नत किस्मों की खेती से उनके गेहूं, मक्का, चावल और गन्ने का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। अब वह नियमित रूप से पीएयू के विस्तार केंद्रों द्वारा आयोजित विस्तार कार्यक्रमों जैसे किसान मेला, क्षेत्र दिवस और फसल सेमिनार में भाग लेते हैं। वह वाष्पीकरण के माध्यम से नुकसान पर कटौती करने के लिए भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से फसलों की सिंचाई करता है। बाजार में संकट की बिक्री को रोकने के लिए, वह अपने कृषि उत्पादों को संग्रहीत करता है, जैसे बासमती और मक्का, भंडारण संरचनाओं में भविष्य में उच्च दर पर बेचने के लिए। टेक-सेवी किसान के रूप में, वह अपने स्मार्ट फोन और इंटरनेट का उपयोग कृषि-बाजारों, मौसम की जानकारी और उन्नत कृषि-तकनीक से नवीनतम दरें प्राप्त करने के लिए करता है और आपसी लाभ के लिए अपने साथी किसानों के साथ जानकारी साझा करता है। श्री सिंह अपने खेत में प्रयोग करते हैं और परिणामों को वैज्ञानिकों के साथ साझा करते हैं। उन्होंने गेहूं के वैकल्पिक गीलेपन और सूखने के प्रभाव को देखा और निष्कर्ष निकाला कि यह अंकुरण, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाता है। जिला प्रशासन के आदेशों के अनुपालन में, वह 15 एकड़ में गेहूं की बुवाई करता है और हर साल हैप्पी सीडर के साथ 5 एकड़ में जई का चारा खाता है। इसलिए, वह धान के पुआल को जलाता नहीं है, बल्कि पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त करने के लिए इसे वापस मिट्टी में डुबोता है। गेहूं, चावल, बासमती, जई, हल्दी और गेंदा जैसी विविध फसलों को उगाने के लिए उनके पास एक अचेतन स्वभाव है। इस फसल के पैटर्न से उन्हें प्रति एकड़ कुल वार्षिक आय प्राप्त होती है। गेहूं से, रु. 30,000 / -, चावल से रु 40,000 / - , बासमती से रु. 27,000 / - , मक्का से रु. 40,000 / - , जई से रु. 20, 000 / - हल्दी से रु. 2,40,000 / - और गेंदा की खेती से रु. 30,000 / -। वह एक दुग्ध उद्यम भी रखता है जिसमें 9 दुधारू पशु शामिल हैं। चार भैंस और पांच गाय प्रतिवर्ष लगभग 126 क्विंटल दूध का उत्पादन करती हैं। घरेलू खपत के लिए दूध बख्शने के बाद, अधिशेष दूध डेयरी इकाइयों को बेचा जाता है, जिससे उन्हें वार्षिक रु. 3,78,000 / - आय मिलती है। श्री सिंह को 2017 में पीएयू लुधियाना द्वारा फसल विविधीकरण के लिए दलीप सिंह धालीवाल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह सादगी, रोमांच और ज्ञान के साथ संयुक्त कृषि विज्ञान, आर्थिक समृद्धि और मानवीय मूल्यों का उपयोग करते हुए आधुनिक खेती का एक सफल समामेलन है।
कर्नाटक का मसाला धनी किसान।
कर्नाटक का मसाला धनी किसान। श्री डी.एम. रमेश (59), दरदाहल्ली गाँव, मुदिगेरे तालुक, चिक्कमगलुरु जिला, कर्नाटक, भारत से हैं। उन्होंने पूर्व-विश्वविद्यालय स्तर तक अध्ययन किया है। वर्तमान में वह 15 एकड़ भूमि का मालिक है और वृक्षारोपण फसलों जैसे कॉफी, काली मिर्च और सुपारी को उगाता है। श्री रमेश के अनुसार, हम जिस तरह से समाज में बढ़ते हैं, वह किसी विशेष क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति पर निर्भर करता है। उनकी खेती में गहरी रुचि है क्योंकि उनके पूर्वज खेती करते थे। वह वृक्षारोपण फसलों की खेती करना चाहते थे, लेकिन पूर्ण गरीबी के कारण उनके पास अपनी जमीन नहीं थी और इसलिए वह अपने सपने को हासिल नहीं कर सके। वह नौकरी की तलाश में कूर्ग से मुडिगेरे में शिफ्ट हो गया। उन्होंने अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए मुदिगेरे में वर्ष 1987 में सीठा चूड़ी भंडार की शुरुआत की। कुछ वर्षों के बाद, उन्होंने शादी कर ली और परिवार की आय बढ़ाने के लिए लकड़ी के व्यवसाय में प्रवेश किया। हालाँकि उन्होंने लकड़ी के व्यवसाय से पर्याप्त पैसा कमाया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे और इसमें काम करना बंद कर दिया। बाद में, उन्होंने दारदहल्ली में 15 एकड़ जमीन खरीदी और वर्ष 1995 में कॉफी, काली मिर्च, केला और सुपारी की खेती शुरू की। पांच साल के लिए, उन्हें अच्छी उपज मिली, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिली। हालांकि, 2002 और 2008 के बीच, कॉफी की दरों में 3,500 / - से रु। 700 / - रुपये से काफी कमी आई। । भले ही इस समय में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खेती करना नहीं छोड़ा। उन्होंने जारी रखा क्योंकि वह दृढ़ता से मानते थे कि अगर उन्होंने कड़ी मेहनत की और भक्ति के साथ खेती की तो वह कभी असफल नहीं होंगे। उन्होंने शहर छोड़ दिया और खेती पर अपने प्रयासों को पूरी तरह से केंद्रित करने के लिए 2004 से खेत में रहना शुरू कर दिया; इस समय तक, उनका बैंक ऋण लगभग रु.40 लाख बढ़ गया। उन्होंने बुरे दौर में जीवन के उतार-चढ़ाव का सामना करते हुए खेती जारी रखी। 2008 के बाद से, उन्हें कॉफी, काली मिर्च और सुपारी के लिए अच्छी कीमत मिलनी शुरू हुई। उन्होंने सरकार से कुछ सहायता के साथ किस्तों में बैंक ऋण चुकाना शुरू किया। श्री रमेश के अनुसार, काली मिर्च की खेती के लिए औसतन 60- 80 इंच बारिश की आवश्यकता होती है, और जून से अक्टूबर तक काली मिर्च के पत्तों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए ताकि उन्हें भारी बारिश से बचाया जा सके, और मार्च से मई तक , छिड़काव के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने रोपण फसलों के प्रभावी विकास के लिए फार्म यार्ड खाद (FYM) का उपयोग किया। उन्होंने बोर्दो पेस्ट को जमीनी स्तर से 2.5 फीट ऊपर इस्तेमाल किया और फसलों को रोगजनकों से बचाने के लिए नीम केक और ट्राइकोडर्मा लगाया। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों को जून और सितंबर के महीनों में भी लागू किया, जो 400 से 500 ग्राम तक एनपीके प्रति काली मिर्च के पौधे से लगाया गया। काली मिर्च के पौधों को भारी वर्षा के दौरान लीफ स्पॉट की बीमारी हो जाती है; इससे निपटने के लिए, उन्होंने बाविस्टिन (कार्बेन्डाजिन 50% डब्ल्यूपी) के एक स्प्रे का उपयोग करके निवारक उपाय किए। जड़ रोगों से बचने के लिए उन्होंने थिमेट का उचित आवेदन भी लिया। श्री रमेश का मानना है कि एक अनुभवी किसान एक वास्तविक कृषि वैज्ञानिक है। उन्होंने उल्लेख किया है कि काली मिर्च का पौधा बहुत संवेदनशील है, और इसके विकास के लगभग प्रत्येक चरण में विशेष देखभाल की जानी चाहिए। वह प्रति वर्ष 8 1/2 टन काली मिर्च, 450 बैग कॉफी और सुपारी और लगभग रु. 40 लाख उनकी वार्षिक आय के रूप में मिलता है । वह अपनी सफलता को कड़ी मेहनत, सही समय पर सही निर्णय लेने और फसलों की खेती के लिए वैज्ञानिक प्रथाओं को लागू करने का श्रेय देता है। उन्हें कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोग्गा, कर्नाटक द्वारा प्रगतिशील किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उन्हें ब्लैक गोल्ड लीग (बीजीएल), मुददेरे, चिक्कमगलुरु में एक काली मिर्च उत्पादक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार भी मिला। श्री रमेश का मानना है कि सफल खेती के लिए किसानों को 50 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं है; उन्हें समर्पण और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि युवा "कृषि और संबद्ध गतिविधियों को लें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे पैतृक व्यवसाय को संरक्षित रखें"।
आंध्र प्रदेश में मवेशी आधारित जैविक खेती का रुझान।
आंध्र प्रदेश में मवेशी आधारित जैविक खेती का रुझान। श्री गड्डे सतीश (47), वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और भारत के आंध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के सीतमपेटा गाँव, देंडुलुरु मंडल, एलुरु से हैं। वह वर्तमान परिदृश्य में भी खेती जारी रखते हैं, जहां कई किसानों को लगता है कि कीटों और बीमारियों, फसल की पैदावार में ठहराव, श्रम की कमी और खेती की उच्च लागत के कारण खेती किसी भी अधिक लाभदायक नहीं है। वह 16 एकड़ नारियल के बागान के मालिक हैं, 19 एकड़ में धान की खेती करते हैं और 20 एकड़ में मकई की। उनके पास 37 भैंसें भी हैं, जिनमें बछड़े, बछिया और वयस्क शामिल हैं। उन्होंने अपने पिता से मवेशी आधारित जैविक खेती के बारे में जाना और इसके साथ आगे बढ़े क्योंकि उनका मानना है कि यह सबसे अच्छी खेती प्रणाली है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। उन्होंने समकालीन युग में पशुपालक जैविक कृषि प्रणाली को जोखिम और अनिश्चितता के बावजूद जारी रखा क्योंकि उन्होंने 1990 के दशक से ही अपने परिवार में इस कृषि प्रणाली की सफलता का अवलोकन किया था। श्री सतीश के अनुसार, दोनों उद्यमों के बीच प पूरक संबंध के कारण डेयरी पशु जैविक कृषि प्रणालियों का हिस्सा हैं। मवेशी आधारित जैविक खेती के कई लाभों में से एक यह है कि महंगी रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता नहीं है, जिसके कारण उत्पादन लागत में कमी आती है, जो लंबे समय में ऊर्जा की बचत करती है और पर्यावरण की रक्षा करती है। वह दिन में खुली चराई करते हैं, और रात के समय में, जानवरों को एक लंबी रस्सी का उपयोग करके खेत में पंक्तियों में बांधा जाता है; वैकल्पिक दिनों में, जानवरों की आराम की जगह / स्थिति को बदलने के लिए रस्सी को कुछ मीटर आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरह से, जानवरों के गोबर और मूत्र को जमीन के इंसेटु द्वारा अवशोषण के लिए अनुमति दी जाती है। खेत की खाद, मिट्टी की उर्वरता को समृद्ध करती है और खरपतवार को कम करती है। श्री सतीश कहते हैं कि श्रम की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या को कम करने के लिए, वह नारियल के बागों के लिए सिंचाई की बेसिन पद्धति का उपयोग करते हैं। खुले चराई के साथ-साथ, वह पशुओं को चारे के समय दुबला धान खिलाता है। खेत की नहर के माध्यम से बाढ़ सिंचाई नारियल के पेड़ों की गहरी जड़ों के लिए अनुमति देता है और पौधे तनाव सहिष्णु हो जाता है। श्री सतीश कहते हैं कि प्राकृतिक चराई के कारण, पशु प्रजनन क्षमता और प्रजनन समस्याओं से प्रभावित नहीं होते हैं। चूंकि बछड़ों के लिए पूरा दूध छोड़ दिया जाता है, इससे बछड़ों को स्वस्थ होने में मदद मिलती है। उनके अनुभव के अनुसार, उचित प्रबंधन प्रथाओं से 24 महीने की उम्र में परिपक्वता और गर्भ धारण करने वाले जानवरों को जन्म दिया जाता है, जबकि अन्य मामलों में, इसमें अधिक समय लग सकता है। वह बिना किसी उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के, 19 एकड़ में व्यवस्थित रूप से धान उगाता है। वह कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के लिए मिट्टी में धान के अवशेष जोड़ता है, जो मिट्टी के सूक्ष्मजीवों को बनाने में मदद करता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। धान व्यवस्थित रूप से उगाया जाता है, जब एक बार काटा जाता है तो खेत में छोड़ दिया जाता है या एक सप्ताह के लिए सूख जाता है, फिर एक जगह पर ढेर लगा दिया जाता है और तीन महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद, धान को लगभग एक वर्ष के लिए संग्रहित किया जाता है, प्रीमियम मूल्य पर जैविक चावल के रूप में बेचा जाता है। उनका मानना है कि चावल की खेती की जैविक विधि में अकार्बनिक विधि की तुलना में अतिरिक्त पोषण मूल्य और स्वाद है। कृषि और पशुपालन विभागों में विस्तार अधिकारियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। उन्होंने खेती से संबंधित कई सेमिनारों और बैठकों में भी भाग लिया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) -इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च (IIRR), हैदराबाद द्वारा सर्वश्रेष्ठ मवेशी आधारित जैविक खेती अभ्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें एक प्रगतिशील किसान के रूप में पहचाना गया है और वे जैविक खेती के अपने समृद्ध ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वह कृषि और संबद्ध विभागों में किसानों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने अनुभव को साझा करने में संकोच नहीं करते। उनका मानना है कि जीवन शैली की बीमारियों के कारण जैविक उत्पादों की खेती की विश्वसनीयता, बाहरी आदानों पर कम निर्भरता, श्रम का न्यूनतम उपयोग और जैविक उत्पादों के लिए उच्च बाजार की मांग की वजह से मवेशी आधारित खेती जीवन का एक तरीका है। उन्होंने अपने फसल पैटर्न में प्रमुख कीटों के हमलों या बीमारियों का सामना नहीं किया है। जैविक चावल के लिए उन्हें प्रीमियम मूल्य मिलता है, जो 80 / - से रु। 100 / - प्रति किलो रुपये से शुरू होता है। वह जैविक खेती को एक संस्कृति और एक परंपरा मानता है। भविष्य में, वह बेहतर आय और स्थिरता के लिए भैंसों की संख्या में 37 से 60 की वृद्धि करना चाहता है। श्री सतीश ने बेहतर कृषि पद्धतियों को शिक्षित और प्रसारित करने के लिए कृषि-पर्यटन और डेयरी पर्यटन शुरू करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई है। उन्होंने किसानों को मूल्यवान सलाह दी है कि वे आर्थिक दृष्टि से और मौद्रिक लाभ के मामले में खेती पर विचार न करें, लेकिन इसे भावी पीढ़ी के लिए एक स्थायी तरीके के रूप में स्वीकार करें। उनका मानना है कि हर किसान को खेती के एकीकृत तरीके का पालन करना चाहिए क्योंकि यह पूरक और पूरक तरीकों से होता है जो फसलों की उत्पादकता को बढ़ाता है।
तेलंगाना के मिलेट मैन।
तेलंगाना के मिलेट मैन। श्री वीर शेट्टी बिरादर (44) भारत के तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले के गंगापुर गाँव, झारसंगम मंडल से हैं। वह एक स्नातक है और 13 एकड़ शुष्क भूमि और 5 एकड़ सिंचित भूमि का मालिक है। वह गन्ना, चना, लाल चना, ज्वार, बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा और फिंगर बाजरा उगाते हैं। एक बार, महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान, श्री बिरादर को खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिला और परिणामस्वरूप भुखमरी का सामना करना पड़ा। उन्होंने महाराष्ट्र से वापस आने के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने बाजरा उगाना शुरू किया और डॉ. सी. एल. गौड़ा, उप महानिदेशक, ICRISAT, और डॉ.सी.एच. रविंद्र रेड्डी, निदेशक, एमएसएसआरएफ (एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन), जेपोर, ओडिशा के तकनीकी मार्गदर्शन में मूल्य वर्धित बाजरा उत्पादों के क्षेत्र में प्रवेश किया। मूल्य वर्धित बाजरा उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने का एक कारण शहरी आबादी के बीच जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का उभरना और युवाओं में जंक फूड के सेवन की व्यापकता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2009 में, श्री बिरादर ने एसएस भवानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुडा कॉलोनी, चंदननगर, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में मिलों के लिए एक वैल्यूएड सेंटर शुरू किया। लिमिटेड सात साल की अवधि के भीतर, उनकी कंपनी ने सोरघम, बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा और फिंगर बाजरा से 60 मूल्य वर्धित बाजरा उत्पाद विकसित किए। वह दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की शुरुआत के साथ जून-जुलाई में बाजरा लेता है। वह उचित प्रबंधन प्रथाओं के साथ मिल्ट्स (फॉक्सटेल बाजरा 3-3.5 क्विंटल / एकड़, बाजरा 4-5 क्विंटल / एकड़, शर्बत 4-5 क्विंटल / एकड़ और उंगली बाजरा 4-5 क्विंटल / एकड़) से अच्छी उपज प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। सही समय भले ही उनके गांव में अल्प वर्षा हो। श्री बिरादर के अनुसार, बाजरा भविष्य की पीढ़ी के लिए सुपर खाद्य पदार्थ हैं क्योंकि पक्षी के नुकसान को छोड़कर, कीट और रोग के हमले का जोखिम तुलनात्मक रूप से कम है। उनका मानना है कि एक किसान और एक जवान हमारे देश की दो आंखें हैं। किसान को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने हैदराबाद के चंदननगर के हुडा कॉलोनी में स्वयंवर शक्ति नामक एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) की शुरुआत की। एनजीओ संगारेड्डी जिले के 8 गांवों के 1000 किसानों को शामिल करता है। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य किसानों को समय पर सूचना प्रसारित करना और नई तकनीकों को किसान समुदाय के घर-घर तक पहुंचाना है। श्री बिरादर ने भारतीय प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान (IIMR), हैदराबाद, तेलंगाना से बाजरा प्रसंस्करण, मशीनरी के प्रकार आदि के बारे में तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने IIMR के सहयोग से FARMER FIRST नामक एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) परियोजना के साथ भी काम करना शुरू किया। उन्होंने बाजरा आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों के कवरेज का विस्तार करने के लिए 27 फरवरी, 2017 को एक और मूल्य वर्धित केंद्र (दुकान) शुरू किया। उन्होंने MSSRF, जेपोर, ओडिशा में "पोषण सुरक्षा के लिए फसलों को कम करके" पर एक संगोष्ठी दी, जिसके बाद ओडिशा में किसानों को शिक्षित करने के लिए एक क्षेत्र का दौरा किया। उनका मानना है कि सभी बाजरा आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों को जगह के बावजूद सभी के लिए पूरे वर्ष उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्री बिरादर ने बाजरा आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों को विकसित करने की अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया और कहावत है कि "जर्नी के दौरान पत्थर और लाठी को केवल फल देने वाले पेड़ों पर ही फेंका जाता है"। एसएस भवानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रति माह 1 लाख वह रुपये कमाता है। मिस्टर स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF), जेयपोर, ओडिशा से 2017 में, बेस्ट फार्मर अवार्ड’, डॉ. एम वी राव मेमोरियल अवार्ड '2017 में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PJTSAU) और 2017 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च (IIMR) हैदराबाद से' बेस्ट मिलेट मिशारय्या अवार्ड ' सहित उल्लेखनीय मूल्य वाले उत्पादों के लिए श्री बिरादर के काम को कई पुरस्कारों के माध्यम से स्वीकार किया गया है। वो बाजरा आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के अलावा कृषि से सालाना 3-4 लाख कमाते है । भविष्य में, वह बाजरा खाद्य पदार्थों को तैयार करना शुरू करना चाहता है और देश भर में अधिकतम क्षेत्रों को कवर करना चाहता है।
सहजन (ड्रमस्टिक) खेती सक्सेस स्टोरी - बीड, महाराष्ट्र।
सहजन (ड्रमस्टिक) खेती सक्सेस स्टोरी - बीड, महाराष्ट्र। ओडिसा और मोरिंगा सहजन पौधे और ड्रिप सिंचाई प्रणाली किसानों को मुफ्त में गैर-सरकारी संगठनों की मदद से वितरित की गईं, जो मानवलोक अम्बजोगाई और सेव इंडियन फार्मर्स (एसआईएफ) जैसे सामाजिक कारणों के लिए समर्पित हैं। इस अवसर का उपयोग करते हुए, किसानों ने पानी के कुशल उपयोग से बंजर भूमि पर सहजन फसल लेकर बड़ी आय प्राप्त की है। यह वास्तव में मेहनती किसान श्री श्रीपति चन्नार की कहानी है, जो येल्डा गाँव से है, जो कि भारत के महाराष्ट्र से बीड जिले के अंबजोगाई ब्लॉक में स्थित है। वह पानी की कमी का सामना कर रहे ऐसे सूखा प्रभावित क्षेत्र में सहजन के उच्च फसल उत्पादन को लेने में सक्षम है। मानावलोक और सेव इंडियन किसान दोनों ने सहजन और ड्रिप सिंचाई किट के सहारे उसकी मदद की; परिणामस्वरूप वह इस गतिविधि से एक लाख रुपये की आय प्राप्त करने में सक्षम हुआ। येल्डा एक विकसित गांव है। वहां रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं। येल्डा के अधिकांश लोग पारंपरिक किसान हैं जो कृषि की पारंपरिक तकनीकों को लागू करते हैं, जो अक्सर सूखे और पानी की कमी से प्रभावित होते हैं। अधिकांश लोग अपनी फसल से पर्याप्त धन प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए वे अच्छी फसल पाने के लिए स्थानीय साहूकारों से बीज, उर्वरक, खाद खरीदने के लिए ऋण लेते हैं। यदि फसल इष्टतम नहीं है या फसल खराब होती है, तो किसान को ऋण बंद करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिए, किसान फिर से अधिक फसलें उगाने, उन्हें बेचने और पिछले ऋणों का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत ऋण लेता है। यह दुष्चक्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कई किसानों का कब्जा हो जाता है। इससे कई किसान आत्महत्या भी करते हैं। अब परिवार के सदस्य गरीबी में आगे बढ़ रहे हैं जो न केवल आर्थिक बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक 50 वर्षीय किसान श्रीपति चामर जो इस अत्यंत चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य रास्ता चुनते हैं। पहले वह कपास की फसल ले रहा था, लेकिन बदलते जलवायु और अपर्याप्त पानी के कारण उसे इससे पर्याप्त आय नहीं मिली। श्रीपति पारंपरिक खेती में वह हासिल नहीं कर पाए, जो उन्होंने हमेशा कुछ असाधारण, कृषि में अलग करने के लिए माना। इसके बाद श्रीपति को मानवलोक और सेव इंडियन फार्मर्स (एसआईएफ) दोनों के बारे में पता चला। इन दोनों एनजीओ ने श्रीपति जैसे कई किसानों को अपनी सहायता (ड्रमस्टिक पौधे और ड्रिप सिंचाई) दी ताकि वे सफलतापूर्वक उस स्थिति से बाहर आ सकें। इसके औषधीय उपयोग के कारण बाजार सहजन की बहुत मांग है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, श्रीपति चमनार ने अपने एक बार बांझ खेत में सहजन खेती को लागू किया। श्रीपति ने दो एकड़ में 1600 सहजन पौधे लगाए। ये पौधे क्रमशः 10 x 6 फीट और 1 × 1 फीट की गहराई पर बोए गए थे। उन्होंने जीवा-अमृत , गाय के गोबर का खाद / उर्वरक के रूप में उपयोग किया, जिसका अर्थ है कि वे शुद्ध जैविक खेती करते हैं क्योंकि इसके कारण वे अतिरिक्त खर्च को कम करने में सक्षम थे। सहजन के उपज 6 महीने के बाद शुरू हुए, इस सहजन के पौधे लगाए गए थे। आमतौर पर, सहजन फसल को किसी भी बीमारी, कीट का खतरा नहीं होता है। सहजन के पेड़ को कम जगह की आवश्यकता होती है जो किसान के लिए उच्च आय के साथ उच्च उत्पादन कम खर्च देता है। सहजन एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की कम खपत होती है, जिसमें शैल्फ जीवन होता है और कम प्रारंभिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। चूंकि सहजन को विकास के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, यह पानी की कमी वाले क्षेत्र में उगने वाली एक उपयुक्त फसल है। साथ ही, फसल उगाने के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जा सकता है। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि इसमें उच्च शैल्फ जीवन है, जिसका अर्थ है कि परिवहन और भंडारण के दौरान फसल खराब होने की संभावना न्यूनतम है। दरअसल, हफ्ते में 5 से 6 दिन इन पौधों की कटाई की जाती थी और एक हफ्ते में फसल ली जाती थी। प्रत्येक सहजन लगभग 2 से 2.5 फीट है। 5 से 6 ऐसे सहजन का वजन लगभग 1 किलो होगा। बाजार में इसकी कीमत 60 से 70 रुपये प्रति किलो है। इसी सहजन के खेतों में, उन्होंने भिंडी, बैंगन , टमाटर और मक्का की मिश्रित फसलें भी ली हैं। श्रीपति अब इस मौसम में 4000 किलोग्राम सहजन फसल उत्पादन से कम से कम दो लाख की आय की उम्मीद कर रहे हैं। कम निवेश से वह इस साल स्थिर आय अर्जित कर सकता है। इस प्रकार उनके जीवन स्तर और जीवन स्तर में सुधार होता है। श्रीपति कहते हैं, “मेरे गाँव येल्दा में ज्यादातर कपास की फसल ली जाती थी इसलिए मैं वैकल्पिक विकल्प खोज रहा था। जब मैंने मानवलोक के बारे में सीखा और भारतीय किसानों को बचाया, जो कृषि आय कुशल के माध्यम से किसानों के बेहतर जीवन को बेहतर बनाने के लिए सहजन वृक्षारोपण की पहल के साथ आए हैं, मैंने अपने खेत में इस गतिविधि को करने का फैसला किया। अब मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे पारंपरिक फसलों के बजाय सहजन के माध्यम से अधिक लाभ और आय प्राप्त हो रही है। ”