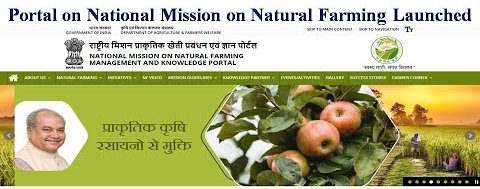# नबनिता दास का नर्स से किसान बनने का सफर# परिचय: असम के जोरहाट जिले के स्वर्गीय आनंद दास की बेटी सुश्री नबनिता दास एक युवा, ऊर्जावान और गतिशील प्रगतिशील महिला किसान हैं। हाई स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उन्होंने एक सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया। हालांकि उसने एक किसान की बेटी होने के कारण उसने हमेशा अपने दिल में एक 'किसान' का पालन-पोषण किया। प्रशिक्षण और प्रेरणा: एक नर्स के रूप में काम करते हुए, उन्होंने अस्पताल के रास्ते में सड़क के दोनों ओर हरे-भरे खेतों को देखकर खेती के प्रति आकर्षण विकसित किया। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने जोरहाट के एक सरकारी अस्पताल से नर्सिंग पेशा छोड़कर खेती को अपना व्यवसाय चुना और वर्ष 2010 से जैविक खेती शुरू की। अब वह एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान हैं और "नबनिता ऑर्गेनिक फार्म" की मालिक हैं। उनका पहला औपचारिक प्रशिक्षण 2014 में कृषि विभाग, असम सरकार (असम सरकार) द्वारा आयोजित बागवानी फसल पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। इसके बाद, उन्होंने कई बार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों (HMNEH), RKVY, असम कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (APART), असम सरकार के लिए बागवानी मिशन के तहत प्रशिक्षण में भाग लिया। उपलब्धियां: जिला कृषि विभाग, असम से प्रशिक्षण और सहयोग के साथ; असम कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र; उन्होंने एक प्रगतिशील किसान और कृषि उद्यमी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। अब वह एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान हैं और अपने गांव में "नबनिता ऑर्गेनिक फार्म" की मालिक हैं। उन्होंने बागवानी, मछली तालाब और पशुपालन आदि के एकीकरण के साथ एक मॉडल फूल फसल आधारित खेती प्रणाली मेंरैंजड और सुनकेन पद्धति को अपनाकर अपनी पिछली विशिष्ट मोनो फसल चावल भूमि को परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में उसका खेत फूलों (एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लैडियोलस, ट्यूबरोज आदि), चावल, विभिन्न दालें, तिलहन, फल और सब्जियां, मछली (स्थानीय प्रकार और कार्प), अंडे, दूध, बकरी और विभिन्न पोल्ट्री नस्लों जैसे के सिल्की चिकन, रेनबो रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ, तुर्की, गुनिया मुर्गी; कबूतर ((मसोकाली); बत्तख की नस्लें (व्हाइट पेइकिन), भारतीय धावक और देशी बत्तख उत्पादन के साथ एक छोटा कृषि केंद्र बन गया है। उसके खेत की सुंदरता यह है कि उसने कृषि भूमि के हर इंच का उपयोग ऊर्ध्वाधर स्थान का उपयोग करके उत्पादक संपत्ति के रूप में किया है। हाल ही में उसने वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन शुरू किया है और अजोला संस्कृति। सरकारी हस्तक्षेप से पहले जमीन से उसकी कमाई केवल 4000 रुपये थी। अब वह पहले वर्ष (2014) में 30,000 रुपये शुद्ध लाभ कमाती है, दूसरे वर्ष (2015) में 56,000 रुपये, तीसरे वर्ष (2016) में 96,000 रुपये, चौथे वर्ष (2017) में 1,10,000/- रुपये और 2019 में 1,25,000/- रुपये। योगदान देने वाले कारक: जैविक खेती के बारे में, वह हमेशा कहती हैं कि, 'उत्पादन की कम लागत, सर्वोत्तम स्वाद के साथ गुणवत्ता वाली उपज और अच्छी प्रीमियम कीमत जैविक उत्पादन प्राप्त करने का अवसर वास्तव में आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। चूंकि मेरे इलाके के साथ-साथ मेरे नजदीकी शहर जोरहाट में भी इसकी अच्छी मांग रही है, जहां स्थानीय लोगों के साथ-साथ विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के खरीदार इन उत्पादों को खरीदने के लिए उत्सुकता से तैयार हैं। वास्तव में मेरी जैविक खेती और इसकी उपज ने मुझे एक व्यवहार्य आय प्रदान की है जो मुझे अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। नर्सिंग से खेती में बदलना मेरी वित्तीय सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है।' वह केटेकी जोहा, कुनकुनी जोहा, कोलाजोहा इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के स्वदेशी सुगंधित चावल जीनोटाइप की खेती और संरक्षण करती है। इसके अलावा वह काले चावल की खेती कर रही है जो मणिपुर में उत्पन्न हुई है और इसका काले चावल के विभिन्न उत्पाद बनाने में उपयोग किया जाता है । पुरस्कार और मान्यता: कृषि के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के लिए, उसने कुछ विशेष पुरस्कार हासिल किया। 1 असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट में भारत के उपराष्ट्रपति, 2018 द्वारा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार। 2 2018 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पटना द्वारा "अभिनव चावल किसान पुरस्कार"। 3 महिला किसान दिवस, 2018 के अवसर पर नई दिल्ली में 'प्रगतिशील महिला किसान पुरस्कार'। 4 विभिन्न अवसरों पर उन्हें माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और असम के माननीय कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। 5 इसके अलावा, वर्ष 2019 में उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित असमराज्य के अन्य प्रगतिशील किसानों के साथ-साथ नवीन खेती प्रथाओं के बारे में जानने के लिए वियतनाम जाने का अवसर प्राप्त किया। 6 कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने उन्हें अपनी यात्रा के माध्यम से प्रोत्साहित किया है जिसमें असम के माननीय मुख्यमंत्री, असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय कृषि मंत्री (जीओए) और असम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हैं। अन्य किसानों पर प्रभाव: उनकी सफलता की एक झलक पाने के लिए कई किसान और युवा उनके खेत में जाते हैं और कई उनके नक्शेकदम पर चलते हैं।
Farmer Success Stories
!.......बेकार पड़ी थी 10 एकड़ जमीन, महिला ने अपने जज़्बे से शुरू की ऑर्गेनिक खेती, बन गई कामयाब किसा
!........बेकार पड़ी थी 10 एकड़ जमीन, महिला ने अपने जज़्बे से शुरू की ऑर्गेनिक खेती, बन गई कामयाब किसान.......! मदुरै (Madurai) की रहने वाली 54 साल की पी. भुवनेश्वरी (P. Buvaneshwari) की कामायाबी के पीछे भी उनका दृढ़ विश्वास ही है| पी. भुवनेश्वरी ने जब जैविक खेती (Organic Farming) करने का फैसला किया, तो कई लोग उनके इस निर्णय से सहमत नहीं थे. मगर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने फैसले को सही साबित कर दिखाया| प्रकृति की गोद में पली-बढ़ी....! पी. भुवनेश्वरी का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले (Tamil Nadu’s Thanjavur District) के कल्याणाओदई गांव (Kalayanaoai Village) में एक किसान परिवार में हुआ था| भुवनेश्वरी प्रकृति की गोद में पली-बढ़ी हैं| उनके घर के पास से कावेरी नदी की कल-कल करती धारा बहती थी| लिहाजा, वो हमेशा से प्रकृति के पास ही रहना चाहती थीं| पी. भुवनेश्वरी कहती हैं कि बचपन से ही उनके खेत और गांव में पैदा होने वाले कई तरह के फल और सब्जियां आसानी से उन्हें मिलते रहे हैं| वो कहती हैं कि जब उनके घरवाले खेतों में जाते थे, तो वो भी जाती थीं और बड़े ध्यान से देखती और समझती थीं कि कैसे खेती की जाती है| उसी समय से उन्हें खेती में रुचि पैदा हो गई थी| ससुराल में किया फैसला.....! शादी के बाद पी. भुवनेश्वरी मदुरै के पुदुकोट्टई करुप्पयुरानी गांव आ गईं | अपने ससुराल में उन्होंने शौकिया तौर पर फूल लगाना शुरू किया| जब भुवनेश्वरी ने पूरी तरह से खेती करने का फैसला किया तो उन्होंने अपने सामने दो लक्ष्य रखे- पहला कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना है और दूसरा चावल की देसी किस्मों का फिर से उत्पादन करना है| भुवनेश्वरी ने अपने परिवार से 10 एकड़ के खेत में से 1.5 एकड़ खाली जमीन मांगी ताकि वह प्राकृतिक रूप से घर के लिए खेती कर सकें| खेती का फैसला तो ठीक था, लेकिन बगैर कीटनाशक का प्रयोग किए खेती करने के निर्णय पर कोई भी सहमत नहीं था| यहां तक की खेतिहर मजदूरों को भी उनके इस निर्णय पर भरोसा नहीं था| मगर भुवनेश्वरी को यकीन था कि वो पूरी तरह से जैविक खेती कर सकती हैं| अपनी किचन गार्डेनिंग के अनुभव के आधार पर उन्होंने खेती करना शुरू किया| जैविक खेती के लिए ट्रेनिंग भी ली....! साल 2013 में उन्होंने जैविक खेती का प्रयोग शुरू किया| वह प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली सब्जियों, अनाज और फलों के लिए एक आसान तरीका चाहती थीं| लिहाजा उन्होंने जैविक खेती के बारे में अधिक जानने के लिए करूर स्थित वनगम नम्मलवर इकोलॉजिकल फाउंडेशन (Vanagam Nammalvar Ecological Foundation, Karur) से संपर्क किया| फाउंडेशन ने उनका पूरा सहयोग किया| मेहनत लाई रंग.....! आहिस्ता-आहिस्ता उनकी मेहनत रंग लाई और लोगों को उन पर भरोसा हो गया| आज की तारीख में पूरे 10 एकड़ की खेत में बगैर किसी केमिकल और कीटनाशकों का प्रयोग किए हुए लहलहाती फसल हो रही है| अब भुवनेश्वरी लोगों को अपने खेत दिखाने के लिए बुलाती भी हैं| साथ ही उन्हें बताती हैं कि कैसे पूरी तरह से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती की जा सकती है|
जैसलमेर के खजूर फॉर्म ने बेचे 50 लाख के खजूर:भोजका गांव में 13 साल पहले लगा भारत का सबसे बड़ा खजूर फॉ
जैसलमेर के खजूर फॉर्म ने बेचे 50 लाख के खजूर:भोजका गांव में 13 साल पहले लगा भारत का सबसे बड़ा खजूर फॉर्म, हर साल 400 टन खजूर देता है। जैसलमेर के भोजका गांव में लगे खजूर फॉर्म हाउस ने किसानों को करीब 50 लाख के खजूर के पौधे बेचे। पूरे प्रदेश के किसानों ने इस साल इस खजूर फॉर्म हाउस से खजूर के पौधे खरीद कर अपने जिलों में लगाने के लिए ले गए हैं। प्रदेश में खजूर की खेती अब फलफूल रही है। इस खेती से किसान खजूर की पैदावार करके लाखों रुपए का मुनाफा कमाएंगे। भोजका गांव में लगे करीब 100 हेक्टेयर में फैले खजूर के फॉर्म हाउस में करीब 400 टन खजूर मिल रहा है। भारत- इजरायल परियोजना से मिल रहा खजूर प्रदेश में खाड़ी देशों की तरह खजूर की खेती का क्रेज बढ़ता जा रहा है। भारत-इजरायल परियोजना के तहत साल 2008 में जिले के भोजका गांव में 15 हजार खजूर के पौधों का एक फार्म तैयार किया गया। सरकार के कृषि विभाग ने गुजरात की अतुल कंपनी के सहयोग से भोजका में खजूर का खेत तैयार किया था। उस समय यहां 15 हजार 500 पौधे लगाए गए थे। 4 साल बाद फल लगना शुरू हुआ और अब रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। जानकारी के अनुसार इस फार्म में सालाना 400 टन खजूर का उत्पादन होता है। ये फॉर्म हाउस करीब 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें खजूर की 9 किस्में लगाई जाती हैं। हर साल 400 टन खजूर का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश के किसानों में भी अब खजूर की खेती को लेकर क्रेज बढ़ गया है। यहां खजूर की मांग अब पूरे देश में बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर के किसानों ने अब अपने खेतों में खजूर की खेती शुरू कर दी है। 50 लाख के पौधे बेचे सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स फॉर खजूर उद्यान के उपनिदेशक प्रताप सिंह कुशवाहा ने बताया कि हमारे यहां खजूर के पौधे तैयार करके किसानों को बेचा भी जा रहा है और किसान खजूर कि खेती को सीखकर बड़ी संख्या में खेती के लिए इन पौधों को लेकर जा रहे हैं। एक पौधे की कीमत 1500 रुपये है। हालांकि सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जाती है। लेकिन खजूर के खेत में पौधे का पूरा पैसा मिलता है। इस साल भी खजूर के खेत में चार हजार पौधे लगाने का लक्ष्य है। जिस पर फार्म द्वारा 4 हजार 105 पौधे तैयार किए गए हैं। जिसमें से 3 हजार 892 पौधे भी किसानों को बेचे जा चुके हैं। खजूर की खेती से भी 50 लाख रुपये की कमाई हुई है। इसके अलावा बाकी बचे 2 हजार पौधे तैयार हैं और करीब 30 लाख के पौधे और बिकेंगे।
पुरस्कार विजेता किसान मावूराम मल्लिकार्जुन रेड्डी कीसॉफ्टवेयर से कृषि तक की यात्रा की कहानी।
पुरस्कार विजेता किसान मावूराम मल्लिकार्जुन रेड्डी कीसॉफ्टवेयर से कृषि तक की यात्रा की कहानी। कहानी 2014 में शुरू हुई जब बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) में स्नातक और सिमेंटिक स्पेस टेक्नोलॉजीज के एक कर्मचारी मल्लिकार्जुन ने हैदराबाद में अपनी सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़ दी। उनके परिवार के लिए खेती कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने अपने किसान-पिता और रोल मॉडल लक्ष्मी रेड्डी के स्वामित्व वाली 12 एकड़ जमीन ग्रहण की और धान के साथ एक अर्ध-जैविक खेत - एक अनोखा रास्ता जुताई करना शुरू कर दिया। चूंकि परिणाम अपेक्षित नहीं थे, उन्होंने ड्रिप सिंचाई में धान की खेती की और फिर संकर लाल चने की खेती की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन (SRI) खेती पद्धति का पालन किया। वह हैदराबाद के बाहरी इलाके राजेंद्रनगर में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि नवाचारों का पालन करके लगातार ज्ञान बढ़ाते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय से सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार भी जीता। अब, वे कहते हैं, उनकी जैविक खेती से उन्हें अन्य किसानों की तुलना में अधिक लाभ मिलता है। यदि नियमित खेती के लिए 60 क्विंटल धान के लिए ₹50,000 के निवेश की आवश्यकता होती है, तो मल्लिकार्जुन उत्पादन प्राप्त करने के लिए ₹1,13,000 के सकल राजस्व के साथ केवल ₹25,000 का निवेश करता है। उनके आईसीएआर पुरस्कार का एक प्रमुख कारण कम निवेश करने और बड़ा रिटर्न प्राप्त करने की उनकी क्षमता थी। एकीकृत खेती में मल्लिकार्जुन के प्रयासों, भूजल में वृद्धि के लिए खेत के तालाबों और खुले कुओं के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कीटनाशकों के दुरुपयोग और पराली प्रबंधन पर अन्य किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के प्रयासों की भी सराहना की गई है। दिलचस्प बात यह है कि मल्लिकार्जुन बिना श्रमिकों के अकेले ही खेतों का प्रबंधन करते हैं। तकनीकी विशेषज्ञ से किसान बने केपीएचबी कॉलोनी में एक जैविक दुकान भी खोली है, जहां वह अपने गांव के किसानों के एक समूह की उपज बेचते हैं। वे बताते हैं, "जैविक खेती पर्यावरण को बनाए रखती है। छोटे किसानों को खेती और अपनी आजीविका को भी बनाए रखने के लिए छोटी शुरुआत करनी होगी।”
कनक लता, उत्तप्रदेश की एक प्रेरणादायक महिला किसान, जो प्रति दिन 7 क्विंटल जैविक टोमैटो का उत्पादन ले
कनक लता, उत्तप्रदेश की एक प्रेरणादायक महिला किसान, जो प्रति दिन 7 क्विंटल जैविक टोमैटो का उत्पादन लेती है, जो यूके और ओमान में निर्यात होता है। उत्तर प्रदेश के विट्टलपुर से कनक लता, टमाटर की दुर्ग और आर्यमन किस्मों को उगाती है जो अब स्थानीय लोगों और विदेशियों के लिए एक हिट है। 2017 में, कनक लता के पति वासुदेव पांडे की एक सहकारी बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद, दंपति अपने बेटे के साथ कुछ महीने बिताने के लिए यूएसए गए। लेकिन, कुछ समय बाद, दंपति ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित विट्टलपुर गांव में अपनी सेवानिवृत्ति के लिए भारत लौटने का फैसला किया। अपने खर्च का समर्थन करने के लिए कोई पेंशन नहीं होने के कारण, पति और पत्नी ने अपने 1.5 एकड़ के खेत में खेती शुरू करने का फैसला किया। हालांकि, उनमें से किसी को भी आवश्यक अनुभव नहीं था। कनक कहती हैं, "हमारे दोनों परिवारों की कृषि में पृष्ठभूमि है, और मैंने हमेशा अपने दादा और दूसरे रिश्तेदारों को खेत में देखा।" 57 वर्षीय कनक ने अपने परिवार से बहुत कम जानकारी के साथ शुरुआत की कि गेहूं, मटर और टमाटर कैसे उगाए जाते हैं। लेकिन वह परिणाम से संतुष्ट नहीं थी। “उपज बहुत कम थी, और फसल अस्थिर थी। मिट्टी की उर्वरता खराब थी और पड़ोसी किसानों ने हमें कम उपजाऊ भूमि में सब्जियां उगाने के बारे में ताना मारा, ”वह कहती हैं। कुछ असफलताओं के बाद, कनक ने खेती के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण किया और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, जो हर दिन 7 क्विंटल की कटाई में सक्षम था। उनके जैविक खेत से न केवल नजदीकी बाजारों में मांग बढ़ी है बल्कि यूके और ओमान के ग्राहकों को भी आकर्षित किया है। कनक ने स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए। इसके लिए, उन्होंने नव चेतना कृषि केंद्र निर्माता कंपनी लिमिटेड से परामर्श किया, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के एक सहयोगी उपक्रम है। जैविक खेती के प्रशिक्षण के तहत, उन्होंने अपने खेत में आवश्यक बदलाव करने के लिए दिल्ली में प्रयाण संस्थान से 50,000 रुपये का ऋण लिया। कनक कहते हैं, "मैंने टमाटर उगाने और जैविक खाद, वर्मीकम्पोस्ट के साथ जमीन का इलाज करने और अन्य प्राकृतिक तत्वों से समृद्ध करने का फैसला किया।" अगस्त 2020 में, उसने दो किस्मों के टमाटर लगाए - दुर्ग और आर्यमान। “मैंने हाल ही में दुर्ग वैरायटी की कटाई की है जो तुरंत बाजार में लोकप्रिय हो गई है। मैंने प्रति क्रेट 100 रुपये [नियमित टमाटर की तुलना में] कमाया। टमाटर कम खट्टा और ज्यादा रसीला होता है और जीवन अवधि भी ज्यादा है । जिला बागवानी अधिकारी (डीएचओ), मेवाराम, ने भी खेत का दौरा किया और कनक की उपज से नमूने लिए। वह कहते हैं, “टमाटर रेफ्रिजरेटर में रखे बिना कम से कम दो सप्ताह तक रह सकता है। वे अन्य देसी किस्मों की तुलना में लंबे, गोल और बेहतर स्वाद के हैं। ” कनक हर दिन 50 क्रेट फलों की फसल लेने का दावा करती है। “प्रत्येक टोकरा 25 किलो का होता है। मैंने एक अच्छी आय अर्जित की जिससे ऋण और अन्य निवेशों को चुकाने में मदद मिली। वह कहती हैं कि जल्द ही मुनाफा होने लगेगा और मुझे लगभग 2.5 लाख रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है। नव चेतना एग्रो सेंटर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ मुकेश पांडे कहते हैं, “वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, जैसे मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन और अन्य पहलुओं ने कनक को सफलता हासिल करने में मदद की। टमाटर को राजभवन भेजा गया और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इसकी सराहना की गई। अपने लोकप्रिय टमाटर के कारण वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गई हैं। मुकेश कहते हैं कि कनक की सफलता ने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "वे अगले सीजन में टमाटर की किस्म बढ़ाएंगे।" कनक कहती हैं कि खेती के तरीकों को सीखने के अलावा, उन्होंने मजदूरों की कमी, पानी की आपूर्ति और तकनीकी कठिनाइयों जैसे मुद्दों पर काबू पाया। अपनी उपलब्धि से संतुष्ट, कनक शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और काले टमाटर के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। “मैं कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के कारण सफलता का स्वाद चख सकती थी । यह जानकर अच्छा लगता है कि लोग कृषि उपज को पसंद कर रहे हैं और मुझे बार-बार ग्राहक मिलते रहते हैं। फलते-फूलते खेत का नजारा संतोषजनक है। और मेरे पति ने इस प्रयास में मेरी मदद की है, ”वह कहती हैं। कनक ने सभी किसानों से पानी और बिजली बचाने के लिए सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने का आग्रह किया। “मिर्जापुर एक पहाड़ी क्षेत्र है, और किसानों को अक्सर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। ड्रिप सिंचाई से कम पानी की खपत और उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को वैज्ञानिक तरीकों पर भरोसा करना शुरू कर देना चाहिए और पारंपरिक खेती छोड़ देनी चाहिए।
फसल अवशेषों को अपने एमजीएमटी से जलाने से किसान की सफलता की कहानी।
फसल अवशेषों को अपने एमजीएमटी से जलाने से किसान की सफलता की कहानी। फतेहगढ़ साहिब जिले के बोंगा ज़ीर गाँव के 39 वर्षीय किसान पलविंदर सिंह ने फसल अवशेषों का प्रबंधन करके साथी किसानों के लिए एक मिसाल कायम की है। सहकारी प्रबंधन में स्नातकोत्तर और उच्च डिप्लोमा, पलविंदर सिंह ने समाज की भलाई के लिए किसान बनने के अपने बचपन के सपने को आगे बढ़ाने के लिए खेती की। वह 20 साल के खेती के अनुभव के साथ 22 एकड़ में - खुद का और 16 पट्टे पर 6 एकड़ में खेती करता है। चावल-गेहूं; चावल-आलू; और चावल-आलू-सूरजमुखी उसके द्वारा अपनाई गई मुख्य फसल प्रणाली है। 1998 से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किसान मेले के शौकीन होने के नाते, उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) द्वारा प्रसारित नई तकनीकों से मोहित किया गया है। 2006 में, वह कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), फतेहगढ़ साहिब से जुड़ गए। प्रारंभ में, उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, फतेहगढ़ साहिब से संसाधनों के संरक्षण पर प्रशिक्षण प्राप्त किया, और प्राकृतिक संसाधनों - हवा, मिट्टी और पानी को बचाने के लिए प्रेरित किया। “मैंने फतेहगढ़ साहिब कृषि विज्ञान केंद्र का कई बार दौरा किया और क्षेत्र में पुआल का उपयोग करने के लिए विभिन्न साधनों और तरीकों पर चर्चा की और परिणामस्वरूप कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए मिट्टी में पुआल को शामिल करने की कोशिश की। यह 2007 में मेरी एक यात्रा के दौरान था जिसमें मैं 'खुश बीजक' के रूप में आया था। 2008 में, पीएयू से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. एचएस सिद्धू और ऑस्ट्रेलिया से डॉ. जॉन ब्लैकवेल के मार्गदर्शन में, मैंने अपने 1.5 एकड़ जमीन पर खुश बीज बोने के साथ गेहूं बोया, ”उन्होंने आगे कहा। लेकिन शुरुआती वर्षों में किसान के लिए पुआल प्रबंधन अभियान एक कठिन कार्य था। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) की डॉ. नवजोत कौर ढिल्लों ने कहा कि कई बार उनके दोस्तों ने उन्हें हतोत्साहित किया और उन्हें धान के पुआल को जलाने और बिना किसी अतिरिक्त लागत के खेत तैयार करने का सुझाव दिया। “खुशहाल सीडर के साथ गेहूँ बोना जब खेतों में अभी भी पड़ा था, एक विचार था जो कई लोगों को स्वीकार्य नहीं था। मैं परिवार और दोस्तों के लिए हंसी का पात्र बन गया, जिन्होंने मुझे अक्सर कहा था कि इस तरह से बुवाई करने से खेतों पर अंकुरण नहीं होगा। लोग कहते थे कि मेरी शिक्षा पिछड़ गई है और मैं पागल हो गया हूं। हतोत्साहित करने के बावजूद, मेरी माँ जसवीर कौर और पैतृक चाचा हुकुम सिंह मेरी तरफ से खड़े थे, ”उन्होंने साझा किया। पहले साल में, खुश बीज बोने वाले गेहूं ने संतोषजनक परिणाम नहीं पाए, लेकिन वह नवाचार को अपनाने के लिए दृढ़ था, चाहे वह कोई भी हो। अगले साल, कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ संशोधनों और प्रेरणा के साथ उसी प्रथाओं का पालन करते हुए, वह मिट्टी की उन्नत गुणों के साथ बम्पर फसल प्राप्त करने में सक्षम था। दोस्तों से अलगाव के इन वर्षों में, उनका एकमात्र साथी उनका स्मार्ट फोन था, जिस पर उन्होंने तस्वीरें और वीडियो कैप्चर किए, जिसे बाद में उन्होंने खुशहाल बीजक खेतों से अच्छी फसल लेने के बाद साथी किसानों के साथ साझा किया। गेहूं की फसल की प्रभावशाली वृद्धि और उपज के साथ, वह शहर की चर्चा बन गया, जो कि प्रशंसा की तरह है। 2010 में, उन्होंने अपने गाँव के कई किसानों को खुशहाल बीजक के साथ कम से कम एक एकड़ गेहूं बोने के लिए प्रेरित किया और 20 से अधिक किसानों ने उनकी इच्छा पर भरोसा किया। कुछ ही समय में, वह किसानों के लिए एक आदर्श बन गया। 2008 के बाद से, वह खुश बीज के साथ गेहूं बो रहा है। अन्य किसान सूट का पालन करते हैं। शहीद भगत सिंह यूथ वेलफेयर क्लब, ब्रोंगा ज़ीर के सदस्य होने के नाते, पलविंदर सिंह ने अपनी तकनीक के परिणामों को दिखाकर आसपास के ग्रामीणों को प्रेरित किया। इसके बाद, किसानों ने लेजर लैंड लेवलर और हैप्पी सीडर जैसी संसाधन संरक्षण तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया। पलविंदर सिंह के खेतों पर नवाचार के परिणामों का गवाह बनने के बाद, तीन किसानों - लखवीर सिंह, गुरजंत सिंह और मनजीत सिंह ने खुश बीज खरीदे। उनमें से चार ने एक समूह बनाया और उनके खुशहाल बीजकों को आसपास के गांवों के किसानों को पट्टे पर दे दिया गया - बरौंगा बालुंद, सलाना, रतनपालो, कुंभ, और कुंभरा। 2017 में, पंजाब भर के कई किसानों ने उन्हें इन सभी वर्षों के दौरान PAU खुश बीजर के साथ अपने अनुभव को जानने के लिए बुलाया।
छिदामी यादव- बुंदेलखंड के जैविक किसान की सफलता की कहानी।
छिदामी यादव- बुंदेलखंड के जैविक किसान की सफलता की कहानी। 52 साल के छिदामी यादव को नंदनपुर में कृषि / खेती में 40 साल का अनुभव है। उसके पास 10 एकड़ जमीन है, लेकिन पानी के संकट के कारण, वह केवल 2-4 एकड़ का उपयोग करने में सक्षम है। वह रबी सीजन के दौरान गेहूं और मोती बाजरा उगाता है। खरीफ के मौसम में, वह अपने बेटों के साथ नौकरी की तलाश में शहर में प्रवास करता है। उसके पास पशुधन भी है - 25 बकरियां जिनका गोबर जैविक खाद तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है, 15 भैंस जिनका दूध रुपये में बेचा जाता है। 30 / लीटर, 500 रुपये किलो पर घी, पड़ोस को बांटी गई छाछ और खाद के रूप में इस्तेमाल होने वाला गोबर। उसके पास 3 गायें भी हैं जिनकी उपज का उपयोग घर पर किया जाता है। परमार्थ समाज सेवा संस्थान के हस्तक्षेप के बाद, रबी के मौसम में उन्होंने एसडब्ल्यूआई और एसवीआई जैसी कम लागत वाली कृषि प्रथाओं के बारे में सीखा। उन्होंने 1 एकड़ में गेहूं, 1 एकड़ में चने और 1 एकड़ में जौ उगाया है। खरीफ के इस मौसम में उन्होंने अपनी 1 एकड़ जमीन में जैविक तरीके से टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, धनिया, तारो की जड़ें, आलू, करेला, प्याज, कद्दू और गिल्की जैसी सब्जियां उगाई हैं। उन्होंने कहा कि वह इस सूखे के मौसम में जैविक सब्जी की खेती करके बहुत खुश हैं। परमार्थ के समर्थन के बाद, उनके पास सिंचाई के लिए एक कुएं के अलावा अपना खुद का बोरवेल रिचार्ज है। वह सप्ताह में दो बार अपनी सब्जी की उपज पास के गोर गांव में बड़े बाजार में बेचता है और लगभग 500 रुपये प्रति बाजार की कमाई करता है। उन्होंने कहा कि परमार्थ टीम के साथ काम करने से उन्हें नए सीखने के अनुभव प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से जैविक खेती के संबंध में, अर्थात्, रोजमर्रा की सामग्री का उपयोग करके जीव अमृत 1 और अमृत पाणि 2 बनाना। जब इस कार्यक्रम से उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने बाजार से कीटनाशक और सब्जियां खरीदने के लिए पैसे नहीं बचाए हैं। उसे विश्वास दिलाया जाता है कि वह और उसका परिवार स्वस्थ, जैविक सब्जियों को अपने खेत में उगाते हैं। इस सीजन में, वह 4 क्विंटल चना, 12 क्विंटल गेहूं और 10 क्विंटल जौ का उत्पादन करने में सक्षम था। सब्जी मंडी से उनकी कमाई ने उन्हें अपने पोते की शिक्षा और जीवन स्तर के लिए अधिक खर्च करने में मदद की है। 1 एकड़ जमीन के लिए जीव अमृत तैयार करने की विधि। सामग्री: पानी - 200-250 लीटर गोबर - 10- 15 किलोग्राम गोमूत्र- 3-4 लीटर गुड़ - 1-2 कि.ग्रा प्रक्रिया: सभी सामग्री को मिलाएं और 3-4 दिनों के लिए छाया में रखें। मिश्रण को दिन में एक बार हिलाएं और यह 4 वें दिन तक उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। अमृत पानी तैयार करने की विधि सामग्री: पानी - 200 लीटर गोबर - 10 किग्रा देसी घी - 250 ग्राम शहद - 500 ग्राम प्रक्रिया: सभी सामग्रियों को मिलाएं और फसल बोने के बाद खेत में छिंड़काव करे।
झारखंड के राजेंद्र बेदिया नाम के किसान ने पीले ताइवानी तरबूज की खेती कर भारतीय कृषि में एक नया अवसर
झारखंड के राजेंद्र बेदिया नाम के किसान ने पीले ताइवानी तरबूज की खेती कर भारतीय कृषि में एक नया अवसर पैदा करके एक मिसाल कायम की है । झारखंड के एक किसान ने पीले तरबूज की पैदावर की है. किसान का नाम राजेंद्र बेदिया है. उन्होंने इस ताइवानी तरबूज की खेती करके एक मिसाल कायम कर ली है. अब पूरे क्षेत्र में लोग उनसे इस खेती के बारे में पूछ रहे हैं. राजेंद्र ने इन तरबूजों से लागत की तीन गुनी कमाई कर ली है । राजेंद्र रामगढ़ के गोला प्रखंड के चोकड़बेड़ा गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने पहली बार तरबूज की खेती का प्लान बनाया. लेकिन, उन्होंने देसी नहीं ताइवानी तरबूज को उगाने का प्लान किया. इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन ताइवानी तरबूज के बीच मंगाए. बस फिर क्या उनकी मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है । राजेंद्र के ये तरबूज अब बड़े हो गए हैं. पीले तरबूज का रंग और आकार लाल तरबूज की तरह ही है. लेकिन, काटने पर ये पीला नजर आता है. इस तरबूज को अनमोल हाइब्रिड किस्म का तरबूज कहते हैं. इसका रंग बाहर से सामान्य हरा और अंदर से पीला होता है. यह स्वाद में ज्यादा मीठा और रसीलापन लिए रहता है । 10 ग्राम अनमोल किस्म के ये बीच 800 रुपये के मिले. इसके बाद प्रयोग के तौर पर एक छोटे से खेत में प्लास्टिक मंचिंग और टपक सिंचाई तरीके से खेती की. अब 15 क्विंटल से अधिक पीले तरबूज की खेती हुई है. उनका अनुमान है कि उन्हें 22 हजार की आमदनी हो सकती है. यह लागत मूल्य से तीन गुना ज्यादा है ।
जीरो बजट खेती का एक वास्तविक उदाहरण।
जीरो बजट खेती का एक वास्तविक उदाहरण। श्री मल्लेशप्पा गुलप्पा बिरसोट्टी हिरेगंजल गाँव, कुंदगोल तालुका, धारवाड़ जिले, कर्नाटक, भारत से हैं। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र को एक संक्रमणकालीन बेल्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। 1990 के बाद से, क्षेत्र में मानसून की बारिश की शुरुआत काफी कम हो गई है और किसानों को आस-पास के गांवों से पीने का पानी लाना पड़ता है और कृषि कार्यों के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इन कठिन परिस्थितियों में, श्री बेसरोटी ने फसल उत्पादन के लिए एक वैकल्पिक पद्धति के रूप में जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाया। वह पिछले एक दशक से लगातार जैविक खेती कर रहे हैं। उन्होंने फार्म यार्ड खाद (FYM), कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट का उपयोग करके जैविक कृषि अभ्यास शुरू किया। चार वर्षों के उपयोग में, उन्होंने देखा कि उनकी फसलें बेहतर हो रही हैं और उन्होंने वर्मी-कम्पोस्ट के विकास और इसके सतत अनुप्रयोग में रुचि विकसित की है। उन्होंने कृषि फसल उत्पादन में एक शून्य निवेश पद्धति तरल जीवनमूर्ति जैविक तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन पकड़ यह थी कि तरल जीवमृथा तैयार करने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता थी। पानी की कमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने ठोस जीवामृत का प्रयोग शुरू किया और पिछले छह वर्षों में फसलों को बढ़ाने में सफल रहे। ठोस जीवामृत एक स्थानीय गाय या बैल से 10 किलो गोबर, 250 ग्राम दाल का आटा (कोई भी), 250 ग्राम गुड़, 500 ग्राम मिट्टी और 1.5 से 2.0 लीटर मवेशी के मूत्र से तैयार किया जाता है। इन उत्पादों को अच्छी तरह से मिलाया जाता है और एक ढेर को छाया के नीचे बनाया जाता है और 24 घंटे के लिए थैली से ढक दिया जाता है। अगले दिन, थैली को हटा दिया जाता है और उत्पादों को 25-30 दिनों के लिए छाया में सुखाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ठोस जीवमृथा का कंकड़ रूप होता है। फिर, कंकड़ को बारीक और मोटे कणों को अलग करने के लिए बोया जाता है और बुवाई के दौरान सीधे बीज के साथ-साथ शीर्ष-ड्रेसिंग के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इस पद्धति के साथ, श्री बेसरोटी ने केंचुओं की एक विशाल संख्या के विकास पर ध्यान दिया, जिसने जैविक खेती को आशा की एक नई किरण प्रदान की। तीन दिनों के लिए, 20 लीटर ठोस जीवामृत में 2.5 लीटर पानी डाला गया। उन्होंने ऊष्मायन के तहत 45 दिनों के बाद ट्रे में लगभग 1,000 केंचुए पाए। वर्मी-कम्पोस्ट की तैयारी के 71 दिनों के बाद, उन्होंने केंचुआ कॉलोनियों, प्यूपा और छोटे कृमियों की एक बड़ी संख्या को पाया और ट्रे में 1,500 अच्छी तरह से विकसित और विकसित केंचुओं को देखा। उन्हें प्रत्येक ट्रे से 20 किलोग्राम वर्मी-कम्पोस्ट मिलता है, जिसे खाद और ठोस जीवनमूथा के साथ मिलाया जाता है और फसलों के लिए उपयोग किया जाता है। ठोस जीवनमूर्ति और वर्मी-कम्पोस्ट तैयार करने की इस नई विधि की मदद से, श्री बिस्सरोटी हर साल 10 मीट्रिक टन वर्मी-खाद और 5 मीट्रिक टन ठोस जीवनमूर्ति का उत्पादन करते हैं। इन जैविक उत्पादों के साथ, वह स्थायी फसलों का उत्पादन करने में सक्षम है जो अकार्बनिक खेती प्रथाओं के माध्यम से उत्पादित लोगों की तुलना में स्वाभाविक रूप से बेहतर हैं। हर दिन, वह प्रति ट्रे में न्यूनतम 15 किलोग्राम ठोस जीवनमूर्ति तैयार करता है, जो एक वर्ष में अधिक से अधिक 5,475 किलोग्राम ठोस जीवामृत की मात्रा है। वह 17 नीम के पेड़ों से एकत्र किए गए बीजों के साथ 200 किलोग्राम नीम केक भी तैयार करता है और वर्मी-खाद उत्पादन के लिए नीम के पत्तों का उपयोग करता है। उन्होंने कम्पोस्ट, वर्मी-कम्पोस्ट और स्थानीय बीज सामग्री के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर टिकाऊ कृषि की खोज की। जैविक खेती के इस तरीके को अपनाने से, वह वर्षा की स्थिति के तहत प्रति एकड़ भूमि में बेहतर फसल उत्पादकता हासिल करने में सक्षम हो गया है। इसके अलावा, अंतिम उपज का पाक मूल्य और शेल्फ जीवन अच्छा है और भंडारण पर इसकी मूल पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। श्री बिरसोट्टी का मानना है कि यदि अन्य किसान इन सभी वर्षों में जैविक खेती पद्धति का पालन करते हैं, तो इससे उन्हें टिकाऊ कृषि को बनाए रखने और अनिश्चित और अप्रत्याशित वर्षा से प्रभावित परिस्थितियों में कृषि कार्यों से पारिश्रमिक आय प्राप्त करने में बहुत लाभ होगा।
टिकाऊ खेती के लिए प्राकृतिक संसाधन समृद्ध करना।
टिकाऊ खेती के लिए प्राकृतिक संसाधन समृद्ध करना। श्री प्रसाद (50), भारत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सगीपाडु पोस्ट एंड विलेज, रथनागिरिनगर के कोटा मंडल के हैं। उनके पास बोरवेल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी के साथ 25 एकड़ तक की भूमि है। उनके पिता एक कृषि अधिकारी थे, जो बचपन से ही कृषि और संबद्ध उद्यमों में रुचि रखते थे, हालांकि वे पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और कुछ वर्षों के लिए एक निजी कंपनी के साथ बॉयलर इंजीनियर के रूप में काम किया है। खेती शुरू करने के लिए एक इंजीनियर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ने का उनका कारण यह है कि वह किसी पर भी निर्भरता के बिना एक किसान के रूप में जीना चाहते थे। वह श्री के पास गया। खेती की पालेकर प्रणाली, प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा और खुद की खेती प्रणाली शुरू करने से पहले कुछ खेतों का दौरा किया। वह केले के साथ नारियल (कर्पूरम किस्म) की खेती 12.5 एकड़ में 8x8 मीटर रिक्ति के साथ करते हैं, चार एकड़ में अंतर फसल के रूप में कोको, दो एकड़ में केला और दो एकड़ में चारा और सब्जी के साथ नारियल की खेती करते हैं। उन्होंने बड़ी मोटरों के बजाय पावर टिलर और छोटे उपकरण खरीदे। उनका खेत गाँव से सटा हुआ है और प्रचुर मात्रा में श्रम उपलब्ध है। कम समय में उनकी उपलब्धियों के कारण, उनका खेत कई आगंतुकों को आकर्षित करता है। वह नेशनल एसोसिएशन ऑफ पाम ऑरचर्ड्स के अध्यक्ष और काउ-बेस्ड एग्री के सदस्य हैं। सोसायटी, वर्ष 2011 के दौरान 120 किसानों के साथ सदस्यों के रूप में शुरू हुई। 2007 के बाद से, उन्होंने धीरे-धीरे बाहरी आदानों को कम करना शुरू कर दिया और जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित किया। 2011 में, उन्होंने गाय आधारित खेती की शुरुआत की। जब उन्होंने कृषि क्षेत्र में कदम रखा, तो उन्होंने देखा कि पानी की कमी और खराब मिट्टी की स्थिति, लाभहीन कृषि के मुख्य कारण थे। उन्होंने पालेकर सिद्धांतों पर आधारित खेती शुरू की। पालेकर प्रणाली के कुछ सिद्धांत शून्य बजट खेती हैं - बाहरी आदानों पर खर्च किए बिना, प्राकृतिक निवेश जैसे कि गोबर, मूत्र आदि से तैयार किए गए जीवामृत, कई फसलें उगाना। उसने खेत में ढलान के खिलाफ दो फीट चौड़ाई और 2-6 फीट लंबाई की खाइयों को खोदकर पाथ-वे बनाये और उन्हें जल संरक्षण संरचनाओं के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उनमें जंगली घास और गोबर भर गया। उन्होंने पूरे खेत में पौधों के बीच लगभग नौ इंच गहराई के साथ उथले गड्ढों को भी खोदा और बारिश के पानी को निकालने के लिए नारियल के गोले के साथ गड्ढों को भर दिया। उन्होंने मिट्टी को समृद्ध करने के लिए ताड़, नारियल और कोको का पत्ता बाग में गिरता है इसके विघटन की भी व्यवस्था की । इन उपायों के माध्यम से, वह अपने खेत में अधिशेष वर्षा जल की प्राप्ति करने और विघटित खेत कचरे को शामिल करके मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में सक्षम था। उन्होंने लगभग रु. 30,000 प्रतिवर्ष की ओर। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तो अधिक लोग इन उपायों को अपना सकते हैं। श्री प्रसाद ने सूक्ष्म सिंचाई, खाइयों को बारिश के पानी की प्राप्ति , कार्बनिक कार्बन के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य के निर्माण, मौजूदा पंपिंग प्रणाली को बढ़ावा देने और पौधों के बीच सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और उथले गड्ढों में दबाव बनाने के लिए दो एचपी की मोटर स्थापित करने के लिए अनुकूलित किया है। वाष्पीकरण के नुकसान को कम करने के लिए संयंत्र अपशिष्ट के साथ कवर किया गया। वह विशेष रूप से फसलों को सिंचाई के लिए न्यूनतम पानी का उपयोग करने के बारे में है और 1995 के बाद से बढ़ रही सभी फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई प्रणाली की स्थापना की है। जी से सड़न के लिए पौधों के चारों ओर मिट्टी की सतह पर, पौधों को सिंचाई प्रदान करने के अलावा उन्होंने पत्ती कूड़े पर पानी छिड़कने के लिए बाग में ड्रिप के बजाय एक जेट लगाया । उन्होंने कोको और केले को जमीन, पानी और श्रम से लाभ को अधिकतम करने के लिए ताड़ और नारियल के बागानों में अंतर-फसलों के रूप में उगाया है। इससे उन्हें तब भी बेहतर कमाई करने में मदद मिली, जब तक कि कोको की अंतर-फसल से उन्हें आय प्राप्त नहीं हुई, ताड़ के तेल की कीमतें कम हो गईं। उन्होंने कई रणनीतियों को अनुकूलित किया है, जैसे गायों को पालने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को समृद्ध करने और गाय और पौधों पर आधारित उत्पादों का उपयोग करके कीटों और बीमारियों का प्रबंधन करने के लिए। उनकी प्रथाओं ने न केवल उत्पादन की लागत को कम किया है, बल्कि मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य के कारण गुणवत्ता के उत्पादन का भी एहसास हुआ है। वह लगभग 25 एकड़ ऊंचे खेत के माध्यम से सालाना रु.18 लाख कमाता है। वह अपनी आय का 30% श्रम मजदूरी, मशीनरी के रखरखाव पर 15%, घरेलू खर्च पर 30% और संपत्ति खरीदने और खेत पर पुनर्निवेश पर 25% खर्च करता है। उनकी भविष्य की योजनाएं हैं कि वे अपने खेत को जैविक प्रमाणित करें, विजयवाड़ा में जैविक उत्पाद बेचने के लिए एक रिटेल आउटलेट खोलें और सब्जियों के जैविक उत्पादन के लिए किसान समूहों को संगठित करें।