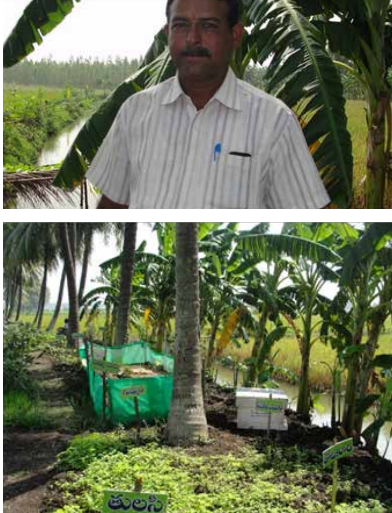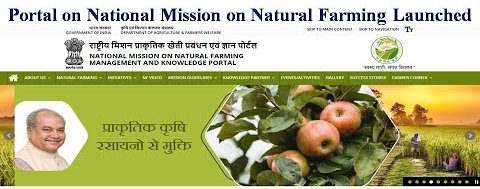मत्स्य पालन में अग्रणी मार्ग: कैलाश फिशरीश एंड एक़्वेटिक। श्री अक्षय कुमार साहू ओडिशा के बालासोर में अस्सापुरा गाँव, बिसिंगा मंडल, मयूरभंज जिले के 41 वर्षीय प्रगतिशील किसान / उद्यमी हैं। उनके पिता, श्री मानरंजन साहू ने 1.5 एकड़ भूमि में मछली पालन शुरू किया, और पारंपरिक तरीके से भारतीय प्रमुख कार्प्स (कैटला, रोहू और मिरगल) की खेती की, लेकिन उत्पादन ज्यादा नहीं था। बाद में, उन्होंने और उनके छोटे भाई, श्री संजय साहू ने, ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर (CIFA) के वैज्ञानिकों की मदद से खेती करने का एक तकनीकी तरीका शुरू किया। श्री अक्षय कुमार साहू ने मीठे पानी की मछली के प्रजनन और संस्कृति प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने के लिए कई प्रशिक्षणों को पूरा किया। उन्होंने अपने स्वयं के हैचरी में भारतीय प्रमुख कार्प और अन्य प्रजातियों की स्वदेशी प्रजातियों का प्रजनन शुरू किया। उन्होंने धीरे-धीरे अपने संस्कृति क्षेत्र को बालासोर में चार अलग-अलग स्थानों में 100 एकड़ तक बढ़ाया और अपनी खुद की मछली हैचरी शुरू की, जिसमें मीठे पानी की मछली की 25 किस्में हैं, जिनमें मीठे पानी की झींगा और स्कैम्पी शामिल हैं। ओडिशा में प्रजनन, पालन और संवर्धन के मामले में कैलाश फिश हैचरी सबसे बड़ी है। श्री अक्षय न्यूनतम मूल्य पर ट्रेन या वायु द्वारा ऑक्सीजन युक्त पैकिंग के साथ देश के सभी हिस्सों में मछली की सालगिरह और उंगलियों की आपूर्ति भी करते हैं। उनके खेत को भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित ICARCIFA, भुवनेश्वर, ओडिशा के तहत किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक एक्वाकल्चर फील्ड स्कूल माना जाता है। इसमें एक प्रशिक्षण हॉल, एक ऑडियो विजुअल रूम, आवास, एक प्रदर्शन खेत क्षेत्र और एक हैचरी जैसी सुविधाएं हैं। कई किसान प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं। श्री साहू किसान आवश्यकताओं के आधार पर बीज की आपूर्ति करते हैं। उन्होंने राज्य के मत्स्य विभाग, राज्य सरकार की सहायता से अपने और पड़ोसी जिलों की किसानों की आवश्यकताओं के आधार पर अपने खेत पर अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त कैलाश फ्लोटिंग फिश फीड मिल संयंत्र की स्थापना की। ओडिशा का, और सहायक राज्य योजना से वित्तीय सहायता। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB), हैदराबाद; पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भी गिस्क तिलपिया, एशियाई समुद्री बास और पंगेसियस जैसी मांग पर वाणिज्यिक प्रजातियां उगाने के लिए रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। श्री साहू ने मछली के बीज, चारा और प्रशिक्षण आदि की पैकिंग और परिवहन के साथ ही एक उत्कृष्ट कृषि सुविधा, हैचरी, फीड मिल, रियरिंग टैंक विकसित किए हैं। श्री साहू के उद्यम की सफलता को देखते हुए, मत्स्य पालन विभाग, सरकार ओडिशा ने 2011 में सफल प्रेरित प्रजनन के लिए अपने खेत को ओडिशा प्राइवेट हैचरी के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। ICAR-CIFA, भुवनेश्वर, ने अपने उद्यम "कैलाश फिशरीज एंड एक्वेटिक्स" को अपने एक्वाकल्चर फील्ड स्कूल के माध्यम से इनक्यूबेट्स में से एक के रूप में मान्यता दी। 5-7 जनवरी, 2018 से आयोजित "कृषि और जलीय कृषि हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों की आय में सुधार" पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान, कृषि विज्ञान केंद्र ने उन्हें ओडिशा में "सर्वश्रेष्ठ किसान" का नाम दिया और उन्हें "अभिनव किसान पुरस्कार" से सम्मानित किया। 7 जून, 2018 को ICAR-CIFA में अभिनव किसानों की बैठक राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB), पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने उन्हें 2016, 2017 और 2018 में विश्व मत्स्य दिवस समारोह के दौरान "सर्वश्रेष्ठ उद्यमी" पुरस्कार से सम्मानित किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट (MANAGE) ने कैलाश फिशरीज एंड एक्वेटिक्स को भविष्य में मत्स्य क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर गतिविधियों के हिस्से के रूप में फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए फील्ड केंद्रों में से एक के रूप में मान्यता दी है। श्री साहू ने नियमित गतिविधियों के लिए लगभग 100 स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। कैलाश फिशरीज 250 करोड़ स्पॉन, 100 लाख फ्राई और 60 टन फिंगरिंग का उत्पादन करती है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपये है। वह मत्स्य पालन विभाग, ओडिशा सरकार, ICAR-CIFA, NFDB और कौशल विकास मंत्रालय के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है और सीखने और नवाचार के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करता है।
Farmer Success Stories
फलों की पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज और मार्केटिंग के माध्यम से सफलता।
फलों की पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज और मार्केटिंग के माध्यम से सफलता। श्री वेंकट नरसिम्हा राजू आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के केसवारम गाँव से हैं। वह एक कृषि परिवार से आता है, जिसमें 14 एकड़ मछली तालाब और 9 एकड़ वेटलैंड है। उन्होंने फसलों, पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ एक एकीकृत कृषि प्रणाली चलाई और मत्स्य उद्योग की ओर अधिक झुकाव हुआ। उसने मछली तालाबों से एक महान खिंचाव महसूस किया। इसने उन्हें अभिनव विचारों और निरंतर प्रयोग के साथ आने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें मत्स्य पालन में मान्यता और कई सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार मिले। वह भारतीय कैटफ़िश प्रजनन और हैचरी शुरू करने वाले अपने जिले के पहले व्यक्ति हैं। वह केंद्रीय संस्थानों जैसे सेलुलर और आणविक जीवविज्ञान (CCMB), हैदराबाद के केंद्रीय संस्थानों की अनुसंधान गतिविधियों में शामिल थे; केंद्रीय मीठे पानी एक्वाकल्चर (CIFA), भुवनेश्वर; केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (CIFE), बालाबाडपुरम, पूर्वी गोदावरी, A.P .; कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस (मुत्तुकुर, नेल्लोर, ए.पी.) और केवीके (उडी, पश्चिम गोदावरी, ए.पी.)। वह अनुसंधान केंद्रों को मछली की लुप्तप्राय प्रजातियों की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बन गया। हालांकि, श्री राजू के सपने तब कुचले गए जब सरकार ऑपरेशन कोल्लेरू, 2006 के साथ सामने आई। इसने न केवल पिछले 60 वर्षों में परिवार के स्वामित्व वाले मछली तालाबों को नष्ट किया, बल्कि श्री राजू के उद्यमी कौशल को भी प्रभावित किया, जिसने कई व्यक्तियों और संगठनों का समर्थन किया। । रातोंरात, एक नियोक्ता जिसने कई लोगों को रोजगार प्रदान किया वह खुद बेरोजगार हो गया। यद्यपि वह व्यथित था, उसने खुद को सांत्वना दी और विकास के अन्य क्षेत्रों में अपने कैलिबर को साबित करने के लिए नए सिरे से अपने काम की दिशा बदल दी। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को एक संगठित क्षेत्र से संगठित एक में बदलना चाहते थे। इस विचार के साथ, उन्होंने एक कंपनी के संचालन के तौर-तरीकों और भविष्य के विकास के लिए इतिहास बनाने में इसके निहितार्थों का पता लगाया। इस विचार प्रक्रिया ने कृषि आधारित उद्योग शुरू करने के उनके संकल्प को मजबूत किया। श्री राजू ने अप्रैल 2012 में "कोल्ड स्पेस एग्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" नामक एक फर्म शुरू करने के लिए तीन अन्य समान उद्यमियों के साथ हाथ मिलाया। यह उद्यम प्री-कूलिंग और स्टोरेज के साथ फलों और सब्जियों के लिए पोस्ट-फसल प्रबंधन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो एथिलीन-आधारित है। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दबाव वाले पकने वाले चैंबर। इस उद्यम के मुख्य उद्देश्य किसानों को "अच्छी कृषि पद्धतियों" (जीएपी) में मदद और शिक्षित करना है; सरकारी संगठनों, अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और व्यक्तिगत किसानों के साथ काम करते हैं और निजी क्षेत्र या सरकार द्वारा आयोजित "आम-मेला" में भाग लेते हैं। श्री राजू और उनकी टीम के सदस्यों ने अपने पेशेवर कृषि पृष्ठभूमि के माध्यम से और क्षेत्र से संबंधित वेबसाइटों के लिए इंटरनेट ब्राउज़ करके और व्यक्तिगत प्रयोगों के माध्यम से पकने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने का बीड़ा उठाया। टीम ने आम, केला, सपोटा, मुसम्बी, पपीता जैसे फलों में पकने की प्रक्रिया का मानकीकरण किया, साथ ही पकने के लिए पूर्व शर्त, जैसे कि समय, कटाई और परिवहन के लिए बेहतर परिणाम। उन्होंने समान पकने और फल की गुणवत्ता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखा। श्री राजू और उनकी टीम की पहल ने गाँव में रोजगार के कई अवसर पैदा किए हैं। पिछले 4 वर्षों में 15 व्यक्तियों के लिए नियमित रोजगार प्रदान किया गया है, जिसमें पारिश्रमिक प्रति माह 9,000-12,000 / - रुपये है। इस इकाई के माध्यम से उत्पन्न रोजगार पिछले चार वर्षों से लगातार 190 से 353 दिनों तक बढ़ा है। आम के मौसम (मार्च-जून) के दौरान, अतिरिक्त श्रम और लदान के लिए लगे हुए हैं, और प्रत्येक टोकरे के लिए 2.25 / - रुपये का भुगतान किया जाता है और एक मजदूर औसतन रुपये 600-700 / - प्रति दिन कमाता है। इसने कॉलेज जाने वाले छात्रों को अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इस नौकरी को लेने और अपने गांव से आवश्यक शुल्क अर्जित करने के लिए आकर्षित किया है। आज शीत अंतरिक्ष पांच राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र से फल लाने वाले 170 किसानों और फल विक्रेताओं को सेवाएं प्रदान कर रहा है। न्यूनतम अवशेष स्तर के साथ आम के उत्पादन के लिए किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों में शिक्षित करना; सदस्य किसानों को नई तकनीकों और मशीनरी पर बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए फर्म एफपीओ, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, विस्तार अधिकारियों, सुपरमार्केट के साथ नेटवर्किंग कर रहा है। श्री राजू और उनकी टीम अन्य गतिविधियों में शामिल हैं, एक ही परिसर में एक रसोई उद्यान का प्रचार, अधिकारियों की क्षमता निर्माण, खरीदार और विक्रेता की व्यवस्था और कार्बाइड मुक्त आम उत्पादन पर किसानों और व्यापारियों का उन्मुखीकरण। श्री राजू, एक सक्रिय और जानकार किसान, कृषि क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों का विस्तार करने में एक रोल मॉडल साबित हुआ है और कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्हें नई मछली प्रौद्योगिकियों को अपनाने और समुदाय के लिए नेतृत्व पर सराहना पत्र मिला, सफल मछली पालन के लिए मत्स्य पालन में योग्यता का प्रमाण पत्र और एपी में मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने में उनका योगदान और कृष्णा जिले में आयोजित मत्स्य प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार । उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भारतीय मत्स्य मंच में भी भाग लिया है। “कोल्ड स्पेस एग्रो-टेक इंडिया प्रा लि. ”ने अभी-अभी निर्यात सेवा शुरू की है और अगले दो वर्षों में गर्म पानी के उपचार और ऑटो-ग्रेडिंग सुविधाओं को स्वचालित करके संयंत्र के विस्तार पर विचार कर रहा है। टीम ने किसानों और विक्रेताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और प्राकृतिक खेती (रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मुक्त) में आम, अनार, पपीता आदि जैसे फलों का उत्पादन करने के लिए कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई है।
सशक्त महिलाएं एक सफल डेयरी उद्यम चलाती हैं।
सशक्त महिलाएं एक सफल डेयरी उद्यम चलाती हैं। विनम्र पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिलाओं का एक समूह करनाल के पास अमृतपुर कलां नामक गांव में एक साथ आया है और "अनमोल महिला अधिकार समिति" का गठन किया है, जिसने उन्हें सशक्त बनाया है और उन्हें अन्य महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनाया है। अर्पणा ट्रस्ट, जिसने महिलाओं को जुटाने के लिए पहल की है, महिलाओं को कुछ उद्यमशीलता गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। समूह के सदस्यों ने महसूस किया कि दो कारणों से दूध आधारित उद्यम शुरू करने की गुंजाइश है: (i) उनके गाँव में पर्याप्त दुग्ध उत्पादन और (ii) दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिलना। उन्होंने किसानों से 20 लीटर दूध इकट्ठा करना शुरू किया और 500 लीटर / दिन तक चला गया। उन्होंने रु.20 / लीटर की दर से दूध खरीदना शुरू कर दिया , जब स्थानीय बाजार में कीमत केवल रु.12 / लीटर था । करनाल के निवासियों को वे गाय के दूध को रु. २० / लीटर में खरीदते हैं और बेचने के लिए रु.28 / लीटर और रुपये के लिए भैंस के दूध की खरीद रु. 35 / - प्रति लीटर और रु. 45 / - प्रति लीटर में बेचते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनडीआरआई), करनाल, ने आगे आकर गाँव की चुनिंदा महिलाओं के लिए मूल्य वर्धित डेयरी उत्पादों पर तीन महीने का प्रशिक्षण शुरू किया। व्यवसाय की क्षमता को महसूस करते हुए, महिलाओं के समूह ने शुरुआत में अनमोल महिला दुग्ध समिति के नाम से एक दूध संग्रह केंद्र शुरू किया। हार्पाना ट्रस्ट ने उन्हें 1.5 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया। समूह ने अपने उद्यम से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को खरीदा, जैसे कि वजन मशीन, वसा विभाजक, फ्रिज, सिलेंडर, बर्तन और दूध के डिब्बे। एनडीआरआई द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण और उसके बाद उनके द्वारा प्राप्त विश्वास के आधार पर, अनमोल महिला समिति ने एनडीआरआई के तकनीकी समर्थन के साथ खोआ, पनीर, दही, मक्खन, घी आदि जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों को तैयार करना शुरू कर दिया है। तैयार किए जाने वाले मूल्य वर्धित उत्पादों की मात्रा मांग और प्राप्त आदेशों के आधार पर तय की जाती है। सदस्य अपने उत्पादों के विपणन के लिए एनडीआरआई छात्रावास, विवाह पक्ष, होटल / ढाबे और प्रसिद्ध स्वीट स्टॉल जैसे संस्थानों से संपर्क करते हैं। दिवाली जैसे त्यौहार के मौसम, उनके द्वारा निर्मित दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किए जाते हैं। उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता के कारण बाजार में उनके उत्पादों की निरंतर मांग है। संतोष व्यक्त करते हुए, अनमोल महिला दुद्धी समिति की सचिव श्रीमती सविता कहती हैं कि प्रत्येक सदस्य प्रति माह अपने काम से रु. 5,000-6,000 / - मासिक आय अर्जित करता है। जो वे अपने परिवार और घरेलू काम की देखभाल करने के अलावा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी सदस्य एक परिवार के रूप में काम करते हैं और काम को वितरित करते हैं, जैसे दूध संग्रह, ऑर्डर लेना, पुस्तक रखरखाव, मूल्य संवर्धन आदि। तीन महिलाएं सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक और अन्य तीन दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक काम करती हैं। शेष सदस्य, समूह की नेता सुश्री कमलेश, पास के शहर करनाल में मूल्य वर्धित डेयरी उत्पादों को बेचने के लिए दूध प्राप्त करने से लेकर विपणन की सभी गतिविधियों को संभालती हैं। समूह के सदस्यों ने याद दिलाया कि शुरुआती दिनों के दौरान, उद्यम शुरू करने में उनके पास परिवार के सदस्यों और गांव के समर्थन की कमी थी। हालांकि, अपने मजबूत दृढ़ संकल्प के कारण, वे मूल्य वर्धित डेयरी उद्यम में सभी बाधाओं के खिलाफ सफल रहे। शुरुआती दिनों में उन्हें जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने उन्हें आगे की प्रगति के लिए पर्याप्त सबक दिया। अब, वे सफल, लाभ कमाने और आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ-साथ सामाजिक रूप से भी महसूस करते हैं। समूह ने महसूस किया कि एनडीआरआई प्रशिक्षण ने उन्हें इस उद्यम को एक सफल उद्यम बनाने में लाभान्वित किया। इसने उन्हें सशक्त बनाने में मदद की, आस-पास के गांवों में अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गईं और महिलाओं के बारे में सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ दिया। समूह के सदस्यों ने कहा कि उनकी बचत में वृद्धि हुई है, उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार हुआ है और वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं। समूह भी उच्च रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग शुरू करने की योजना बना रहा है।
जहां चाह, वहां राह।
जहां चाह, वहां राह। कई किसान आजकल बेहतर जीवनयापन की तलाश में खेती छोड़ रहे हैं और शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, नासा सलंगरी गाँव, ऊना जिला, हिमाचल प्रदेश के एक किसान श्री यूसुफ खान ने मशरूम की खेती शुरू करने के लिए अपनी पेशेवर विशेषज्ञता का उपयोग किया। बचपन से ही उन्हें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का शौक था। एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला लेने के बाद, उनकी रूचि गहरी हुई और उन्होंने वर्ष 2000 में नांगल सलांगरी, ऊना में अपनी मशरूम की खेती की इकाई स्थापित की। इस उद्यम में सफलता के साथ, उन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जो हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश में मशरूम की खेती को बढ़ावा और लोकप्रिय बना रहा है। इसके साथ ही उन्होंने संरक्षित सब्जी की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती और एरोपोनिक्स (टमाटर, ककड़ी) आदि की शुरुआत की। केंद्र मशरूम परियोजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान करता है। अब तक, उन्होंने बहरीन के कुछ किसानों को प्रशिक्षित करने के अलावा, देश भर में 1,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया है। उनकी इकाइयों का कारोबार लगभग रु.70-80 लाख / वर्ष है। इकाई में एक अच्छी तरह से सुसज्जित स्पॉन लैब, खाद इकाई, बढ़ती इकाई और प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। वह स्पॉन लैब में दूधिया और बटन मशरूम की खेती करता है, जिसमें 1.36 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। इस उद्देश्य के लिए प्रति माह खाद के लगभग 20,000 बैग तैयार किए जाते हैं। बटन मशरूम का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। नाइट्रोजन और जिप्सम के स्रोत के रूप में पोल्ट्री खाद और पूरक (सूरजमुखी केक और कपास के बीज) के साथ गेहूं का भूसा, कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। 1 किलो गेहूं के भूसे को बनाने में 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और इसे 75-800 सेल्सियस के आवश्यक तापमान पर गेहूं के भूसे के बाहरी चरण के लिए न्यूनतम 12 दिनों तक छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। 12 दिनों के बाद, इसे खाद तापमान पर स्थानांतरित किया जाता है और फिर एक पेस्टिसिएशन चैम्बर में ले जाया जाता है। ५C-६००C पर से १० घंटे के लिए पेस्टिसिकेशन किया जाता है; इस अवधि में, सभी नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दिया जाता है, जो मशरूम के लिए पोषक माध्यम के रूप में कार्य करता है। एक बार खाद तैयार हो जाने के बाद, तापमान की आवश्यकता 220C हो जाती है। 10 किलो खाद के लिए, स्पान की आवश्यक मात्रा 50-80 ग्राम होती है। उसके बाद, एक बंद कमरे में 220C तापमान बनाए रखा जाता है। 15 दिनों के भीतर, स्पॉ को खाद बैग में ले जाया जाता है। श्री खान संरक्षित खेती के तहत खेत में टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, धनिया, सलाद और स्ट्रॉबेरी भी उगाते हैं। खेत पर दो पॉलीहाउस हैं, 1,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं जिसमें ककड़ी और टमाटर जैसी सब्जियां उगाई जाती हैं। उन्होंने मीडिया में एक बीज रहित ककड़ी नर्सरी विकसित की है, और फिर इसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में स्थानांतरित कर दिया गया है। श्री खान को वर्ष 2006 में दिव्य हिमाचल से "प्रगतिशील किसान" पुरस्कार और 2010 में CSKHP पालमपुर विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश से "कृषि उदयमी पुरस्कार" (कृषि उद्यमी पुरस्कार) मिला। अखिल भारतीय मशरूम एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने "उत्कृष्ट मशरूम उत्पादक" पुरस्कार भी प्राप्त किया। । उनके अनुसार, "दरवाजे पर संसाधनों का उपयोग सफलता की कुंजी है"। उनका सुझाव है कि बेरोजगार कृषि स्नातक कृषि उद्यम लेते हैं क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
समग्र खेती से आय में वृद्धि।
समग्र खेती से आय में वृद्धि। श्री अंगाराजू सत्यनारायणाराजू (47), कुमुदावल्ली गांव, पालकोदरु मंडल, पश्चिम गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश, भारत से हैं। उनके पास 10 एकड़ जमीन है, और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। वह एक ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी का भी मालिक है और उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती के नवीन और लाभदायक तरीकों की तलाश में रहता है। यह ज्ञात है कि धान की खेती खेत में की जाती है और मछली तालाबों में। हालांकि, श्री सत्यनारायणाराजू एक एकड़ भूमि में सब्जियों के साथ धान और मछली भी उगाते हैं। उन्होंने कृषि और प्रबंधन विभाग (एडीए) के सहायक निदेशक श्री ए. श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा पश्चिम गोदावरी में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के मार्गदर्शन में समग्र कृषि शुरू करने से पहले एक प्रदर्शन में भाग लिया। एडीए ने कुछ साल पहले केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक, ओडिशा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर इस अवधारणा को बढ़ावा दिया। कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के तकनीकी मार्गदर्शन और अभिनव गतिविधियों की श्रेणी में ATMA के वित्तीय समर्थन के तहत समग्र खेती पर प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया गया था। श्री सत्यनारायणाराजू ने दो क्विंटल वर्मी-कम्पोस्ट और न्यूनतम मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया, अर्थात् एसएसपी (सिंगल कंपोज़िट फ़ार्मिंग इनोवेटिव फ़ार्मर्स सुपर फ़ॉस्फ़ेट से 46 प्रेरक कहानियाँ), पोटाश (10 किग्रा) और यूरिया (15 किग्रा), पोखर का समय। उन्होंने MTU 1010, PLA 1100 धान बीज और 300 ग्राम नीम तेल स्प्रे तीन बार इस्तेमाल किया। मछली की किस्मों के बीच, केवीके वैज्ञानिकों द्वारा सलाह के अनुसार, उसने 50-100 ग्राम वजन वाली शीलावती (800), बोचा (200) और मोसा (100) उंगलियों का इस्तेमाल किया। चावल के प्रत्यारोपण के 20 दिन बाद इन्हें खाइयों में छोड़ दिया गया। उन्होंने हर वैकल्पिक दिन में पांच किलो चावल की भूसी (एक वर्ष में 1,000 किग्रा), 200 किग्रा मवेशी खाद और कम मात्रा में अजोला का उपयोग मछली के भोजन के लिए किया। मछली के लिए फ़ीड के रूप में सेवा करने के अलावा, अजोला धान के खेत में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करने और आपूर्ति करने में भी मदद करता है। यह देखा गया कि धान के खेतों में स्वतंत्र रूप से चलती मछली ने लार्वा और अंडे खाने से स्वाभाविक रूप से कीट नियंत्रण किया। श्री सत्यनारायणाराजू ने 20 गुंटे पर एक वर्ष में 820 किलोग्राम मछलीka उत्पादन लिया , और उन्हें भीमवारम बाजार में बेचा गया। उन्होंने मध्यम और लंबी अवधि में अपनी आय के पूरक के लिए केले, पपीता, मिर्च, टमाटर, लौकी, नारियल के पेड़, ड्रमस्टिक, पेड़ पौधों आदि को भी बंडलों पर लगाया। उन्होंने पूरक आय प्राप्त करने और परागण में मदद करने के लिए खेत स्तर पर खाद तैयार करने के लिए एक वर्मी-संस्कृति इकाई और शहद मधुमक्खी बॉक्स की शुरुआत की। उन्होंने स्थानीय सामग्री का उपयोग करके मछली की खाई के ऊपर पक्षियों के लिए एक छोटे से घोंसले का निर्माण करके अपने खेत में विभिन्न प्रकार के पोल्ट्री पक्षियों को भी जोड़ा है। पहले साल में, श्री सत्यनारायणाराजू ने एक एकड़ भूखंड से 1.19 लाख रु का शुद्ध लाभ अर्जित किया। । प्रत्येक मौसम में औसतन 16 क्विंटल धान की कटाई की जाती है, जो कि छोटे परिवार के लिए वर्ष के लिए पर्याप्त है। अकेले मछली की खेती उसके लिए उच्च शुद्ध आय का स्रोत रही है। श्री सत्यनारायणाराजू का CB अनुपात 1: 2.60 था। वह अपने खेत में जानवरों की कुछ और किस्मों को पेश करने की योजना बना रहा है और मुर्गी, बकरियों और भेड़ों के लिए एक स्थायी संरचना बनाने के लिए खेत के एक तरफ तीन मीटर की खाई का निर्माण किया है। वह पेड़ की छांव के नीचे हल्दी और अदरक की खेती करने की योजना बना रहा है। अपने ज्ञान और अनुभव के साथ, वह समग्र खेती पर अन्य किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।
कर्नाटक के पुरस्कार विजेता बागवानी किसान।
कर्नाटक के पुरस्कार विजेता बागवानी किसान। श्री एच। मुरलीधारा (42) होसहुद्या गाँव, देवनहल्ली तालुक, बेंगलुरु ग्रामीण जिले, कर्नाटक से आते हैं। उसके पास कुल 10 एकड़ जमीन है, जिसमें से 8 एकड़ सिंचाई के अधीन है और बाकी 2 एकड़ वर्षा आधारित खेती के तहत है। वह एक कृषि परिवार से है। एक कृषक के रूप में, पहले, वह अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए अनाब-ए-शाही अंगूर की खेतों की फसलें, सब्जियाँ और पुरानी किस्में उगाते थे, लेकिन वे अपनी आय से संतुष्ट नहीं थे। बाद में, उन्होंने कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों से सलाह लेने के बाद उन्नत बागवानी फसलों की खेती की ओर रुख किया, जैसे कि विदेशी अंगूर और अनार की किस्में। 2012-13 में, श्री मुरलीधर ने पेंडल प्रणाली का उपयोग करके अंगूर की विदेशी किस्मों जैसे कि शरद सीडलेस (70 गंटा), रेड ग्लोब (20 गंटा) और सोनका (10 गुंटा) 2.5 एकड़ भूमि पर और बैंगलोर ब्लू 1 एकड़ पर के साथ नए अंगूर रूटस्टॉक, डॉग्रीज़ की जगह ली। उन्होंने विभिन्न किस्मों के लिए वैज्ञानिक रिक्ति भी अपनाई। दूसरे वर्ष से, उन्होंने अंगूर की अच्छी गुणवत्ता वाले गुच्छों का उत्पादन शुरू कर दिया, लेकिन वे अपनी पारिश्रमिक आय को महसूस करने में विफल रहे क्योंकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बाजार की कीमतें कम थीं। बाद के वर्षों में भी, उन्होंने उन्नत उत्पादन प्रथाओं को अपनाने के बाद अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूर का उत्पादन किया, लेकिन बाजार की कम कीमतों के कारण असफल रहे। अपने कटु अनुभवों के बाद, उन्होंने डॉ. जयराम, प्रोफेसर और प्रमुख, कृषि, विपणन और सहयोग विभाग, जीकेवीके, यूएएस, बेंगलुरू से संपर्क किया, ताकि किफायती कीमतों पर अंगूर के विपणन के लिए मदद ली जा सके। उनके सुझावों के आधार पर, श्री मुरलीधर ने अगले कुछ वर्षों में गुणवत्ता वाले फलों की कटाई की और उन्हें "नंदी अंगूर" के अपने ब्रांड नाम के तहत पैक किया, जिसे डॉ. जयराम ने सुझाव दिया था कि उनका खेत नंदी हिल्स के आसपास के क्षेत्र में है। उन्होंने शुरुआत में GKVK मुख्य परिसर के बैनर तले मार्केटिंग की यूएएस, बेंगलुरू, जिसका शीर्षक है “रियायती दरदल्ली रायथरिंडा ग्रहाकारगे इस नए विपणन प्रणाली के तहत नीरा मराटा ”। पहले दिन, उसकी पूरी उपज बेंगलुरु रिटेल मार्केट की कीमत से 30 रुपये कम में गर्म केक की तरह बेची गई। । कम कीमत के बावजूद, उन्होंने के लिए शरद अंगूर 70 रुपये प्रति किलो और रेड ग्लोब रु. 80 प्रति किलो बेचने के बाद अच्छा लाभ कमाया। हालाँकि, HOPCOMS और अन्य मार्केटिंग मौटे इन किस्मों को क्रमशः रुपये 120 प्रति किलो और रु. 200 में बेच रहे थे। वर्ष 2017 में उन्होंने 40 टन का उत्पादन किया और 2018 में उन्होंने अपनी कुल 3.5 एकड़ भूमि से बैंगलोर ब्लू अंगूर और अंगूर की अन्य विदेशी किस्मों सहित 45 टन अंगूर का उत्पादन किया। 2017 में पूरे अंगूर के बाग के लिए रु .6 से रु .7 लाख तक वार्षिक खर्च के साथ खेत में विपणन के अलावा, उन्होंने प्रत्यक्ष विपणन से रु.22 लाख कमाया । इसी तरह, वर्ष 2018 में, उन्होंने रु. 26 लाख कमाया ।अंगूर के प्रत्यक्ष विपणन के बाद वैज्ञानिकों ने उन्हें एमएस बिल्डिंग, मार्केटिंग बोर्ड और आईटी कंपनियों जैसे बेंगलुरु के महत्वपूर्ण आर्म्स हब की मार्केटिंग करने की सलाह दी। अंगूर के अलावा, उन्होंने 2016 के दौरान 2 एकड़ के क्षेत्र में भागवा नामक एक अनार की खेती शुरू कर दी, जिसमें उच्च घनत्व रोपण प्रणाली को अपनाकर 1,000 से अधिक आबादी वाले पौधे लगाए गए। 2017 में, एक ही फसल के साथ, उन्होंने 12 टन के कुल उत्पादन से 6 लाख रुपये की सकल आय पायी । मौजूदा सीज़न में, वह 2 एकड़ से 25 टन की उम्मीद कर रहा है और प्रत्येक संयंत्र से 25 किलोग्राम की बम्पर पैदावार ले रहा है। उन्होंने उसी विपणन रणनीति का उपयोग करके बेंगलुरु के विभिन्न स्थानों में खुदरा मूल्य से 30-40 रुपये प्रति किलो कम करके 80 रुपये प्रति किलो की दर से फल बेचना शुरू किया । बेंगलुरु में । उनके अनुसार, विक्रय मूल्य अभी भी किफायती है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष विपणन के साथ, वह 3 से 4 लाख रुपये के खर्च के साथ 16 से 18 लाख रुपये कमाने की उम्मीद करता है। श्री मुरलीधर कृषि विज्ञान से संबंधित पुस्तकों और लेखों को पढ़ते हैं और उन्होंने रेडियो, द्वारदर्शन और ईटीवी अन्नादता पर कई वार्ताएं की हैं। अंगूर, अनार, ड्रमस्टिक और चाउ-चाउ की वैज्ञानिक खेती में उनकी निरंतर प्रगति के कारण, बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट ने, उन्हें साल 2016-17 में टोटागरिका मेले के दौरान जिले के सर्वश्रेष्ठ बागवानी किसान के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने पावर टिलर का उपयोग करके जुताई, छिड़काव और अन्य कार्यों के लिए मशीनीकरण को भी अपनाया है। उनके पूरे खेत ने ड्रिप सिंचाई को अपनाया है और पानी के उर्वरक मिलाकर सभी पोषक तत्वों को पूरक बनाया है। कभी-कभी, वह IIHR, बेंगलुरू से खरीदे गए पर्ण आवेदन उत्पादों के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। अनार के लिए, वह नियमित रूप से अरका माइक्रोबियल कंसोर्टियम को लागू करता है और मिट्टी-जनित विल्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रबंधन करता है। वह नियमित रूप से अपनी फसलों के लिए ट्राइकोडर्मा, अर्का माइक्रोबियल कंसोर्टियम और बायोफर्टिलाइज़र भी शामिल करता है। अपने खेत में, वह एक वर्मी-कम्पोस्ट यूनिट, 6 लाख लीटर की पानी की क्षमता के साथ खेत तालाब और वर्षा जल संरक्षण तकनीकों का रखरखाव करता है। उनकी पूरी भूमि बाहरी खरीद पर आधार के बिना घर की जरूरतों के लिए उगाए गए फल, फूल और औषधीय और वृक्ष प्रजातियों की जैव विविधता का उदाहरण देती है। श्री मुरलीधर ने एकीकृत कृषि प्रणाली की अवधारणा के साथ अपनी आजीविका हासिल करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रगति की है।
एकीकरण सतत कृषि के लिए नई सफलता का मंत्र है।
एकीकरण सतत कृषि के लिए नई सफलता का मंत्र है। श्री प्रवीण, कर्नाटक के हसन जिले के चन्नारायणपटना तालुक के वगाराहल्ली गाँव के निवासी हैं, उनके गाँव के गरीब किसानों के लिए एक आदर्श है। उनकी कुल भूमि 1.69 हेक्टेयर है। परंपरागत रूप से, उन्होंने रागी, मक्का, आलू और नारियल जैसी फसलों को एक छोटी डेयरी और पोल्ट्री इकाई के साथ उगाया। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), हासन से तकनीकी सहायता ने उन्हें कृषि फसलों, बागवानी फसलों और रेशम कीट पालन के उन्नत किस्मों / संकरों के उपयोग के माध्यम से अपनी खेती को किनारे करने और एकीकृत करने में मदद की; अपनी डेयरी इकाई, मुर्गी पालन, सुअर पालन; भेड़ का स्टाल खिलाना; मवेशी फ़ीड के रूप में अज़ोला का उपयोग; कृमि खाद; कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से सह -3 चारा और कम करना। इससे पहले, उनकी आय का एकमात्र स्रोत रागी, मक्का, आलू और नारियल जैसी फसलों से था, जो उन्हें रु. 47,७४० की वार्षिक शुद्ध आय प्राप्त करते थे। । उच्च मूल्य वाली फसल अदरक और सेरीकल्चर की शुरुआत के साथ, उनकी वार्षिक आय बढ़कर रु. 2,37,५५८ हुई । उन्होंने नारियल के बीच ड्रमस्टिक और पपीता उगाना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। श्री प्रवीण ने हॉर्टी-सिल्वी-पेस्ट्री की खेती के साथ अपने खेत को विकसित किया है। उन्होंने सीमाओं के साथ सिल्वर ओक लगाए हैं, भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग किया है, और स्वर्णधारा (15), गिरिराज (15) और स्थानीय (20) पोल्ट्री नस्लों के साथ पिछवाड़े मुर्गी पालन शुरू किया है। इन पक्षियों से, उन्हें लगभग 4,230 अंडे और रु.49,780 मिलते हैं । इसके अलावा, उनके पास एक भेड़ और सूअर का इकाई है जो उन्हें क्रमशः रु. 23,950 और रु. 73,630 की अतिरिक्त आय लाने में मदद करता है। इसने अपने गांव में कई किसानों को पशुधन के साथ एकीकृत खेती शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। अपनी डेयरी (तीन होल्स्टीन फ्रेशियन गायों, दो नॉन्सस्क्रिप्ट गाय और एक भैंस) और भेड़ इकाई को खिलाने के लिए, उन्होंने केवीके, हसन की मदद से सह -3 और अजोला युक्त चारा ब्लॉक की स्थापना की है। खनिज मिश्रण के साथ अज़ोला के संयोजन ने उन्हें लागत पर रुपये प्रति दिन 150 की बचत करने में मदद की है। जल संरक्षण अभ्यास के रूप में, उन्होंने नारियल के बगीचे में एक सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणाली को अपनाया, जिससे बाढ़ सिंचाई की तुलना में जल उपयोग दक्षता में वृद्धि हुई। वह फार्म ड्रगरी को कम करने के लिए नारियल की लकड़ी और साइकिल के खरपतवार जैसी कृषि मशीनरी का उपयोग करता है। उन्होंने 2012-13 में नारियल पर चढ़ने और पौधों की सुरक्षा पर व्यावसायिक प्रशिक्षण भी लिया। वह केवीके, हासन द्वारा आयोजित तालीम चढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान एक मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करता है, और पड़ोसी किसानों की सहायता भी करता है। श्री प्रवीण वर्मी-कम्पोस्ट यूनिट के माध्यम से खेत के कचरे को स्वस्थ खाद में बदल देते हैं और खेत के भीतर उपलब्ध जैव द्रव्यमान को पुन: चक्रित करके 50% से अधिक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उन्होंने नारियल के बगीचे में सन गांजा की खेती की और जैव द्रव्यमान (हरी खाद) को शामिल किया। प्रति वर्ष उनके खेत से औसत उत्पादन 5,400 नारियल, 10 टन वर्मी-कम्पोस्ट, 5 टन गाय का गोबर, 40 टन चारा घास और सब्जियों की कीमत 1 लाख होती है। थोड़े समय के भीतर, श्री प्रवीण एक बेहतर आजीविका के साथ एक सफल किसान में बदल गए। यूएएस, बेंगलुरु ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ तालुक स्तर के युवा किसान से सम्मानित किया। इसके अलावा, वह व्याख्यान देते हैं और प्रशिक्षुओं और पड़ोसी किसानों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। उनकी सफलता इस तथ्य में परिलक्षित होती है कि वे 1.69 हेक्टेयर भूमि से रु 7.28 की कुल वार्षिक आय अर्जित करते हैं। उसकी वह इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह एकीकृत कृषि पद्धतियों को अपनाना किसानों के लिए आगे का रास्ता हो सकता है।
चारे की फ़सलों के साथ डेयरी फार्मिंग का चलन।
चारे की फ़सलों के साथ डेयरी फार्मिंग का चलन। श्री जी. श्रीनिवासुलु नारायणपुरम गाँव, कल्याणदुर्ग मंडल, अनंतपुर जिले, आंध्र प्रदेश, भारत से हैं। अनंतपुर जिले के अधिकांश खेत (90%) सूखे कृषि के अंतर्गत हैं। श्री श्रीनिवासुलु इससे जुड़े जोखिम के बावजूद 10 वर्षों से डेयरी उद्यम का अभ्यास कर रहे हैं: खर्च का 60-70% चारे की ओर जाता है। चारे की कमी से अनंतपुर में पशुधन आबादी में गिरावट आई है और इस प्रकार यह डेयरी किसानों के लिए गैर-पारिश्रमिक बन जाता है। श्री श्रीनिवासुलु एक लीटर दूध का उत्पादन करने में नुकसान का सामना कर रहे थे और उच्च लागत का सामना कर रहे थे। वह भारी नुकसान के कारण डेयरी छोड़ना चाहता था और यह गैर-पारिश्रमिक था। डेयरी फार्मिंग छोड़ने से पहले, इन समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए उन्होंने श्रीमती लक्ष्मी देवी कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), कल्याणगढ़ से संपर्क किया। अपनी समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद, केवीके के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वह बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा है क्योंकि चारा बाहर से मंगवाया गया था। केवीके वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि वह एक नई और बेहतर उपज देने वाली और सूखा सहन करने वाली हाइब्रिड नेपियर किस्म को फुले जयवंत (आरबीएन -13) कहते हैं। प्रारंभ में, उन्होंने हाइब्रिड नेपियर के कुछ नमूने लिए और उन्हें 500 वर्गमीटर क्षेत्र में लगाया। बाद में, उन्होंने इसे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में गुणा और बढ़ाया। केवीके के हस्तक्षेप के साथ, श्री श्रीनिवासुलु ने हरे चारे की कमी को दूर किया और बाजार से चारा खरीदना बंद कर दिया। अब, वह प्रति वर्ष लगभग 95-120 टन हरा चारा का प्रबंधन कर सकता है, जो न्यूनतम खर्च के साथ 8 डेयरी दुधारू पशुओं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। उचित चारे की खेती ने उन्हें दूध की अधिक पैदावार लेने के अलावा 80% तक खर्च करने में सक्षम बनाया। श्री श्रीनिवासुलु ने अपने अनुभव साझा करके अपने किसानों को चारे की खेती पर मार्गदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने आसपास के गाँवों को भी चारे की बिक्री शुरू की, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हुई। वह आसपास के गांवों में एक रोल मॉडल बन गया है। अब तक, उन्होंने 20 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 25 किसानों को मुफ्त में चारे की आपूर्ति की है, जिसने किसानों के लिए दूध की पैदावार और शुद्ध रिटर्न में सुधार करने में योगदान दिया है। वह कृषि और संबद्ध गतिविधियों के बारे में समय पर जानकारी के लिए KVK, विस्तार एजेंटों और कृषि विभाग के साथ नियमित संपर्क में है। उन्हें अपने गांव में एक अभिनव किसान कहा जाता है क्योंकि शोध संस्थानों द्वारा सुझाई गई नई तकनीकों को लागू करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं।
पंजाब में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आगे का एक नया रास्ता देता है।
पंजाब में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आगे का एक नया रास्ता देता है। श्री सरवन सिंह चंडी, भारत के पंजाब प्रांत के कपूरथला जिले के बूलपुर गाँव के रहने वाले हैं और उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्होंने कृषि को करियर के रूप में शुरू किया। वह कृषि के क्षेत्र में कुछ उपन्यास करना चाहते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों से 14 एकड़ ज़मीन प्राप्त की और 16 एकड़ ज़मीन लीज़ पर खरीदी। उन्होंने पंजाब में चावल-गेहूं की खेती प्रणाली के मोनोकल्चर के कारण हर साल घटती जल तालिका का अवलोकन किया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के वैज्ञानिकों के साथ उनके लगातार संपर्क से, उन्हें विविध कृषि प्रणाली के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी भूमि के 30 एकड़ क्षेत्र में विविध खेती शुरू की, जिसमें अनाज, दालें, चारा फसलें, फूलों की खेती, तिलहन, मधुमक्खी पालन, फलों की खेती जैसी विभिन्न फसलों के संयोजन शामिल हैं। उन्होंने सिंचाई सुविधाओं के विवेकपूर्ण उपयोग में सहायता के लिए सब्जी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी स्थापित की। खरीफ के मौसम में, वह धान, बासमती, चारा, दाल और प्याज उगाते हैं, जिससे उन्हें रु.9,50,250 / - की कुल आय होती है। । विविधतापूर्ण फसल पद्धति से उसे रु। की आय उत्पन्न करने में मदद मिलती है। रु. 3,29,000 / - गेहूं से, रु. 3,15,000 / - आलू से, रु. 40,000 / - दालों से, रु.2,50,000 / - बेल मिर्च से, रु.18,000 / - सूरजमुखी से, रु. 60,000 / - बरसेम से और रु. 25,000 / - मैरीगोल्ड से। उनकी कुल आय रु.10,37,000 / - रबी सीजन के दौरान । विविध क्रॉपिंग प्रणाली से उन्हें रु. 1,38,091 / -की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। दोनों सत्रों से उनकी कुल आय रु. 19,87,250 / - प्रति वर्ष है। श्री चंडी ने अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक पौष्टिक किचन गार्डन बनाया है। वह घरेलू खपत को पूरा करने के लिए सात दुधारू पशुओं का पालन करता है और अतिरिक्त दूध उत्पन्न करता है (प्रतिदिन 3,000 रुपये)। उन्होंने मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण लिया और मधुमक्खी के छत्ते के 50 बक्से खरीदे। पहले वर्ष में, उन्होंने 350 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया, जिसने उन्हें अधिक उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। बाद में, उन्होंने अपना शहद प्रमाणित (एगमार्क) पंजाब सरकार और भारत सरकार से प्राप्त किया। उन्होंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना से आधुनिक पैकिंग तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त किया और "लॉयन ब्रांड शहद" नाम से अपना शहद बेचना शुरू किया। उन्होंने विश्वविद्यालय और कृषि विशेषज्ञों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा और 2011 में अपनी खुद की शहद प्रसंस्करण इकाई शुरू की। वर्ष 2002 में संगरूर में एक राज्य स्तरीय समारोह में सहकारिता विभाग की ओर से उन्हें कृषि मंत्री श्री चौधरी अजीत सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें मार्च 2008 में पीएयू, , लुधियाना में आयोजित किसान मेले में मुख्यमंत्री का पुरस्कार मिला। उन्हें कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने पंजाब में आयोजित विभिन्न किसान मेलों में फसल प्रतियोगिताओं में 52 पुरस्कार जीते। उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले शहद के उत्पादन के लिए रिकॉर्ड 14 बार प्रथम पुरस्कार मिला। उन्होंने अन्य किसानों को किसान मेला और किसान गोष्ठी आदि में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। श्री चंडी की सफलता ने विभिन्न मल्टीमीडिया चैनलों के माध्यम से अन्य किसानों को प्रेरित किया है। उन्होंने कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ गाँव स्तर पर और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किया है। प्रगतिशील खेती के उनके उपन्यास दृष्टिकोण ने उन्हें आर्थिक प्रगति के रास्ते पर धकेल दिया है। वह उच्च आय और स्थिरता के लिए कृषि में विविधीकरण को अपनाने के लिए कृषक समुदाय के लिए एक रोल मॉडल और ज्ञान का एक बीकन बन गया है।
प्रति बूंद अधिक फसल।
प्रति बूंद अधिक फसल। श्री मंजीत सिंह सलूजा (51), राजनांदगांव जिले, छत्तीसगढ़ राज्य, भारत के एक प्रसिद्ध प्रगतिशील किसान हैं। वह 20 साल की उम्र से अपने पिता के साथ खेती से जुड़े हुए हैं। शुरुआत से ही वे नई उत्पादन तकनीकों को सीखने और अपनाने के इच्छुक थे। इस जुनून ने उन्हें कृषि में पेश आने के दौरान ड्रिप सिंचाई को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें अपने खेत में सब्जी की खेती के लिए स्थापित एक स्वचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली, नेताजीत मिली। वर्तमान में, वह प्रयोगात्मक आधार पर 25 एकड़ भूमि पर सब्जियों और फलों की विदेशी किस्मों की खेती कर रहा है। उन्होंने सब्जियों और अनाज दोनों फसलों के लिए इस तकनीक के साथ काम किया है। उनकी विशेषज्ञता और प्रयोग फल की खेती के लिए विस्तारित हुए, और उन्होंने मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हर साल मार्च से जून तक फसल रोटेशन और फार्म यार्ड खाद (FYM) का उपयोग किया और क्षेत्र की परती रखी। उन्होंने एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन को भी अपनाया। उन्होंने प्रत्येक फसल के आय, व्यय, उत्पादन और बिक्री प्रबंधन के रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है। समय के साथ, उन्होंने खेतिहर मजदूरों की उच्च मजदूरी के कारण अपने खेत में श्रमिक समस्याओं का सामना करना शुरू कर दिया। इस समस्या को दूर करने के लिए, उन्होंने अपने खेत में काम करने वालों को अपने व्यवसाय में काम करने वाले भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। हालांकि शुरुआत में प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं थी, समय के साथ, यह काफी बेहतर हो गया और वह खेतिहर मजदूरों की कमी की समस्या को हल करने में सक्षम हो गया। व्यावसायिक खेती के अलावा, वह एक रसोई घर का रखरखाव करता है। उन्होंने राजनांदगांव में अपने फार्महाउस में जैविक सब्जियां उगाना शुरू किया। शुरुआती वर्षों में, उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उपज साझा की, और गुणवत्ता और स्वाद के बारे में उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर, उन्होंने इसे वाणिज्यिक पैमाने पर विस्तारित किया। जैसे ही ताज़ी कृषि उपज के लिए उपभोक्ता आधार में वृद्धि हुई, उन्होंने खुद ही इस क्षेत्र में एक रिटेल आउटलेट खोला और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपज बेचना शुरू किया। आखिरकार, उन्होंने कृषि के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू किया और लोगों को आश्वस्त किया कि कृषि भी पारिश्रमिक हो सकती है। 2003 में स्पाइस बोर्ड ऑफ़ इंडिया, कोचीन द्वारा "कृषक सम्मान समरोह" और "मिर्ची में प्रगतिशील खेती अभ्यास" में उनकी कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयासों को कृषि विभाग, राजनांदगांव द्वारा सम्मानित और सराहा गया। 2013 में, उन्हें महिंद्रा एग्री टेक द्वारा आयोजित पश्चिम क्षेत्र के लिए "कृषि सम्राट सम्मान" से सम्मानित किया गया। 2013 में, उन्हें कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, और CICR, नागपुर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित कृषि मेले में कृषि विभाग द्वारा "इनोवेटिव फार्मर" होने के लिए सम्मानित किया गया। वह राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राजनांदगांव (CG), और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA), राजनांदगाँव के सदस्य हैं, जिसने उन्हें इन संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अन्य किसानों और कृषि अधिकारियों के साथ अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने में सक्षम बनाया है। भविष्य के लिए उनकी योजना अच्छी पैदावार का श्रेय देने वाली फसलों के लिए खेती के क्षेत्र का विस्तार करना है।