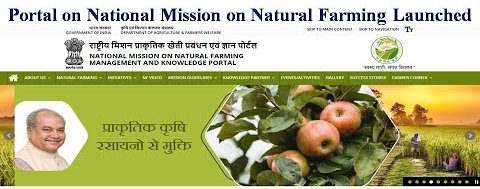1. Add well decomposed FYM to soil. 2. Make nursery beds of 1mt width and 15 cm high. 3. Drench the soil with 0.2 percent Bavistin or Captan before sowing the seeds. 4. Seed rate 40-50gm/ kanal or 800-1000gm/ hactare. 5. Best time of nursery raising is ending week of April to Second week of May. 6. Transplanting should be done when seedling attains three to four pair of true leaves. 7. Spacing of 45 x 45 cm should be followed 8. Apply 200 kg/ ha. Nitrogen in two split doses. First after 20days after transplanting and second after 45 days. 9. Pinching after 40 days of transplanting to encourage more lateral shoots. 10. The flowers should be harvested early in the morning. 11. Yield in case of variety Pusa Naranga is 200-300 qtls/ha. 12. Store flowers in cool place before packing.
Training
Management of root rot
Step 1 First of all dig the soil around the root zone Step 2 Expose the infected roots Step 3 Apply chaubatia paint on infected parts Step 4 Leave the portion for exposure t the sun Step 5 Fill the portion with fresh soil Repeat the same after one month
لہسن کا پاوڈر بنانے کا تریکا
ہم اکثر لہسن کا پیسٹ بناکر رکھ دیتے ہیں جو جلدی خراب ہو سکتا ہے. ہم اگر لہسن کو سکھا کر پاوڈر بنا کر رکھیں وہ زیادہ عرصہ تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. اس لئے آج میں آپ کو لہسن کا پاوڈر بنانے کا طریقہ سکھاتی ہوں لہسن کو چھیل کر اس کا پیسٹ بنا ئیں اس پیسٹ کو صاف برتن یا کپڑے پر تین سے چار دن دھوپ میں سکھایں اس کے بعد اس کو کوٹ کر اسکا پاوڈر بنایں اس پاوڈر کو آپ مہینوں سٹور کر سکتے ہیں یا اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں .
Cumin Farming - जीरा की खेती.......!
इसे ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा के नाम से जाना जाता है। जीरा अपनी तेज सुगंधित गंध और मसालेदार स्वाद के कारण एक प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की पाक तैयारियों में स्वाद बढ़ाने वाले कम्पाउंड के रूप में किया जाता है। किसानों के बीच फसलों की लोकप्रियता और वरीयता के पीछे बढ़ने की छोटी अवधि और उच्च शुद्ध प्रतिफल का गुण हैं। भारत में जीरे की खेती ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रबी की फसल के रूप में की जाती है। राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में जीरे के कुल उत्पादन में 99% का योगदान है। @जलवायु मध्यम ठंडी और शुष्क जलवायु में फसल की सफलतापूर्वक खेती की जाती है। यह फूल आने और बीज बनने की अवस्था के दौरान वातावरण में नमी को पसंद नहीं करता है क्योंकि यह कई बीमारियों के हमले का शिकार होता है। यह फूल आने और फल लगने की प्रारंभिक अवस्था के दौरान पाले से क्षति के प्रति भी अतिसंवेदनशील होता है। इसलिए, जीरे की खेती उस क्षेत्र में प्रतिबंधित है, जहां वायुमंडलीय आर्द्रता कम है और सर्दियां गंभीर नहीं हैं। पुष्पन या जल्दी फल लगने के दौरान और परिपक्वता अवधि के समय बार-बार बारिश अत्यधिक अवांछनीय है। @ मिट्टी जीरे की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, हालांकि या तो कम कार्बनिक पदार्थ वाली रेतीली मिट्टी या अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाली चिकनी दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। मिट्टी में जल निकासी की बेहतर सुविधा होनी चाहिए क्योंकि रुका हुआ पानी और अत्यधिक नमी जीरे की फसल के लिए बहुत हानिकारक होती है। यह बताया गया है कि जीरे को मृदा निलंबन ईसी, 14.0 डीएसएम-1 और बीज मसालों के बीच उच्चतम लवणता सहिष्णु के तहत अच्छी तरह से अपनाया जा सकता है। थोड़ी खारी मिट्टी या सिंचाई के पानी में बीज भरना बेहतर होता है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जीरा किसानों के लिए वरदान है। इसे गहरी, उथली दोनों तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, हालांकि अच्छी मिट्टी की सरंध्रता और जल निकासी की सुविधा वाली बजरीदार या पथरीली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। @ खेत की तैयारी दीमक प्रवण क्षेत्रों में हैरो या देसी हल से 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें। पाटा लगाने से पहले मिट्टी में एंडोसल्फान 4.0%, क्विनालफॉस 1.5% मिलाना चाहिए। फिर तख्ती की सहायता से खेत को समतल कर लें। सिंचाई नालियों के प्रावधान के साथ सुविधाजनक क्यारियां तैयार की जाती हैं। गोबर की खाद या कम्पोस्ट को तीसरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। @ बीज * बीज दर विभिन्न राज्यों के लिए जीरे के लिए अनुशंसित बीज दर। गुजरात - 16-20 किग्रा/हेक्टेयर राजस्थान - 12-15 किग्रा/हेक्टेयर तमिलनाडु - 8-10 किग्रा/हेक्टेयर *बीज उपचार बीज जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा कल्चर (10 ग्राम/किग्रा बीज) या थीरम या कार्बेन्डाजिम @ 2.5 ग्राम/किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए। @ बुवाई *बोने का समय गुजरात - नवंबर का पहला सप्ताह राजस्थान -15-30 नवंबर तमिलनाडु - नवंबर का पहला पखवाड़ा आंध्र प्रदेश - नवंबर का पहला पखवाड़ा मध्य प्रदेश - नवंबर का पहला सप्ताह उत्तर प्रदेश - 15-30 नवंबर * रिक्ति बीजों को 1 सेमी, 22. सेमी और 30 सेमी की दूरी पर खींची गई रेखाओं में बोया जाता है। लाइन से लाइन की दूरी 25 सेमी रखी जानी चाहिए। बीज को 1.5 सेमी से अधिक गहरा नहीं बोना चाहिए। *बुवाई की विधि जीरे की बुवाई दो विधियों से की जाती है, लाइन बुआई और ब्रॉडकास्टिंग। जीरे की बुवाई के लिए सीड ड्रिल का भी उपयोग किया जा सकता है। @ उर्वरक उर्वरक की आवश्यकता मिट्टी की उर्वरता स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए मिट्टी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही खाद का प्रयोग करना चाहिए। फसल की बुवाई से तीन सप्ताह पहले 10 टन/हेक्टेयर गोबर की खाद या 5 टन/हेक्टेयर खाद डालें। 15 किग्रा N, 20 किग्रा P2O5 और 20 किग्रा K2O / हेक्टेयर बेसल खुराक के रूप में डालें और शेष 30 किग्रा बुवाई के 60 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालें। @ सिंचाई अच्छे अंकुरण के लिए बिजाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बीज का अंकुरण बोने के 10-12 दिन बाद दिखाई देगा। मौसम की स्थिति और मिट्टी के प्रकार के आधार पर लगभग 30 दिनों के अंतराल पर फसल की सिंचाई की जाती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब फसल परिपक्वता अवस्था में हो तो सिंचाई से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बीज की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। स्प्रिंकलर भी जीरे की खेती के लिए अच्छा होता है जब पौधा मुरझाने की स्थिति में होता है। जीरे की खेती में ड्रिप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। @ खरपतवार नियंत्रण फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए आमतौर पर 2-3 निराई-गुड़ाई की आवश्यकता होती है। फ्लुक्लोरालिन @ 0.77 से 1.00 किग्रा/हेक्टेयर या बेसालिन @ 2.5 किग्रा/हे या स्टैम्प एफ-34 @ 3.33 किग्रा/हेक्टेयर की दर से उगने से पहले कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।एनआरसीएसएस, अजमेर में जीरा में खरपतवार के नियंत्रण के लिए 75 ग्राम/हेक्टेयर की दर से ऑक्सिडियागल का पूर्व-उद्भवन अनुप्रयोग बहुत प्रभावी बनाया गया है। ये खरपतवारनाशी बुवाई के बाद लेकिन खरपतवार के अंकुरण से पहले डालना चाहिए। @ फसल सुरक्षा * पाले से चोट लगना फसल के मौसम के दौरान तापमान में अचानक गिरावट आने वाले क्षेत्र में कभी-कभी जीरा पाले से प्रभावित होता है। जीरा प्रारंभिक फूल और बीज निर्माण चरण के दौरान ठंढ के लिए अतिसंवेदनशील होता है। पाले की प्रत्याशा में फसल की सिंचाई करना बेहतर होता है यदि वातावरण साफ हो, हवा बहना बंद हो जाए और पाले के अचानक तापमान में गिरावट की आशंका हो। खेत में धुएँ की भी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे फसल को पाले से बचाया जा सके। इसके साथ ही फसल को पाले से बचाने के लिए 0.1% कमर्शियल H2SO4 का प्रयोग प्रभावी पाया गया है। *पीड़क 1. एफिड जीरे पर एफिड्स का निर्माण वानस्पतिक अवस्था में शुरू होता है और फूल आने से लेकर बीज बनने के चरणों तक चरम पर होता है। समय से बोई गई फसल की तुलना में देर से बोई गई फसल को अधिक नुकसान होता है। अधिकतम तापमान में वृद्धि और वर्षा के साथ सापेक्षिक आर्द्रता में कमी का एफिड आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ट्रैपिंग: पीले रंग पंखों वाले एफिड्स को आकर्षित करते हैं और कीट को फंसाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। एफिड की आबादी को कम करने के लिए स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया है। नीम के बीज की गुठली के अर्क (NSKE) @ 5% या नीम के तेल 2% का छिड़काव प्रभावी रूप से फसल पर एफिड्स की शुरुआती आबादी को कम करता है। एंटोमोपैथोजेन वर्टिसिलियम लेकेनी (108 स्पोर/जी) पाउडर फॉर्मूलेशन @ 5.0 ग्राम/लीटर पानी के प्रयोग से अच्छे परिणाम मिलते हैं। उच्च एफिड आबादी में सिंथेटिक कीटनाशकों में से कोई एक यानी डायमेथोएट 0.03%, मेटासिटॉक्स - 0.03%, इमामेक्टिन बेंजोएट @10 ग्राम एआई / हेक्टेयर, या इमिडाक्लोरप्रिड - 0.005%।का छिड़काव करना चाहिए। 2. थ्रिप्स थ्रिप्स का प्रकोप फसल की प्रारंभिक वानस्पतिक वृद्धि के समय शुरू होता है और फूल आने की अवस्था तक पाया जाता है। ये पौधे की पत्तियों को चूसते हैं और पत्तियों को पीला और सुखा देते हैं। अधिक जनसंख्या के कारण पूरे पौधे सूख जाते है। नीम के बीज की गुठली के अर्क (NSKE) का 5% या नीम के तेल का 2% या डाइमेथोएट -0.03% या मेटासिस्टॉक्स - 0.03% या थायोमेथोक्सम - 0.025% का छिड़काव प्रभावी रूप से कीट नियंत्रण करता है। * रोग 1. झुलसा संक्रमित पौधे पत्तियों और तने पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित पौधे मुरझा जाते हैं। रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब (0.2%) या डाइफेनोकोनाज़ोल (0.05%) या एज़ोक्सिस्ट्रोबिन (0.1%) को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर दोहराया जाना चाहिए। बुवाई के 45-60 दिनों के अंतराल पर मैंकोजेब के छिड़काव के बाद 15 दिनों के अंतराल पर डाइफेनोकोनाजोल या एज़ोक्सिस्ट्रोबिन के 2-3 छिड़काव प्रभावी ढंग से रोग का प्रबंधन करते हैं। 2. विल्ट संक्रमित पौधे से पत्तियों गिर जाती है और बाद में पौधे की मृत्यु हो जाती है। मुरझाने का संक्रमण फसल वृद्धि के किसी भी स्तर पर पैच में हो सकता है। जीरे में मुरझान आने के बाद नुकसान को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। उसे गैर-मेज़बान फ़सलों के साथ कम से कम तीन वर्ष का फ़सल चक्र अपनाना चाहिए। बुवाई के लिए स्वस्थ एवं रोगमुक्त बीजों का क्रय करना चाहिए। बीज बोने से पहले उचित/अनुशंसित कवकनाशी या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों के दौरान 2-3 सप्ताह के लिए मिट्टी के सौरीकरण के बाद ट्राइकोडर्मा विरिडे के साथ बीज उपचार रोग के प्रबंधन के लिए प्रभावी होता है। ट्राइकोडर्मा प्रजातियों के कंसोर्टिया के साथ बीज उपचार (10 ग्राम/किग्रा) और मिट्टी का अनुप्रयोग (2.5 किग्रा/हेक्टेयर 50 किग्रा एफवाईएम के साथ मिश्रित) भी जीरे के मुरझान रोग के प्रबंधन के लिए प्रभावी है। 3. फफूंदी प्रारम्भिक अवस्था में पौधों की पत्तियों एवं टहनियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। बाद में पूरा पौधा इस सफेद चूर्ण से ढक जाता है। जीरे में फफूंदी रोग की शुरुआत से 15 दिनों के अंतराल पर 20-25 किग्रा/हेक्टेयर की दर से गंधक के छिड़काव या घुलनशील सल्फर 0.2% का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है। @ कटाई किस्म और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर फसल 80-120 दिनों में पक जाती है। कटाई तब की जाती है जब फसल पीली हो जाती है, पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं और बीज हल्के भूरे भूरे रंग के हो जाते हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान व्यक्तिगत पौधे को उखाड़कर या जमीन के करीब काटकर फसल की कटाई की जाती है। @ उपज उन्नत किस्मों से 8-10 क्विंटल/हेक्टेयर जीरे की उपज मिलती है।
Poppy Farming - भारत में कानूनी अफीम उत्पादन........!
भारत में कानूनी अफीम उत्पादन। हर साल केंद्र सरकार उन चुनिंदा ट्रैकों को अधिसूचित करती है जहां ऐसी खेती की अनुमति होगी, और लाइसेंस की पात्रता के लिए सामान्य शर्तें। लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक शर्त न्यूनतम योग्यता पैदावार (एमक्यूवाई) मानदंड को पूरा करना है, जो प्रति हेक्टेयर किलोग्राम की संख्या में निर्दिष्ट है। पिछले वर्ष में कम से कम इस मात्रा में निविदा करने वाले कृषक लाइसेंस के लिए पात्र हैं। अन्य स्थितियों के बीच लाइसेंस, अधिकतम क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है जिसमें अफीम की फसल बोई जा सकती है। फसल वर्ष 1 सितंबर से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को समाप्त होता है। कुछ स्थान जहाँ अफीम उगाई जाती है, वे हैं राजस्थान में प्रतापगढ़; मंदसौर, मध्य प्रदेश में नीमच; रतलाम और उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, बरेली, लखनऊ और फैजाबाद। फसल वर्ष 2008-09 के लिए, जारी किए गए लाइसेंसों की कुल संख्या 44821 थी, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए MQY 56 किलोग्राम / हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के लिए 49 किलोग्राम / हेक्टेयर निर्धारित किया गया था। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (भारत), 1985 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रूल्स (इंडिया, 1985) के प्रावधानों के अनुसार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) खेती की संपूर्ण निगरानी के लिए जिम्मेदार है । CBN के अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र को मापते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित करता है कि कोई अतिरिक्त खेती न हो। अफीम का निष्कर्षण फरवरी और मार्च के महीनों के दौरान होती है। किसान अभी भी पारंपरिक पद्धति का उपयोग करते हैं, जहां वे प्रत्येक खसखस कैप्सूल को ब्लेड जैसे विशेष उपकरण के साथ मैन्युअल रूप से लांस करते हैं, एक प्रक्रिया जिसे लांसिंग कहा जाता है। लांसिंग दोपहर या शाम को की जाती है। अफीम लेटेक्स जो रात में बाहर निकलता है और निकलता है, अगली सुबह मैन्युअल रूप से स्क्रैप और एकत्र किया जाता है। प्रत्येक खसखस कैप्सूल को तीन से चार लांसिंग दिया जाता है। इस तरह के सभी अफीम को आवश्यक रूप से सरकार को निविदा देने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से अप्रैल के प्रारंभ में अफीम संग्रह केंद्रों की स्थापना की जाती है। केंद्रों पर गुणवत्ता और निरंतरता और वजन के लिए अफीम की जाँच की जाती है। कीमतों का भुगतान किया जाता है जो सरकार द्वारा स्लैब दरों में तय होती हैं, जो अफीम की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करती है। 90% भुगतान काश्तकारों को ई-भुगतान विधि के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है। अफीम कारखाने में प्रयोगशाला परीक्षण के बाद यह पुष्टि करने के बाद कि कोई मिलावट नहीं मिली है अंतिम भुगतान किया जाता है। खरीदे गए सभी अफीम को नीमच और गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम और अल्कलॉइड कारखानों में भेजा जाता है। अफीम को निर्यात के लिए इन कारखानों में सुखाया और संसाधित किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों जैसे कोडीन फॉस्फेट, थेबैइन, मॉर्फिन सल्फेट, नोस्कैपीन आदि के निष्कर्षण के लिए भी किया जाता है।
Sandalwood Farming - चंदन की खेती……!
चंदन के पेड़ को मुख्य रूप से चंदन या श्रीगंधा के नाम से जाना जाता है और यह सबसे महंगा पेड़ है। उष्णकटिबंधीय भारतीय चंदन और समशीतोष्ण शुष्कभूमि ऑस्ट्रेलियाई चंदन दो किस्में हैं जो आमतौर पर उगाई जाती हैं। भारत में चंदन के दो रंग होते हैं सफेद, पीला और लाल। चंदन के पेड़ भारतीय परंपरा में एक प्रमुख स्थान रखते हैं और इसका उपयोग भारतीय लोग पालने से लेकर दाह संस्कार तक करते हैं। चंदन एक सदाबहार पेड़ है जिसका उपयोग ज्यादातर व्यावसायिक, चिकित्सीय, कॉस्मेटिक और दवाओं में किया जाता है। इसका उपयोग फार्मास्युटिकल, अरोमाथेरेपी, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र और साबुन उद्योग में भी किया जाता है। इस कारण से, भारतीय बाजार में चंदन के पेड़ या तेल का व्यावसायिक मूल्य बहुत अधिक है। चंदन के पेड़ की पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। @ जलवायु चंदन बहुत सारे स्थानों पर उगता है, जिसमें बहुत धूप होती है, मध्यम वर्षा होती है और वर्ष के हिस्से के लिए काफी शुष्क मौसम होता है। वे 12 ° -30 ° C की तापमान उचित हैं। वार्षिक वर्षा 850-1200 मिलीमीटर (33-47 इंच) की सीमा में होनी चाहिए। ऊंचाई के संदर्भ में, वे 360 और 1350 मीटर (1181-4429 फीट) के बीच कुछ भी संभाल सकते हैं, लेकिन 600 और 1050 मीटर (1968-3444 फीट) के बीच की मध्यम ऊंचाई पसंद करते हैं। @ मिट्टी किसी भी ऐसी मिट्टी ना चुने , जिसमें जल जमाव हो, जिसे चंदन सहन नहीं करता है। यदि आप एक रेतीली मिट्टी में रोपण कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि पानी जल्दी नहीं निकलता है। चंदन लाल भुरभुरी दोमट मिट्टी को तरजीह देता है।चंदन को रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी और वर्टिसोल में भी लगाया जा सकता है। चंदन चट्टानी जमीन और बजरी वाली मिट्टी को सहन करता है।मिट्टी का पीएच 6.0 और 7.5 के बीच होना चाहिए। @ खेत की तैयारी चंदन की खेती के लिए पहले खेत की अच्छी से गहरी जुताई करे उसे दो या तीन बार पलटी हल से मिट्टी को अच्छे से पलटवार करे फिर उसमे रोटावेटर चलाकर जमींन को समतल बना ले, फिर 12 x 15 फीट की दुरी पर पौधा लगाने के लिए जगह को चिन्हित करे, इसमें पौधे से पौधे की दुरी 12 फीट और क्यारी से क्यारी की दुरी 15 फीट रहेगी | तत्पश्चात उसमे 2*2 फिट का गडडा बनाकर उसे 15 से 20 रोज सुकने दे जिससे उस गड्डे में कुछ हानिकारक किट जो पोधे को नुकसान पंहुचाते है वह समाप्त हो जायेगे जिससे पोधे को कोई नुकसान नहीं होगा | गड्डो में कम्पोस्ट खाद व रेती को मिक्स कर के डालना चाहिये , जहा पर पहले से तीली भूमि है वहा रेत डालने की आवश्यकता नही है | @ बीज बीजों को भिगो कर सुखा लें|चंदन के बीज को 24 घंटे के लिए भिगो दें। उन्हें सूरज के पूर्ण प्रकाश के तहत सूखने दें। 1 दिन धूप में रहने के बाद, आपको बीज में एक दरार विकसित होती हुई दिखनी चाहिए। इस बिंदु पर, यह अंकुरण के लिए तैयार है। @ मिश्रण बनाना कुछ लाल मिट्टी, मवेशी खाद और रेत की आवश्यकता होगी। एक व्हीलब्रो या अन्य कंटेनर में, 2 भाग लाल मिट्टी,1 भाग खाद और 1 भाग रेत मिलाएं। इस मिश्रण के साथ रोपण ट्रे भरें। यदि आप सीधे बीज बोने की योजना बनाते हैं, तो बीज बोने से पहले रोपण गड्ढे को इस मिश्रण से भरें। @ नर्सरी रोपण एक छोटे कंटेनर में चंदन के बीज रोपें, जैसे कि एक पुनर्नवीनीकरण कार्टन या रोपण ट्रे। कंटेनर को तैयार पॉटिंग मिक्स के साथ भरें। बीज को मिट्टी की सतह के नीचे ¾-1 इंच (1.75-2.54 सेंटीमीटर) पर रखें। प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा पानी दें, लेकिन मिट्टी को जल देने से बचें, क्योंकि चंदन का पेड़ सूखी परिस्थितियों को तरजीह देता है। आप देखेंगे कि बीज 4 से 8 सप्ताह के भीतर अंकुरित होने लगते हैं। यह देखने के लिए कि क्या पानी की जरूरत है, अपनी उंगली को मिट्टी में 1 इंच (2.5 सेमी) डालें। यदि आपकी उंगली सूखी महसूस होती है, तो आपको मिट्टी को पानी देना होगा। गमले की मिट्टी को भिगोने से बचें, क्योंकि चंदन के बीज जलयुक्त मिट्टी को सहन नहीं करते हैं। @ बुवाई *बुवाई का समय जब रोपाई लगभग 1 महीने की हो, तो आपको उन्हें ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होगी। चंदन का प्रत्यारोपण करने का सबसे अच्छा समय मई और अक्टूबर के बीच है। * रिक्ति पौधे से पौधे की दुरी 12 फीट और क्यारी से क्यारी की दुरी 15 फीट रहेगी | * बुवाई की विधि रोपण ट्रे के किनारों के चारों ओर मिट्टी को ढीला करने के लिए अपने ट्रॉवेल का उपयोग करें। अपनी उंगलियों को ट्रे के किनारों पर रखें और चंदन के अंकुरण को ऊपर खींचें। इसे रूट बॉल से पकड़कर, धीरे से रोपण गड्ढे में रखें। बहुत गर्म होने से पहले सुबह अंकुरण को प्रत्यारोपण करना सबसे अच्छा है। सुनिश्चित करें कि अंकुरण और रोपण गड्ढे के बीच की जगह पूरी तरह से मिट्टी से भरी हुई है, क्योंकि आपको किसी भी संभावित जलभराव से बचने की आवश्यकता है। @ होस्ट के साथ चंदन का पौधा लगाना चंदन केवल तभी पनप सकता है जब यह एक अन्य पौधे के साथ बढ़ता है जो निश्चित नाइट्रोजन, एक प्रकार का प्राकृतिक उर्वरक पैदा करता है। चंदन का पेड़ अपनी जड़ प्रणाली को उस होस्ट पेड़ से जोड़ता है जिससे उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आदर्श रूप से, आपको पहले से ही स्थापित होस्ट प्रजातियों के बगल में अपने चंदन का पौधा लगाना चाहिए, जैसे कि लंबे समय तक रहने वाले बत्तख (बबूल के पेड़) या कैसुरिनास (उष्णकटिबंधीय सदाबहार का एक जीनस, जिसमें आयरनवुड और शूकर शामिल हैं)। होस्ट प्लांट के रूप में नीम ,केजुरिना ,अमलतास ,सिताफल ,अमरुद ,आदि पौधे महत्वपूर्ण है| उन्हें चंदन के पेड़ों के बीच 1.6-2 मीटर (5.2-6.5 फीट) के अंतराल पर रखें। @ उर्वरक आप फसल की उच्च उपज प्राप्त करने के लिए अपने चंदन के खेतों में बायो उर्वरकों, रासायनिक उर्वरकों और जैविक उर्वरकों का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। आप किसी भी सड़ी हुई FYM (खेत की खाद) का उपयोग भी कर सकते हैं। ● गाय का गोबर ● उद्यान खाद ● वर्मिन-कम्पोस्ट ● हरी पत्तियों से बनी खाद @ सिंचाई चंदन के पौधों की खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। गर्मियों के दौरान युवा चंदन के पौधों को 2 से 3 सप्ताह में एक बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, उन्हें बारिश की स्थिति में सिंचाई की आवश्यकता नहीं हो सकती है। @ होस्ट पेड की छटनी यदि मेजबान प्रजाति चंदन के पेड़ पर छाया देना शुरू कर देती है, तो आपको इसे वापस छटनी करने की आवश्यकता होगी। अन्यथा, चंदन के पेड़ को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलेगा। मेजबान प्रजातियों की छटनी करें ताकि यह चंदन के पौधे की तुलना में थोड़ा छोटा हो, ताकि चंदन को पर्याप्त धूप मिले। @ फसल सुरक्षा चंदन की खेती करने में , पहले साल में सबसे अधिक देखभाल की आवश्कता होती है । पहले साल में चंदन के पौधे पर रोगो का अटेक नही होने देना चाहिए । चंदन के पौधे में सबसे ज्यादा फंगस की बीमारी का असर होता हैं इसलिए चंदन को लगाने से लेकर तीन साल तक उसमें फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। फंगीसाइड में आप बावस्टिंन, सीओसी , थाईफेनेट ,मिथाईल आदि फंगी साइड दवाईयों का स्प्रे करते रहना चाहिए। * कीट 1. वुड-बोरर यह चंदन की लकड़ी को खाने वाला एक कीड़ा होता हैं जिसे वुड बोरर कहते हैं इसकी रोकथाम के लिए क्लोराफाइरीफास दवाई की ड्रिचिंग व गेरू के साथ लेप कर देना चाहिए जिससे कीड़ा तने के उपर न चढ़ सके और पौधे को नुकसान न पहुचाये। 2. दीमक दीमक ऐसा कीड़ा है जो शुरुआत में जड़ो से उपर की ओर जाता है बाद में छाल को खा जाती हैं। इसलिए पहले से ही जिस मिट्टी में ज्यादा दीमक हो तो बोडोपेस्ट के साथ क्लोरोपायरीफास मिक्स करके बार-बार लगाये| 3. मिलीबग मिलीबग भी चंदनके लिए बहुत हानिकारक साबित होती है ,उसकी रोकथाम के लिए डेन्टासु दवाई का स्प्रे या ड्रिंन्चिंग करते रहना चाहिए फिर स्टम्प में नीचे की ओर टेपिंग लपेट देना चाहिए। @ कटाई जब चंदन का पेड़ आठ साल का हो जाता है, तो पेड़ की दृढ़ लकड़ी बनने लगती है और रोपण से 12 से 15 साल बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। चंदन की रसदार लकड़ी (हार्ड वुड ) और सुखी लकड़ी दोनो का मूल्यांकन अलग-अलग होता है। जड़े भी सुंगधित होती है इसलिए चंदन के वृक्ष को जड़ से उखाड़ा जाता है न की काटा जाता हैं। @ उपज एक एकड़ जमीन से आप 5000 किलो चंदन की उपज होती हैं।
Cassava Farming - कसावा की खेती.....!
कसावा उष्ण कटिबंध में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण स्टार्च वाली जड़ वाली फसल है और मुख्य रूप से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में इसकी खेती की जाती है। पुर्तगाली द्वारा सत्रहवीं शताब्दी के दौरान पेश की गई, केरल में कम आय वर्ग के लोगों के बीच भोजन की कमी को दूर करने के लिए फसल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमिगत कंद स्टार्च से भरपूर होता है और मुख्य रूप से पकाने के बाद खाया जाता है। टैपिओका से बने चिप्स, साबूदाना और सेंवई जैसे प्रोसेस्ड उत्पाद भी देश में लोकप्रिय हैं। आसानी से पचने योग्य होने के कारण, यह कुक्कुट और पशु-चारे में एक महत्वपूर्ण घटक बनाता है। यह औद्योगिक शराब, स्टार्च और ग्लूकोज के उत्पादन के लिए भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। @ जलवायु कसावा आम तौर पर उष्णकटिबंधीय तराई में उगाया जाता है और परिपक्व होने के लिए कम से कम 8 महीने के गर्म मौसम की आवश्यकता होती है।यह पूर्ण सूर्यप्रकाश को पसंद करता है। कसावा भूमध्य रेखा के पास सभी क्षेत्रों में 1,500 मीटर से कम ऊंचाई पर, 1,000 से 1,500 मिमी/वर्ष के बीच वर्षा और 23 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में बेहतर होता है। कसावा ठंढ को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए यह ग्रीनहाउस में या कूलर क्षेत्रों में ठंडे फ्रेम संरक्षण के साथ सबसे अच्छा बढ़ता है। @ मिट्टी कसावा की खेती के लिए अच्छी जलनिकासी वाली कोई भी मिट्टी अधिमानतः 5.5 -7.0 की पीएच रेंज वाली लाल लैटेरिटिक दोमट, अच्छी बनावट की हल्की, गहरी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कसावा उगाने के लिए रेतीली और चिकनी मिट्टी कम उपयुक्त होती है। @ खेत की तैयारी अच्छी जुताई के लिए खेत की 4-5 बार जुताई करें। मिट्टी की गहराई कम से कम 30 से.मी. होनी चाहिए और मेड़ और खांचे बनाना चाहिए। हाथ से खेती करने के लिए, जमीन को साफ करें और मिट्टी खोदें। भारी मिट्टी के लिए कोई भी टीला या लकीरें खींची जाती हैं। भारी मिट्टी के लिए यंत्रीकृत खेती, जाइरो-मल्चिंग, जुताई और रिजिंग की जाती है। @ प्रसार कसावा का पौधा तुरंत ही काटे गए पौधों के तनों से कटिंग से बढ़ता है। @ बीज * बीज दर एक हेक्टेयर रोपण के लिए 17,000 कटिंग्स की आवश्यकता होती है। कटिंग को जल्द से जल्द लगाया जाता है, हालांकि उन्हें 3 महीने तक ठंडे, छायांकित स्थान पर सफलतापूर्वक संग्रहीत किया जा सकता है।रोपण सामग्री लेने के लिए स्वस्थ मोज़ेक मुक्त पौधों का चयन करें।तने के मध्य भाग से 8-10 गांठों के साथ 15 सेंटीमीटर लंबे सेट तैयार करें। सेट तैयार करने और संभालने के दौरान यांत्रिक क्षति से बचें। कट एंड एक समान होना चाहिए। * बीज उपचार बुवाई से पहले 15 मिनट के लिए सेट्स को कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम/ एक लीटर पानी में डुबोएं। कलियों को मेड़ों और खांचों के किनारों पर ऊपर की ओर इंगित करते हुए लंबवत रोपें। बारानी परिस्थितियों के लिए, सेट को पोटैशियम क्लोराइड @ 5 ग्राम/लीटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे ZnSO4 और FeSO4 प्रत्येक @ 0.5% की दर से 20 मिनट के लिए उपचारित करें। एज़ोस्पाइरिलम और फॉस्फोबैक्टीरिया में से प्रत्येक को 30 ग्राम/ली की दर से 20 मिनट के लिए डुबोएं। @ बुवाई *रिक्ति सिंचित: 75 x 75 सेमी (17,777 सेट) और 90 x 90 सेमी (12,345 सेट) बारानी: 60 x 60 सेमी (27,777 सेट्स) कन्याकुमारी परिस्थितियों में: 90 x 90 सेमी (12,345 सेट) * बुवाई विधि कटिंग के निचले आधे हिस्से को हर 3 फीट की पंक्तियों में लगाया जाता है जो 3 फीट अलग होते हैं। यदि मिट्टी सूखी है, तो कटिंग को 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। यदि मिट्टी गीली है, तो वे लंबवत रूप से लगाए जाते हैं। @ उर्वरक * सिंचित फसल जुताई के समय 25 टन/हेक्टेयर गोबर की खाद डालें। 45:90:120 किग्रा NPK/हेक्टेयर बेसल के रूप में और 45:120 किग्रा NK/हेक्टेयर रोपण के 90 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने के दौरान डाले। *वर्षा आधारित फसल 12.5 t/ha FYM के साथ 50 kg N, 65 kg P और 125 kg K/ha बेसल के रूप में दिया जाता है। वर्षा होने पर रोपण के 30-60 दिनों के बाद मिट्टी में 2 किग्रा एजाटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है (2.0 किग्रा एजाटोबैक्टर + 20 किग्रा एफवाईएम + 20 किग्रा मिट्टी प्रति हेक्टेयर)। @ सिंचाई पहली सिंचाई रोपाई के समय की जाती है। अगली सिंचाई तीसरे दिन और उसके बाद तीसरे महीने तक 7-10 दिनों में एक बार और 8वें महीने तक 20-30 दिनों में एक बार करें। @ इंटरकल्चर ऑपरेशन रोपण के 20 दिनों के भीतर अंतरालों को भर दें। रोपण के 20 दिन बाद पहली निराई-गुड़ाई करें। बाद में खरपतवार की तीव्रता के आधार पर 5 महीने तक एक महीने में एक बार निराई करनी चाहिए। 60वें दिन प्रति पौधा दो अंकुर तक पतले कर दे। प्याज, धनिया, कम अवधि की दालें और कम अवधि की सब्जियां, रोपण की तारीख से लेकर 60 दिनों तक की अंतर-फसल के रूप में उगाएं। @ फसल सुरक्षा *कीट 1.माइट्स तीसरे और पांचवें महीने के दौरान डायकोफोल 18.5 ईसी 2.5 मिली/लीटर का छिड़काव करके माइट्स को नियंत्रित किया जा सकता है। 2. सफेद मक्खी (बेमिसिया तबसी) वैकल्पिक खरपतवार धारक जैसे अबुटिलोन इंडिकम को हटा दें। पीला चिपचिपा ट्रैप 12 संख्या/हेक्टेयर में स्थापित करें। नाइट्रोजन का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करें। अत्यधिक सिंचाई से बचें। नीम का तेल 3% या फिश ऑयल रोसिन साबुन 25 ग्राम/लीटर या मिथाइल डेमेटॉन 25 ईसी 2 मिली/लीटर का छिड़काव करें। नीम के तेल का उपयोग करते समय, पर्ण के साथ बेहतर संपर्क के लिए टीपोल को 1 मिली/लीटर की दर से मिलाया जाना चाहिए। मिथाइल डेमेटॉन को प्रारंभिक अवस्था में और फोसालोन को फसल के विकास के बाद के चरणों में लगाएं। सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड्स के उपयोग से बचें। फसल वृद्धि को उसकी अवधि से आगे बढ़ाने से बचें। 3. सर्पिलिंग सफेद मक्खी प्रतिरोधी जीनोटाइप विकसित करें। स्टिकी कम लाइट ट्रैप लगाएं और वयस्कों को आकर्षित करने के लिए सुबह 4 से 6 बजे के बीच काम करें। डिक्लोरवोस 76 WSC @ 1 मिली/लीटर या ट्रायज़ोफॉस 40 EC 2 मिली/लीटर का छिड़काव करें। गीला एजेंट जोड़ें। एनकार्सिया हैटेंसिस, ई. गुआदेलूपे परजीवियों का संरक्षण करें। * रोग 1. मोज़ेक रोपण सामग्री का चयन स्वस्थ पौधों से करें। सफेद मक्खी रोगवाहकों के नियंत्रण के लिए आईपीएम प्रथाओं को अपनाएं। 2. सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट को 15 दिनों के अंतराल पर दो बार मैनकोजेब 2 ग्राम/लीटर के छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। 3. कंद सड़ांध जलभराव से बचें। जल निकासी की अच्छी सुविधा दें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम / लीटर के साथ स्पॉट ड्रेंचिंग या मिट्टी के माध्यम से ट्राइकोडर्मा विराइड @ 2.5 किग्रा / हेक्टेयर बेसल के रूप में और रोपण के बाद तीसरे और छठे महीने में लागू करें। 4. आयरन की कमी कमी के लक्षण दिखाई देने पर फेरस सल्फेट 2.5 ग्राम प्रति लीटर की 3 से 4 बार साप्ताहिक अंतराल पर छिड़काव करें। विलयन को तटस्थ करने के लिए समान मात्रा में चूना मिलाना चाहिए। @ कटाई फसल बोने के 9 से 11 महीने बाद काटी जा सकती है। कंद की परिपक्वता के दौरान पत्तियां पीली हो जाती हैं और 50% पत्तियां सूखकर झड़ जाती हैं। तने के आधार के पास की मिट्टी में दरार दिखाई देती है। कन्दों को कांटे या कौबार से उखाड़ा जा सकता है। @ उपज सिंचित : 40 - 50 टन/हेक्टेयर बारानी : 20 - 25 टन/हेक्टेयर
Peanut Farming - मूंगफली की खेती ......!
मूंगफली विश्व का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तिलहन है, जो देश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खेती के लिए आदर्श है। भारत में यह साल भर उपलब्ध रहता है। यह प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है जो ज्यादातर वर्षा-सिंचित परिस्थितियों में उगाया जाता है। गुठली को कच्चा, भूनकर या मीठा करके भी खाया जाता है। वे प्रोटीन और विटामिन ए, बी और बी 2 समूह से भरपूर होते हैं। मूंगफली का प्रमुख उपयोग साबुन बनाने, सौंदर्य प्रसाधन, स्नेहक उद्योगों आदि में पाया जाता है। मूंगफली की खली का उपयोग कृत्रिम रेशों के निर्माण में किया जाता है। मूंगफली के खोल का उपयोग मोटे बोर्ड, कॉर्क के विकल्प आदि के निर्माण के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। पतवारों को पशुओं को (हरा, सुखाया या साइलेज्ड) खिलाया जाता है। मूंगफली एक रोटेशन फसल के रूप में भी महत्वपूर्ण है। भारत में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य हैं। @जलवायु अच्छे अंकुरण और वृद्धि के लिए क्षेत्र का तापमान लगभग 20 -30˚C होना चाहिए। फसलों के लिए आवश्यक न्यूनतम वार्षिक वर्षा 450 से 1250 मिमी के बीच है। मूंगफली की खेती के लिए अधिक ऊंचाई, ठंड और पाला उपयुक्त नहीं है। मूंगफली की खेती के लिए विशेष रूप से लंबी गर्म जलवायु अच्छी होती है। @मिट्टी मूंगफली के पौधों को बेहतर प्रदर्शन के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी गहरी होनी चाहिए और उच्च उर्वरता सूचकांक के साथ मिट्टी का पीएच लगभग 5.5 -7 होना चाहिए। कटाई में कठिनाई और फली के नुकसान के कारण भारी मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त है। मिट्टी प्रकृति में खारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये फसलें नमक के प्रति संवेदनशील होती हैं। मूंगफली की खेती के लिए मिट्टी में पत्थर और चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए अन्यथा उपज प्रभावित होगी। @ खेत की तैयारी पिछली फसल के सभी अवशेषों और खरपतवार को हटा देना चाहिए और पहली जुताई 15-20 सेमी की गहराई तक करनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी की अच्छी भुरभुरापन प्राप्त करने के लिए डिस्क हैरोइंग के 2-4 चक्र लगाने चाहिए।खरीफ की फसल के लिए, मई-जून में बारिश की शुरुआत के साथ, खेत को दो जुताई दी जाती है और अच्छी जुताई प्राप्त करने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर दिया जाता है। खेती के लिए हैरो या टिलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि खेत सफेद सूंडी से संक्रमित है, तो हेप्टाक्लोर या क्लोर्डेन जैसे रसायनों को अंतिम हैरो करने से पहले 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ड्रिल किया जाता है। सिंचित फसल के लिए, भूमि की स्थलाकृति, सिंचाई स्रोत की प्रकृति और पानी उठाने की विधि के आधार पर सुविधाजनक आकार की क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। @बीज *बीज दर बिजाई के लिए 38-40 किलो बीज प्रति एकड़ में प्रयोग करें। *बीज उपचार बुवाई के लिए स्वस्थ और अच्छी तरह से विकसित गुठली का उपयोग करें। बहुत छोटी, सिकुड़ी हुई और रोगग्रस्त गुठली को त्याग दें। बीजों को थीरम 5 ग्राम या कैप्टान 2-3 ग्राम प्रति किलो या मैनकोज़ेब 4 ग्राम प्रति किलो या कार्बोक्सिन या कार्बेनडाज़िम 2 ग्राम प्रति किलो गिरी से उपचारित करें ताकि जमीन में पैदा होने वाली बीमारी से बचा जा सके। रासायनिक उपचार के बाद ट्राइकोडर्मा विराइड 4 ग्राम प्रति किलो बीज या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 10 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। बीज उपचार युवा पौध को जड़ सड़न और कॉलर सड़न संक्रमण से बचाएगा। @बुवाई *बुवाई का समय मूंगफली ज्यादातर वर्षा आधारित खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है, जिसे मानसून की बारिश के आधार पर मई से जून तक बोया जाता है। इसे अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में बोया जाता है। एक सिंचित फसल के रूप में यह जनवरी और मार्च के बीच और मई और जुलाई के बीच सीमित मात्रा में उगाई जाती है। * रिक्ति अपनाई जाने वाली दूरी किस्म के प्रकार पर निर्भर करती है। यानी, अर्ध फैलने वाली किस्मों के लिए पंक्तियों के बीच 30 सेमी और पौधों के बीच 22.5 सेमी की दूरी का उपयोग करें और गुच्छेदार प्रकार की किस्मों के लिए पंक्तियों के बीच 30 सेमी और पौधों के बीच 15 सेमी की दूरी का उपयोग करें। *बुवाई की गहराई बीज को सीड ड्रिल की मदद से 8-10 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। *बुवाई की विधि सीड ड्रिल की मदद से बीज बोए जाते हैं। *बुवाई प्रणाली मूंगफली की बुवाई के लिए तीन प्रणालियाँ विकसित की गई हैं; समतल सतह प्रणाली, चौड़ी क्यारी-खाड़ी प्रणाली और रिज-कुंड प्रणाली। @उर्वरक बारानी फसल के लिए अनुशंसित उर्वरक 6.25 टन गोबर की खाद और 10-25 किग्रा नाइट्रोजन (N), 20-40 किग्रा फास्फोरस (P2O5) और 20-40 किग्रा पोटाश (K2O) प्रति हेक्टेयर है। सिंचित फसल के लिए 12.5 टन गोबर की खाद और 20-40 किग्रा नाइट्रोजन (N), 40-90 किग्रा फास्फोरस (P2O5) और 20-40 किग्रा पोटाश (K2O) प्रति हेक्टेयर है। नाइट्रोजन (एन) का प्रयोग दो बराबर मात्रा में करें, एक बुवाई से पहले और दूसरा बुवाई के 30 दिन बाद। बीज उपचार के रूप में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग गांठों को बढ़ाने और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लाभदायक होता है। पेगिंग अवस्था में 500 किग्रा जिप्सम प्रति हेक्टेयर के प्रयोग से फली बनने में वृद्धि होगी। @सिंचाई अच्छी फसल वृद्धि के लिए मौसमी वर्षा के आधार पर दो या तीन बार सिंचाई आवश्यक है। पहली सिंचाई फूल आने की अवस्था में करें। यदि खरीफ की फसल सूखे की लंबी अवधि में पकड़ी जाती है, विशेष रूप से फली बनने की अवस्था में, पूरक सिंचाई दी जाती है, यदि पानी उपलब्ध हो (फली विकास अवस्था में, मिट्टी के प्रकार के आधार पर 2 - 3 सिंचाइयां दी जाती हैं)। सिंचाई के बीच का अंतराल 8-12 दिनों का होता है। फलियों को मिट्टी से पूरी तरह से निकालने के लिए कटाई से कुछ दिन पहले एक और सिंचाई दी जा सकती है। @ इंटरकल्चर ऑपरेशंस खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए और मिट्टी को भुरभुरी स्थिति में रखने के लिए, फसल को आम तौर पर एक हाथ से निराई और एक या दो गोड़ाई, बैल से चलने वाले औजारों के साथ, पहली गुड़ाई बुवाई के लगभग तीन सप्ताह बाद, दूसरी गुड़ाई लगभग एक पखवाड़े के बाद और तीसरी गुड़ाई लगभग एक महीने बाद करनी चाहिए। पेग्स के भूमिगत होने के बाद कोई इंटरकल्चर नहीं करना चाहिए। मिट्टी में पेग्स के अधिकतम प्रवेश की सुविधा के लिए बंच और अर्ध-फैलने वाले प्रकारों के मामले में मिट्टी चढ़ाना किया जा सकता है। बुवाई के 40-45 दिनों के भीतर मिट्टी चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मिट्टी में पेग्स के प्रवेश में मदद करता है और फली के विकास में भी मदद करता है। @खरपतवार नियंत्रण मूंगफली की बुवाई के दो दिनों के भीतर खरपतवारों को 500 लीटर पानी में 5 लीटर लेस्सो या टोक-ई-25 वीडीसाइड प्रति हेक्टर से भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। फ्लुकोरालिन @ 600 मिली प्रति एकड़ या पेंडीमेथालिन @ 1 लीटर प्रति एकड़ पूर्व-उभरने वाले क्षेत्र के रूप में डालें और रोपण के 36-40 दिनों के बाद एक बार हाथ से निराई करें। @फसल सुरक्षा *पीड़क 1. एफिड वर्षा कम होने पर इसका प्रकोप अधिक होता है। ये काले शरीर वाले छोटे कीट होते हैं जो पौधों का रस चूसते हैं जिससे पौधे बौने और पीले हो जाते हैं। वे पौधे पर एक चिपचिपा द्रव (हनीड्यू) का स्राव करते हैं, जो एक कवक द्वारा काला हो जाता है। जैसे ही लक्षण दिखाई दें, रोगर @ 300 मिली/एकड़ या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल @ 80 मिली/एकड़ या मिथाइल डेमेटॉन 25% ईसी @ 300 मिली/एकड़ का छिड़काव करे, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। 2. सफेद ग्रब्स वयस्क भृंग जून-जुलाई के दौरान बारिश की पहली फुहारों के साथ मिट्टी से निकलते हैं। वे पास के पेड़ों जैसे बेर, अमरूद, रुक्मंजनी, अंगूर की बेल, बादाम आदि पर इकट्ठा होते हैं और रात के समय उनके पत्तों को खाते हैं। अंडे मिट्टी में देते हैं और उनसे निकलने वाले लार्वा (ग्रब) मूंगफली के पौधों की जड़ों या जड़ के बालों को खा जाते हैं। सफेद ग्रब्स के प्रभावी प्रबंधन के लिए मई-जून में खेत की दो बार जुताई करें। यह मिट्टी में आराम करने वाले भृंगों को उजागर करता है। फसल बोने में देरी न करें। बिजाई से पहले बीज को क्लोरपाइरीफॉस 20 ई सी 12.5 मिली प्रति किलो गिरी से उपचारित करें। भृंग नियंत्रण के लिए कार्बेरिल 900 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। प्रत्येक वर्षा के बाद जुलाई के मध्य तक छिड़काव दोहराया जाना चाहिए। फोरेट @ 4 किग्रा या कार्बोफ्यूरान @ 13 किग्रा प्रति एकड़ बुवाई से पहले मिट्टी में डालें। 3. बालों वाली कैटरपिलर कैटरपिलर बड़े पैमाने पर होते हैं और उपज को कम करते हुए फसल को ख़राब करते हैं। लार्वा लाल भूरे रंग के काले बैंड और पूरे शरीर पर लाल रंग के बाल होते हैं। बारिश होने के तुरंत बाद 3-4 लाइट ट्रैप लगाएं। काटे गए क्षेत्र में अण्डों के समूहों को एकत्र कर नष्ट कर दें। संक्रमित खेतों के चारों ओर लंबवत किनारों के साथ 30 सेमी गहरी और 25 सेमी चौड़ी खाई खोदकर लार्वा के प्रवास से बचें। ज़हरीले चारे के छोटे-छोटे गोले शाम के समय खेत में बाँट दें।जहरीला चारा तैयार करने के लिए 10 किलो चावल की भूसी, 1 किलो गुड़ और एक लीटर क्विनालफॉस मिलाएं। छोटे लार्वा को नियंत्रित करने के लिए कार्बेरिल या क्विनालफॉस की 300 मिली/एकड़ की दर से झाड़न करें। बड़े इल्ली को नियंत्रित करने के लिए, 200 मिलीलीटर डाइक्लोरवोस 100 ईसी @ 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। 4. मूंगफली की पत्ती माइनर युवा लार्वा पत्तियों में घुस जाते हैं और पत्तियों पर छोटे बैंगनी धब्बे बनाते हैं। बाद के चरणों में लार्वा पत्रक को आपस में जोड़ लेते हैं और उन पर फ़ीड करते हैं, सिलवटों के भीतर रहते हैं। गंभीर रूप से प्रभावित खेत "जला हुआ" दिखता है। लाइट ट्रैप @ 5/एकड़ लगाएं। डाईमेथोएट 30EC @ 300 मिली/एकड़ या मैलाथियान 50 EC @ 400 मिली/एकड़ या मिथाइल डेमेटॉन 25% EC @ 200 मिली/एकड़ डालें। 5. दीमक दीमक घुसकर जड़ और तने को खोखला कर देते हैं और इस प्रकार पौधे को मार देते हैं। फलियों में छेद करते है और बीजों को नुकसान पहुंचाते है। दीमक के प्रकोप के कारण पौधे का मुरझाना देखा जाता है। अच्छी तरह से सड़ी हुई गाय के गोबर का प्रयोग करें। फसल की कटाई में देरी न करें। क्लोरपाइरीफॉस @ 6.5 मि.ली./किग्रा बीज से बीज उपचार करने से दीमक से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। स्थानिक क्षेत्रों में बुवाई से पहले क्लोरपाइरीफॉस 2 लीटर प्रति एकड़ मिट्टी में डालें। 6.फली छेदक छोटे पौधों में छेद देखे जाते हैं। निम्फ प्रारंभिक अवस्था में सफेद रंग का होता है और बाद में भूरे रंग का हो जाता है। मैलाथियान 5D10 किग्रा/एकड़ या कार्बोफ्युरान 3%CG13 किग्रा/एकड़ की दर से संक्रमित क्षेत्र में बिजाई से 40 दिन पहले मिट्टी में डालें। *रोग 1. टिक्का या सरकोस्पोरा लीफ-स्पॉट: पत्तियों के ऊपरी तरफ एक हल्के पीले रंग की अंगूठी से घिरा परिगलित गोलाकार स्थान बन जाता है। रोग को नियंत्रित करने के लिए शुरुआत से लेकर बीजों के चयन तक का ध्यान रखें। स्वस्थ और बेदाग गुठली चुनें। बिजाई से पहले थीरम (75%) 5 ग्राम या इंडोफिल एम-45 (75%) 3 ग्राम गिरी से प्रति किलो बीज उपचार करें। फसल पर वेटेबल सल्फर 50 WP @ 500-750 ग्राम/200-300 लीटर पानी प्रति एकड़ में स्प्रे करें। अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू करते हुए पखवाड़े के अंतराल पर 3 या 4 छिड़काव करें। वैकल्पिक रूप से, सिंचित फसल पर कार्बेन्डाजिम (बाविस्टिन/डेरोसल/एग्रोज़िम 50 डब्ल्यूपी 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर) प्रति एकड़ में स्प्रे करें। फसल के 40 दिन के होने से शुरू करते हुए पखवाड़े के अंतराल पर तीन स्प्रे करें। 2. कॉलर-सड़ांध और बीज सड़ांध ये रोग एस्परगिलस नाइजर के कारण होते हैं। इससे हाइपोकोटिल क्षेत्र जड़ से नष्ट हो जाता है, पौधे मुरझा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। नियंत्रण हेतु बीजोपचार आवश्यक है। बीज को थीरम या कैप्टान 3 ग्राम/किग्रा बीज से उपचारित करें। 3. अल्टरनेरिया पत्ती रोग इसकी विशेषता पत्तियों के शीर्ष भाग का झुलसना है जो हल्के से गहरे भूरे रंग में बदल जाता है। संक्रमण के बाद के चरणों में, झुलसी हुई पत्तियाँ अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और भंगुर हो जाती हैं। ए. अल्टरनेटा द्वारा उत्पन्न घाव छोटे, हरितहीन, पानी से लथपथ होते हैं, जो पत्ती की सतह पर फैल जाते हैं। यदि प्रकोप दिखे तो मैंकोज़ेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति एकड़ या कार्बेन्डाजिम 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ पत्तियों पर डालें। 3. जंग फुंसी सबसे पहले पत्ती की निचली सतह पर दिखाई देती है। वे फूल और खूंटियों के अलावा सभी हवाई पौधों के हिस्सों पर बन सकते हैं। गंभीर रूप से संक्रमित पत्तियां परिगलित हो जाती हैं और सूख जाती हैं लेकिन पौधे से जुड़ी रहती हैं। संक्रमण दिखाई देने पर मैंकोजेब 400 ग्राम प्रति एकड़ या क्लोरोथालोनिल 400 ग्राम प्रति एकड़ या वेटटेबल सल्फर 1000 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करें। यदि आवश्यक हो तो 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। @ कमी 1. पोटैशियम की कमी पत्तियां ठीक से विकसित नहीं हो रही हैं और अनियमित आकार में बढ़ती हैं। परिपक्व पत्तियाँ हल्के पीले रंग की दिखाई देती हैं और नसें हरी रहती हैं। कमी को दूर करने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश 16-20 किलोग्राम/एकड़ की दर से डालें। 2. कैल्शियम की कमी अधिकतर हल्की मिट्टी या क्षारीय मिट्टी में देखा जाता है। पौधे ठीक से विकसित नहीं हो पाते। पत्तियां मुड़ती हुई दिखाई देती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए खूंटी बनने की अवस्था में 200 किलोग्राम प्रति एकड़ जिप्सम डालें। 3. आयरन की कमी पूरी पत्ती सफेद या हरितहीन हो जाती है। यदि कमी दिखाई देती है, तो फसल पर एक सप्ताह के अंतराल पर फेरस सल्फेट 5 ग्राम + साइट्रिक एसिड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। कमी दूर होने तक छिड़काव जारी रखें। 4. जिंक की कमी प्रभावित पौधे में पत्तियां गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं, पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है और छोटी दिखाई देती हैं। जिंक सल्फेट 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 7 दिन के अंतराल पर दो-तीन बार छिड़काव करें। 5. सल्फर की कमी युवा पौधों की वृद्धि रुक जाती है और आकार में छोटे दिखाई देने लगते हैं। साथ ही पत्तियां छोटी और पीली दिखाई देती हैं। पौधे की परिपक्वता में देरी होती है. निवारक उपाय के रूप में रोपण और स्टैग लगाने पर जिप्सम 200 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। @ कटाई खरीफ की बोई गई फसल नवंबर माह में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जब पौधे में पुरानी पत्तियों के झड़ने के साथ-साथ फसल का एक समान पीलापन दिखाई देता है। अप्रैल के अंत-मई के अंत में बोई गई फसल अगस्त और सितंबर के अंत में मानसून खत्म होने के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। फसल की कुशल कटाई के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद होनी चाहिए और फसल अधिक पकी नहीं होनी चाहिए। @ उपज औसतन लगभग 1500-2500 किग्रा/एकड़ मूंगफली का उत्पादन होता है।
Sufflower Farming - कुसुम की खेती!
कुसुम को आमतौर पर "खुसंभा, कुसुम" के नाम से जाना जाता है। कुसुम का उत्पादन शुरू में इसके फूलों के लिए किया गया था, जिसका उपयोग कपड़ों और भोजन को रंगने के लिए किया जाता था। हालाँकि, अब कुसुम की खेती मुख्यत: तेल के लिए की जाती है, कुसुम के बीजों में 24-36 प्रतिशत तेल पाया जाता है। कुसुम तेल में लगभग 75% लिनोलिक एसिड होता है, जो मकई, सोयाबीन, बिनौला, मूंगफली या जैतून के तेल से अधिक है। इस कुसुम का उपयोग सलाद तेल और नरम मार्जरीन बनाने के लिए किया जाता है। उच्च ओलिक एसिड किस्मों का उपयोग आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज़ को तलने के लिए किया जा सकता है। कपड़े व खाने के रंगों में कुसुम का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में कृत्रिम रंगों का स्थान, कुसुम से तैयार रंग के द्वारा ले लिया गया है। यह तेल खाना-पकाने व प्रकाश के लिए जलाने के काम आता है। यह साबुन, पेंट, वार्निश, लिनोलियम तथा इनसे संबंधित पदार्थों को तैयार करने के काम में भी आता है। इसके तेल से तैयार पेंट व वार्निश में स्थायी चमक व सफदी होती है। कुसुम के तेल का प्रयोग विभिन्न दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। तेल निकालने के बाद बचा हुआ भोजन प्रोटीन स्रोत के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। भोजन में आम तौर पर 24% प्रोटीन और बहुत सारा फाइबर होता है। सजावटी भोजन (ज्यादातर छिलके हटा दिए गए) में कम फाइबर के साथ 40% प्रोटीन होता है। इसके डिकोट केक का उपयोग मवेशियों को खिलाने के लिए किया जाता है। भारत में कुसुम की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश व गुजरात आदि हैं। @ जलवायु कुसुम की खेती ठंडी एवं शुष्क जलवायु की फसल है। यह सूखा प्रतिरोधी फसल है। इसके अंकुरण के लिये उपयुक्त तापक्रम लगभग 15 - 20°C है तथा पौधों की वृद्धि एवं बढ़वार के समय लगभग 24-28°C तापमान उचित रहता है। इसे लगभग 1000 मिमी वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है। उच्च आर्द्रता और वर्षा से कवक रोगों से क्षति बढ़ जाती है। @ मिट्टी कुसुम की फसल विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाई जाती है। कुसुम उत्कृष्ट जल-धारण क्षमता और संग्रहित नमी के साथ गहरी, उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पर पनपता है। अच्छे उत्पादन के लिये कुसुम फसल के लिये बलुई दोमट, कार्बनिक पदार्थ से भरपूर, मध्यम काली से लेकर भारी काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसे हल्की जलोढ़ और दोमट मिट्टी में सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है। इसे मुख्य रूप से असिंचित फसल के रूप में काली कपास मिट्टी में उगाया जाता है। भूमि का pH मान 6.5 से 8 के बीच उपयुक्त रहता है। @ खेत की तैयारी कुसुम के लिए 3 वर्षों में एक गहरी जुताई और उसके बाद 2 से 3 जुताई की आवश्यकता होती है। जुताई के बीच-बीच में ढेले तोड़ें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें।प्रत्येक जुताई या हैरो के पश्चात् भूमि में नमी संरक्षण हेतु पाटा लगाना आवश्यक होता है। 5 से 10 टन FYM/हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिलाया जाता है। @ बीज *बीज दर बुआई के लिए बीज की मात्रा 6 किग्रा बीज /एकड़ या 15-20 किग्रा/ हैक्टेयर पर्याप्त रहती है। *बीज उपचार बुआई से पहले बीजों को कैप्टान या एग्रोसन जीएन या थीरम या मैंकोजेब 3 ग्राम/किग्रा बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बेहतर अंकुरण के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त बीजों को रात भर पानी में भिगोना चाहिए। @ बुवाई *बुवाई का समय बीज बोने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवम्बर का प्रथम सप्ताह है। * रिक्ति पौधे से पौधे की दूरी 15 सेमी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेमी रखें। 45 X 20 सेमी (वर्षा आधारित)। 60 X 30 सेमी (सिंचित)। *बुवाई की गहराई बीज 5-7 सेमी की गहराई पर बोयें। *बुवाई की विधि बुवाई ड्रिलिंग विधि से की जाती है। @ उर्वरक आखिरी जुताई के समय 5 से 10 टन FYM/हेक्टेयर मिट्टी में मिलाया जाता है। उर्वरक की मात्रा है: वर्षा आधारित कुसुम: 25 किग्रा एन/हेक्टेयर। सिंचित कुसुम: 50 किग्रा एन, 25 किग्रा पी2ओ5/हेक्टेयर। वर्षा आधारित फसल में उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय करना चाहिए। सिंचित फसल के मामले में, N की आधी खुराक और P की पूरी खुराक बुआई के समय और N की शेष आधी खुराक बुआई के 30 दिन बाद डालनी चाहिए। @ सिंचाई कुसुम एक सूखा-प्रतिरोधी फसल है, इसलिए इसे आम तौर पर संग्रहित नमी पर वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है। उस क्षेत्र के लिए जहां मिट्टी कम नम है, बुआई से पहले एक भारी सिंचाई करें, यह बेहतर विकास के लिए फायदेमंद होगा।सिंचित फसल के रूप में पहली सिंचाई बुआई से पहले की जाती है। अन्य सिंचाई फूल आने और दाना भरने की अवस्था में, 35 से 40 दिन और बुआई के 65 से 70 दिन बाद करनी चाहिए। @ फसल सुरक्षा * कीट 1. हरा आड़ू एफिड इसका स्वरूप पौधे पर जले हुए जैसा होता है। 2. कुसुम एफिड ये कोमल टहनियों, पत्तियों के साथ-साथ तने पर भी दिखाई देते हैं, इससे पौधा कमजोर दिखता है और कुछ क्षेत्र सूख जाते हैं। नियंत्रण: 100 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस 20EC को 100 लीटर पानी में प्रति एकड़ मिलाकर छिड़काव करें। यदि आवश्यक हो तो 15 दिन बाद भी दोहराया जा सकता है। * रोग 1. मुरझाना और गर्मी से सड़न इसमें पौधा पीला होकर बाद में भूरा हो जाता है और अंत में मर जाता है। स्क्लेरोटिक कवक प्रकार के होते हैं जो मुकुट, निकटवर्ती जड़ क्षेत्रों और तने पर देखे जाते हैं। नियंत्रणः स्वस्थ एवं रोगमुक्त बीजों का प्रयोग करें। बरसात के मौसम में तने के आसपास मिट्टी का ढेर नहीं लगाना चाहिए। @ कटाई कुसुम 150-180 दिनों में पक जाता है। कुसुम कटाई के लिए तब तैयार होता है जब अधिकांश पत्तियाँ भूरे रंग की हो जाती हैं और नवीनतम फूल वाले सिरों की शाखाएँ बमुश्किल हरी होती हैं। @ उपज असिंचित क्षेत्रों में कुसुम फसल की उपज 10-12 क्विटल/हैक्टेयर होती है, व सिंचित क्षेत्रों में 14-18 क्विटल/हैक्टेयर तक उपज प्राप्त हो जाती है। मिश्रित फसल: 125 किग्रा/हेक्टेयर। एकमात्र फसल: 500 से 800 किग्रा/हेक्टेयर। डाई का उद्देश्य: 100 से 150 किलोग्राम सूखी पंखुड़ियाँ/हेक्टेयर।
Sunflower Farming - सूरजमुखी की खेती ..!
सूरजमुखी भारत में ख़रीफ़ सीज़न में उगने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। यह मुख्य रूप से इसके तेल के लिए उगाया जाता है। सूरजमुखी का तेल अपने हल्के रंग, हल्के स्वाद, उच्च धूम्रपान बिंदु और लिनोलिक एसिड के उच्च स्तर के कारण सबसे लोकप्रिय है जो हृदय रोगियों के लिए अच्छा है। बीजों को सुखाकर, भूनकर या अखरोट के मक्खन में पीसकर खाया जा सकता है। सूरजमुखी के बीज में लगभग 48-53 प्रतिशत खाद्य तेल होता है। तेल का उपयोग वनस्पति की तैयारी और साबुन और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। इसका केक प्रोटीन से भरपूर होता है और इसका उपयोग मवेशियों और मुर्गीपालन के चारे के रूप में किया जाता है। भारत में सूरजमुखी की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार में व्यापक रूप से की जाती है। सूरजमुखी भारत के कई हिस्सों में जायद मौसम की फसल के रूप में भी उगाया जाता है। @ जलवायु सूरजमुखी को समशीतोष्ण के साथ-साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी उगाया जा सकता है। इसके लिए 20-25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बेहतर प्रदर्शन के लिए 27-28 डिग्री इष्टतम होगा। इसके लिए 500-700 मिमी वर्षा की आवश्यकता होती है। इस फसल को अंकुरण और अंकुर वृद्धि के दौरान ठंडी जलवायु, अंकुर चरण से लेकर फूल आने तक गर्म मौसम और फूल आने से लेकर परिपक्वता तक बिना बादल वाले, धूप वाले दिनों की आवश्यकता होती है। @ मिट्टी इसे बलुई दोमट से लेकर काली मिट्टी तक विस्तृत प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। यह गहरी, तटस्थ, उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में उगाए जाने पर यह सर्वोत्तम परिणाम देता है। यह हल्की क्षारीय मिट्टी को सहन कर सकता है। अम्लीय और जलभराव वाली मिट्टी में बुआई करने से बचें। मिट्टी का इष्टतम पीएच 6.5-8.5 है। @ खेत की तैयारी एक बार ट्रैक्टर से या दो बार लोहे के हल से या तीन से चार बार देशी हल से तब तक जुताई करें जब तक सारे ढेले टूट न जाएं और बारीक जुताई न हो जाए। उसके बाद पाटा लगाएं। बुआई से पहले खेत में 4-5 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। @ बीज *बीज दर बुआई के लिए 2-3 किलोग्राम/एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। जबकि संकर के लिए 2-2.5 किलोग्राम/एकड़ की आवश्यकता होती है। *बीजोपचार शीघ्र अंकुरण के लिए बुआई से पहले बीजों को 24 घंटे तक पानी में भिगोकर छाया में सुखा लें। फिर बीज को 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। यह बीजों को मिट्टी जनित कीड़ों और बीमारियों से बचाएगा। बीज-जनित फंगल रोगों को नियंत्रित करने के लिए, बीज को ब्रैसिकल या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने की सलाह दी जाती है। फसल को मृदु फफूंदी से बचाने के लिए बीज को मेटलैक्सिल 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीजों को इमिडाक्लोप्रिड 5-6 मि.ली. प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। @ बुवाई * बुवाई का समय अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सूरजमुखी की बुआई जनवरी के अंत तक पूरी कर लें। बुआई में देरी होने की स्थिति में, जब बुआई फरवरी में करनी हो, तो रोपाई विधि का उपयोग करें क्योंकि सीधी बुआई से उपज में कमी आती है, साथ ही देर से बुआई करने पर कीट और रोग का प्रकोप अधिक होता है। * रिक्ति पंक्तियों के बीच 60 सेमी की दूरी रखें जबकि पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी रखें। * बुवाई की गहराई बीज को 4-5 सेमी की गहराई पर बोयें। * बुवाई की विधि बुआई के लिए डिबलिंग विधि का प्रयोग करें। सूरजमुखी की बुआई के लिए पंक्ति फसल बोने की मशीन की सहायता से समतल क्यारी या मेड़ पर बीज रखने का भी उपयोग किया जाता है। देरी से बुआई होने पर रोपाई विधि का प्रयोग करें। एक एकड़ भूमि में रोपाई के लिए 30 वर्ग मीटर की नर्सरी उपयुक्त होती है। बीज दर 1.5 कि.ग्रा. प्रयोग करें। रोपाई से 30 दिन पहले नर्सरी तैयार करें। बीज क्यारी तैयार करने के लिए 0.5 किलोग्राम यूरिया और 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपरफॉस्फेट मिलाएं। बीज क्यारी को पारदर्शी पॉलिथीन शीट और तैयार सुरंग से ढक दें। अंकुर निकलने के बाद पॉलिथीन शीट हटा दें। जब अंकुर 4 पत्ती अवस्था में हों, तो वे रोपाई के लिए तैयार होते हैं। रोपाई के लिए फसल उखाड़ने से पहले नर्सरी की सिंचाई करें। @ उर्वरक बुआई से दो से तीन सप्ताह पहले प्रति एकड़ 4-5 टन सड़ी हुई गाय का गोबर मिट्टी में डालें। कुल मिलाकर N :P @ 24:12 किलोग्राम प्रति एकड़ मिट्टी में यूरिया 50 किलोग्राम, एसएसपी 75 किलोग्राम के रूप में डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फॉस्फरस की पूरी मात्रा बुआई के समय डालें। शेष नाइट्रोजन बुआई के 30 दिन बाद डालें। सिंचित फसल के मामले में, नाइट्रोजन की शेष आधी खुराक दो बराबर भागों में डालें, पहले बुआई के 30 दिन बाद और शेष 15 दिन बाद। बेहतर वानस्पतिक वृद्धि के लिए पानी में घुलनशील 19:19:19 @ 5 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें जब फसल 5-6 पत्तियों की अवस्था में हो, आठ दिनों के अंतराल पर दो छिड़काव करें। रे फ्लोरेट के खुलने की अवस्था में बोरोन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। @ सिंचाई आमतौर पर सूरजमुखी की फसल के लिए 9-10 सिंचाइयां आदर्श होती हैं। सटीक संख्या जलवायु और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः हल्की मिट्टी के लिए 9-10 तथा भारी मिट्टी के लिए 5-6 सिंचाईयाँ पर्याप्त होती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 30 दिन बाद करें। 50% फूल आने के दौरान तथा नरम और सख्त आटे की अवस्था सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। बार-बार सिंचाई करने से बचें, क्योंकि इससे जड़ सड़न और मुरझाने का खतरा बढ़ सकता है। भारी मिट्टी में 20-25 दिन के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। हल्की मिट्टी में 8-10 दिनों के अंतराल की आवश्यकता होती है। @ खरपतवार प्रबंधन बुआई से पहले 2.0 लीटर/हेक्टेयर फ्लुक्लोरेलिन डालें और बुआई के 5 दिन बाद प्री - इमरजंस स्प्रे के रूप में डालें या लगाएं। इसके बाद सिंचाई करें। या बुआई के 3 दिन बाद प्री - इमरजंस स्प्रे के रूप में पेंडीमेथालिन लगाएं। इन शाकनाशियों का स्प्रे फ्लैट फैन नोजल से लगे बैक पैक/नैपसेक/रॉकर स्प्रेयर के साथ स्प्रे तरल पदार्थ के रूप में 900 लीटर पानी/हेक्टेयर का उपयोग करके पूरा किया जाना चाहिए। सभी शाकनाशी प्रयोग के बाद बुआई के 30-35 दिन बाद देर से हाथ से निराई करनी चाहिए। बुआई के 15वें और 30वें दिन हाथ से निराई-गुड़ाई करें और खरपतवार हटा दें। सिंचाई की स्थिति में खरपतवारों को 2-3 दिन तक सूखने दें और उसके बाद सिंचाई करें। @ फसल सुरक्षा * कीट 1. तम्बाकू कैटरपिलर ये सूरजमुखी के गंभीर कीट हैं। इसका प्रकोप अप्रैल-मई माह में देखा जाता है। वे पत्तियों खाते हैं। खेत से दूर फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ युवा लार्वा को भी नष्ट करें। यदि तम्बाकू इल्ली का प्रकोप दिखे तो फिप्रोनिल एससी 2 मि.ली. प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। गंभीर स्थिति में 10 दिनों के अंतराल पर दो स्प्रे करें या स्पिनोसैड 5 मिली प्रति 10 लीटर पानी या नुवान+इंडोक्साकार्ब 1 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। 2. हेड बोरर या अमेरिकन बॉलवॉर्म यह सूरजमुखी का गंभीर कीट है। यह पौधे को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये ऊतक और सिर में विकसित हो रहे दानों को खाते हैं। कवक विकसित हो जाता है और सिर सड़ जाते हैं। लार्वा का रंग हरे से भूरे तक भिन्न होता है। कीट की तीव्रता निर्धारित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप @ 4ट्रैप/एकड़ का उपयोग करें। यदि इसका प्रकोप दिखे तो कार्बेरिल 1 किलोग्राम या एसीफेट 800 ग्राम या क्लोरपाइरीफोस 1 लीटर को 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। 3. बालों वाली कैटरपिलर युवा लार्वा अधिकतर पत्तियों की सतह के नीचे पत्तियों को खाते हैं। प्रकोप के कारण पौधे सूखने लगते हैं। लार्वा काले बालों वाले पीले रंग के होते हैं। खेत से दूर फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ युवा लार्वा को भी नष्ट करें। यदि संक्रमण दिखे तो फिप्रोनिल एससी 2 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। गंभीर स्थिति में 10 दिनों के अंतराल पर दो स्प्रे करें या स्पिनोसैड 5 मि.ली. प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 4. जैसिड जैसिड जैसे रस चूसने वाले कीटों की घटना कली लगने की अवस्था में देखी जाती है। जैसिड में कप जैसी , झुर्रीदार पत्तियाँ और जली हुई उपस्थिति क्षति के लक्षण हैं। यदि 10-20% पौधों में रस चूसने वाले कीट का प्रकोप देखा जाए, तो फसल पर नीम के बीज की गिरी का रस 50 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। * रोग 1. जंग रतुआ रोग से उपज में 20% तक की हानि हो सकती है। यदि जंग का प्रकोप दिखे तो प्रभावी नियंत्रण के लिए ट्राइडेमोर्फ 1 ग्राम प्रति लीटर या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर या हेक्साकोनाज़ोल 2 मि.ली. प्रति लीटर पानी में 10 दिन के अंतराल पर दो बार करें। 2. चारकोल सड़ांध प्रभावित पौधा कमजोर हो जाता है और जल्दी परिपक्व हो जाता है, साथ ही तने का रंग काला, राख जैसा हो जाता है। परागण के बाद पौधे का अचानक मुरझाना देखा जाता है। बुआई के 30 दिन बाद मिट्टी में ट्राइकोडर्मा विराइड 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 20 किलोग्राम सड़ी हुई गाय के गोबर या रेत के साथ डालें। कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 3. तना सड़न बुआई के 40 दिन के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पौधा बीमार हो जाता है और दूर से भी देखा जा सकता है। प्रभावित पौधे के पास की मिट्टी की सतह पर सफेद कॉटनी कवक देखा जाता है। बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। 4. अल्टरनेरिया ब्लाइट यह एक गंभीर बीमारी है, इससे बीज और तेल की उपज में कमी आती है। गहरे, भूरे काले धब्बे पहले निचली पत्तियों पर विकसित होते हैं, बाद में मध्य और ऊपरी पत्तियों तक फैल जाते हैं। गंभीर संक्रमण में तने, डंठलों पर धब्बे दिखाई देते हैं। यदि प्रकोप दिखाई दे तो मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर चार बार छिड़काव करें। 5. सिर सड़ना प्रारंभ में, पकने वाले सिर के पीछे की ओर भूरे रंग के अनियमित जल सोख धब्बे देखे जाते हैं। बाद में धब्बे बड़े और गूदेदार हो जाते हैं और सफेद रूईदार कवक से ढक जाते हैं, बाद में काले हो जाते हैं। फूल आने से पहले या सिर के विकास के शुरुआती चरण में चोट लगने से संक्रमण होने की संभावना होती है, इसलिए सिर पर चोट लगने से बचें। यदि संक्रमण दिखाई दे तो मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। @ कटाई सूरजमुखी की फसल 90-100 दिनों में पक जाती है। सूरजमुखी की फसल की कटाई तब की जाती है जब सभी पत्तियाँ सूख जाती हैं और सूरजमुखी के सिर का पिछला भाग नींबू जैसा पीला रंग प्राप्त कर लेता है। @ उपज सूरजमुखी की फसल वर्षा आधारित परिस्थितियों में 300-500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सिंचाई के तहत उगाए जाने पर 800-1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज देती है।